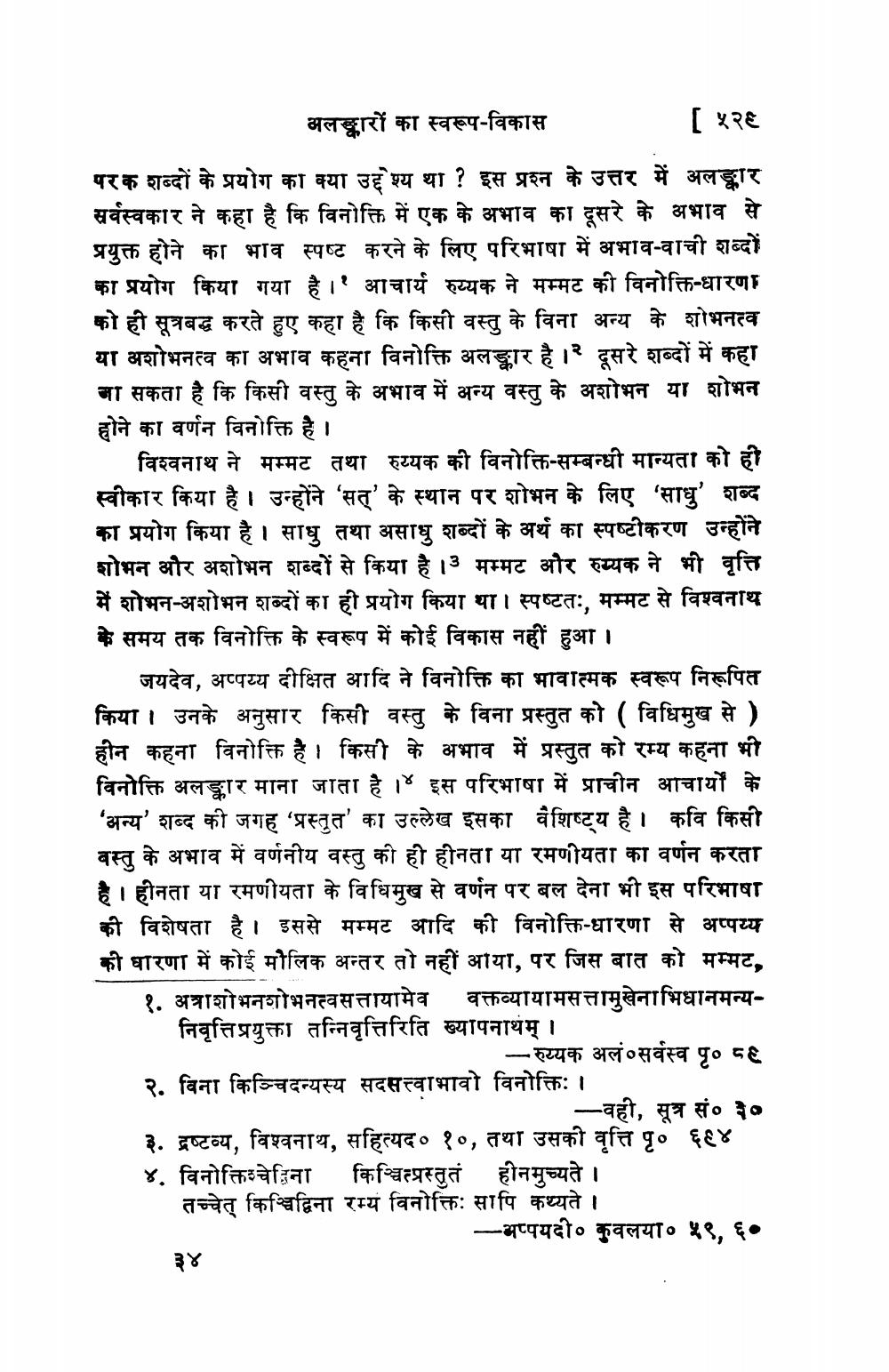________________
अलङ्कारों का स्वरूप - विकास
[ ५२६
परक शब्दों के प्रयोग का क्या उद्देश्य था ? इस प्रश्न के उत्तर में अलङ्कार सर्वस्वकार ने कहा है कि विनोक्ति में एक के अभाव का दूसरे के अभाव से प्रयुक्त होने का भाव स्पष्ट करने के लिए परिभाषा में अभाव-वाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। आचार्य रुय्यक ने मम्मट की विनोक्ति-धारणा को ही सूत्रबद्ध करते हुए कहा है कि किसी वस्तु के विना अन्य के शोभनत्व या अशोभनत्व का अभाव कहना विनोक्ति अलङ्कार है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के अभाव में अन्य वस्तु के अशोभन या शोभन होने का वर्णन विनोक्ति है ।
विश्वनाथ ने मम्मट तथा रुय्यक की विनोक्ति-सम्बन्धी मान्यता को ही स्वीकार किया है । उन्होंने 'सत्' के स्थान पर शोभन के लिए 'साधु' शब्द का प्रयोग किया है । साधु तथा असाधु शब्दों के अर्थ का स्पष्टीकरण उन्होंने शोभन और अशोभन शब्दों से किया है । 3 मम्मट और रुम्यक ने भी वृत्ति में शोभन अशोभन शब्दों का ही प्रयोग किया था । स्पष्टतः, मम्मट से विश्वनाथ के समय तक विनोक्ति के स्वरूप में कोई विकास नहीं हुआ ।
जयदेव, अप्पय्य दीक्षित आदि ने विनोक्ति का भावात्मक स्वरूप निरूपित किया । उनके अनुसार किसी वस्तु के विना प्रस्तुत को ( विधिमुख से ) हीन कहना विनोक्ति है । किसी के अभाव में प्रस्तुत को रम्य कहना भी विनोक्ति अलङ्कार माना जाता है । इस परिभाषा में प्राचीन आचार्यों के 'अन्य' शब्द की जगह 'प्रस्तुत' का उल्लेख इसका वैशिष्ट्य है । कवि किसी वस्तु के अभाव में वर्णनीय वस्तु की ही होनता या रमणीयता का वर्णन करता है । हीनता या रमणीयता के विधिमुख से वर्णन पर बल देना भी इस परिभाषा की विशेषता है । इससे मम्मट आदि की विनोक्ति धारणा से अप्पय्य की धारणा में कोई मौलिक अन्तर तो नहीं आया, पर जिस बात को मम्मट, १. अत्राशोभनशोभनत्वसत्तायामेव वक्तव्यायामसत्तामुखेनाभिधानमन्यनिवृत्तिप्रयुक्ता तन्निवृत्तिरिति ख्यापनार्थम् ।
— रुय्यक अलं० सर्वस्व पृ० ८६
२. विना किञ्चिदन्यस्य सदसत्त्वाभावो विनोक्तिः ।
- वही, सूत्र सं० ३० ३. द्रष्टव्य, विश्वनाथ, सहित्यद० १०, तथा उसकी वृत्ति पृ० ६६४
४. विनोक्तिश्चेविना किञ्चित्प्रस्तुतं हीनमुच्यते ।
तच्चेत् किञ्चिद्विना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते ।
३४
अप्पयदी० कुवलया० ५९, ६०