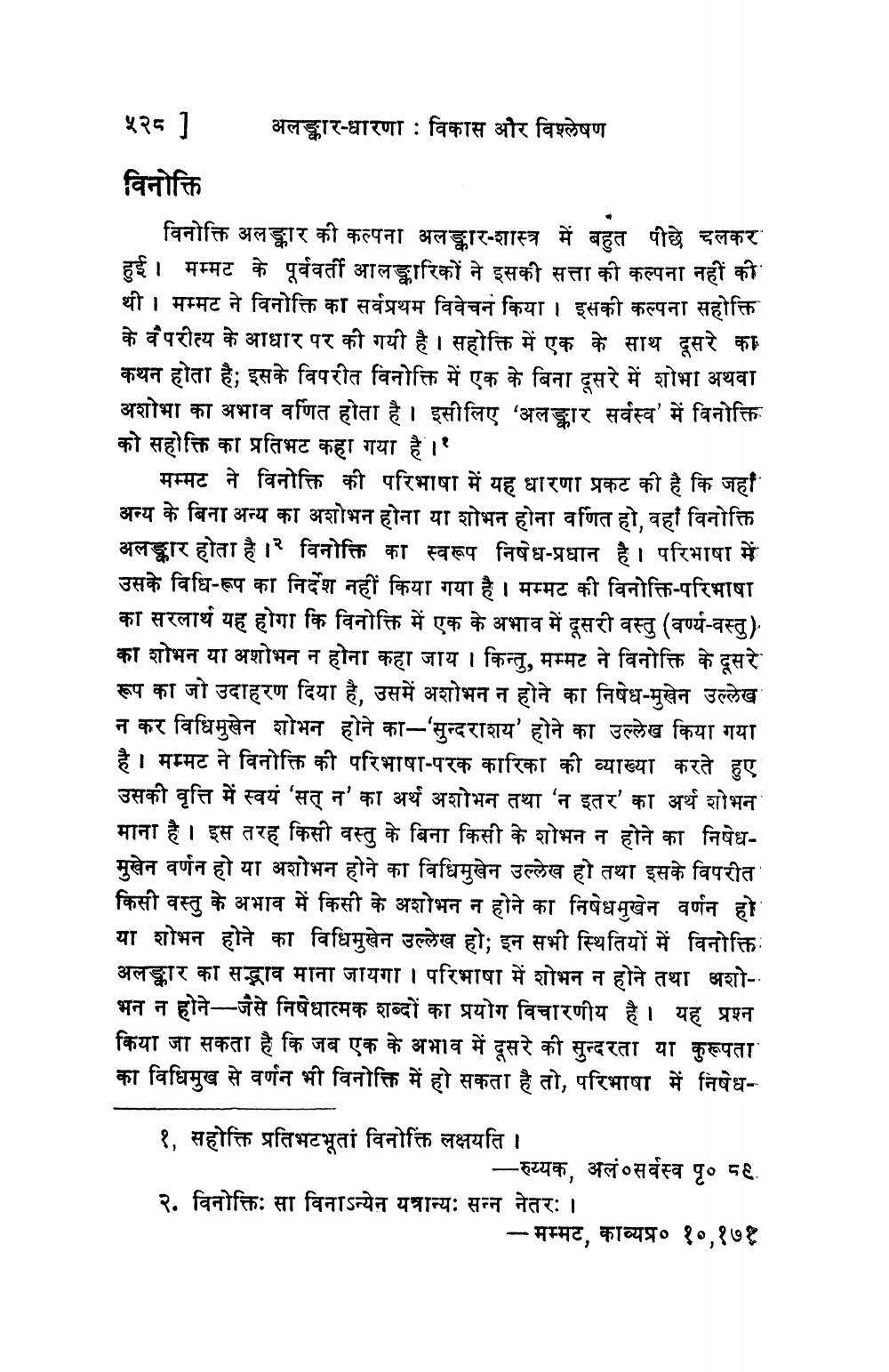________________
५२८ ]
विनोक्ति
हुई ।
विनोक्ति अलङ्कार की कल्पना अलङ्कार-शास्त्र में बहुत पीछे चलकर मम्मट के पूर्ववर्ती आलङ्कारिकों ने इसकी सत्ता की कल्पना नहीं की थी । मम्मट ने विनोक्ति का सर्वप्रथम विवेचनं किया । इसकी कल्पना सहोक्ति के वैपरीत्य के आधार पर की गयी है । सहोक्ति में एक के साथ दूसरे का कथन होता है; इसके विपरीत विनोक्ति में एक के बिना दूसरे में शोभा अथवा अशोभा का अभाव वर्णित होता है । इसीलिए 'अलङ्कार सर्वस्व' में विनोक्ति को सहोक्ति का प्रतिभट कहा गया है । "
मम्मट ने विनोक्ति की परिभाषा में यह धारणा प्रकट की है कि जहाँ अन्य के बिना अन्य का अशोभन होना या शोभन होना वर्णित हो, वहाँ विनोक्ति अलङ्कार होता है । २ विनोक्ति का स्वरूप निषेध-प्रधान है । परिभाषा में उसके विधि-रूप का निर्देश नहीं किया गया है । मम्मट की विनोक्ति - परिभाषा का सरलार्थ यह होगा कि विनोक्ति में एक के अभाव में दूसरी वस्तु ( वर्ण्य-वस्तु) का शोभन या अशोभन न होना कहा जाय । किन्तु, मम्मट ने विनोक्ति के दूसरे रूप का जो उदाहरण दिया है, उसमें अशोभन न होने का निषेध - मुखेन उल्लेख न कर विधिमुखेन शोभन होने का - ' सुन्दराशय' होने का उल्लेख किया गया है । मम्मट ने विनोक्ति की परिभाषा परक कारिका की व्याख्या करते हुए उसकी वृत्ति में स्वयं 'सत् न' का अर्थ अशोभन तथा 'न इतर' का अर्थ शोभन माना है । इस तरह किसी वस्तु के बिना किसी के शोभन न होने का निषेधमुखेन वर्णन हो या अशोभन होने का विधिमुखेन उल्लेख हो तथा इसके विपरीत किसी वस्तु के अभाव में किसी के अशोभन न होने का निषेधमुखेन वर्णन हो या शोभन होने का विधिमुखेन उल्लेख हो; इन सभी स्थितियों में विनोक्तिः अलङ्कार का सद्भाव माना जायगा । परिभाषा में शोभन न होने तथा अशोभन न होने — जैसे निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग विचारणीय है । यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब एक के अभाव में दूसरे की सुन्दरता या कुरूपता का विधिमुख से वर्णन भी विनोक्ति में हो सकता है तो, परिभाषा में निषेध -
-
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
१, सहोक्ति प्रतिभटभूतां विनोक्ति लक्षयति ।
— रुय्यक, अलं० सर्वस्व पृ० ८६
२. विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः ।
- मम्मट, काव्यप्र० १०, १७१