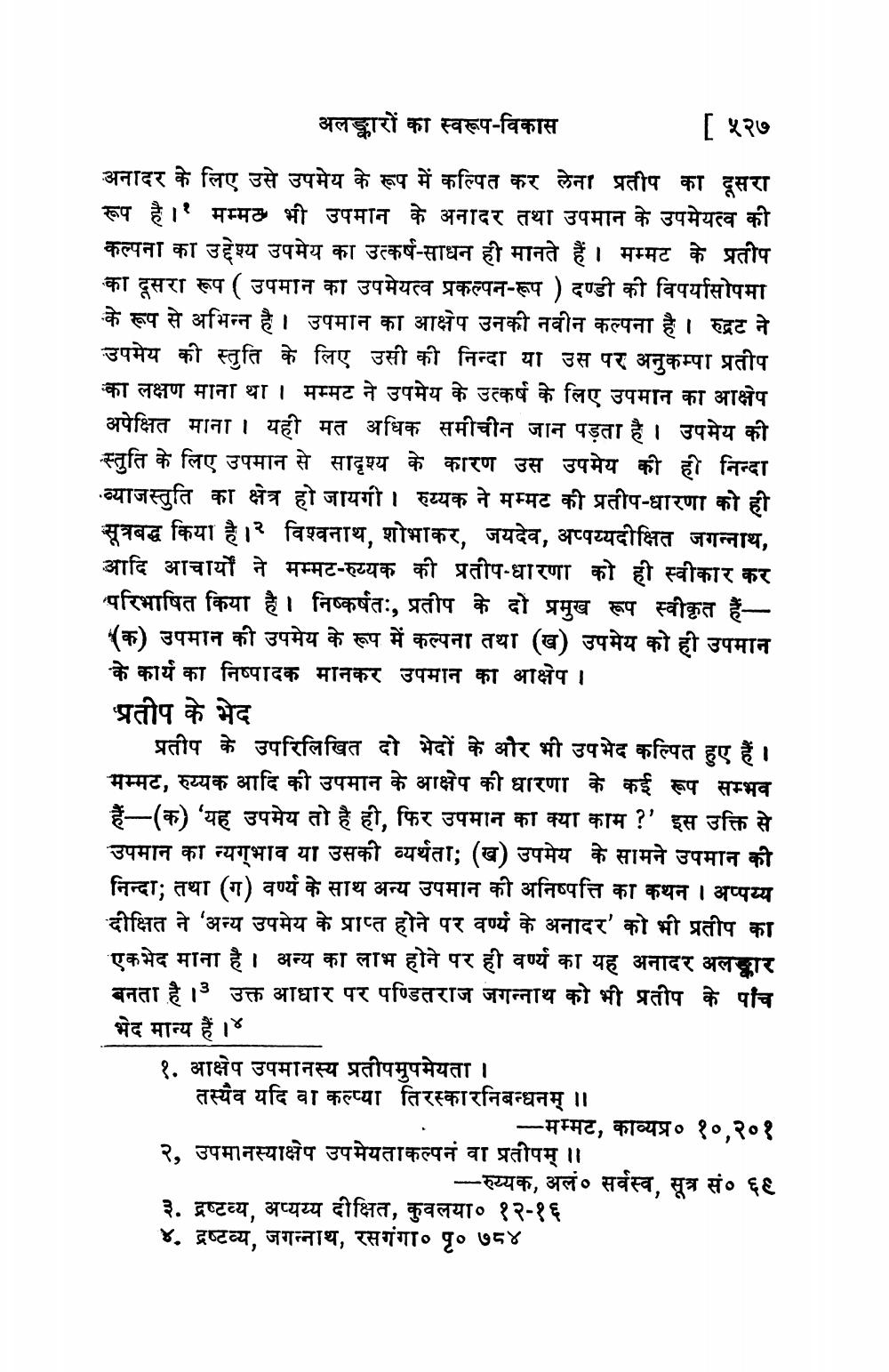________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ५२७
अनादर के लिए उसे उपमेय के रूप में कल्पित कर लेना प्रतीप का दूसरा रूप है।' मम्मळ भी उपमान के अनादर तथा उपमान के उपमेयत्व की कल्पना का उद्देश्य उपमेय का उत्कर्ष-साधन ही मानते हैं। मम्मट के प्रतीप का दूसरा रूप ( उपमान का उपमेयत्व प्रकल्पन-रूप ) दण्डी की विपर्यासोपमा के रूप से अभिन्न है। उपमान का आक्षेप उनकी नवीन कल्पना है। रुद्रट ने उपमेय की स्तुति के लिए उसी की निन्दा या उस पर अनुकम्पा प्रतीप का लक्षण माना था। मम्मट ने उपमेय के उत्कर्ष के लिए उपमान का आक्षेप अपेक्षित माना। यही मत अधिक समीचीन जान पड़ता है। उपमेय की स्तुति के लिए उपमान से सादृश्य के कारण उस उपमेय की ही निन्दा व्याजस्तुति का क्षेत्र हो जायगी। रुय्यक ने मम्मट की प्रतीप-धारणा को ही सूत्रबद्ध किया है।२ विश्वनाथ, शोभाकर, जयदेव, अप्पय्यदीक्षित जगन्नाथ, आदि आचार्यों ने मम्मट-रुय्यक की प्रतीप-धारणा को ही स्वीकार कर परिभाषित किया है। निष्कर्षतः, प्रतीप के दो प्रमुख रूप स्वीकृत हैं"(क) उपमान की उपमेय के रूप में कल्पना तथा (ख) उपमेय को ही उपमान के कार्य का निष्पादक मानकर उपमान का आक्षेप । प्रतीप के भेद
प्रतीप के उपरिलिखित दो भेदों के और भी उपभेद कल्पित हुए हैं। मम्मट, रुय्यक आदि की उपमान के आक्षेप की धारणा के कई रूप सम्भव हैं—(क) 'यह उपमेय तो है ही, फिर उपमान का क्या काम ?' इस उक्ति से उपमान का न्यग्भाव या उसकी व्यर्थता; (ख) उपमेय के सामने उपमान की निन्दा; तथा (ग) वर्ण्य के साथ अन्य उपमान की अनिष्पत्ति का कथन । अप्पय्य दीक्षित ने 'अन्य उपमेय के प्राप्त होने पर वर्ण्य के अनादर' को भी प्रतीप का एकभेद माना है। अन्य का लाभ होने पर ही वर्ण्य का यह अनादर अलङ्कार बनता है। उक्त आधार पर पण्डितराज जगन्नाथ को भी प्रतीप के पांच भेद मान्य हैं। १. आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता। तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनम् ॥
-मम्मट, काव्यप्र० १०,२०१ २, उपमानस्याक्षेप उपमेयताकल्पनं वा प्रतीपम् ।।
-रुय्यक, अलं० सर्वस्व, सूत्र सं० ६६ ३. द्रष्टव्य, अप्यय्य दीक्षित, कुवलया० १२-१६ ४. द्रष्टव्य, जगन्नाथ, रसगंगा० पृ० ७८४