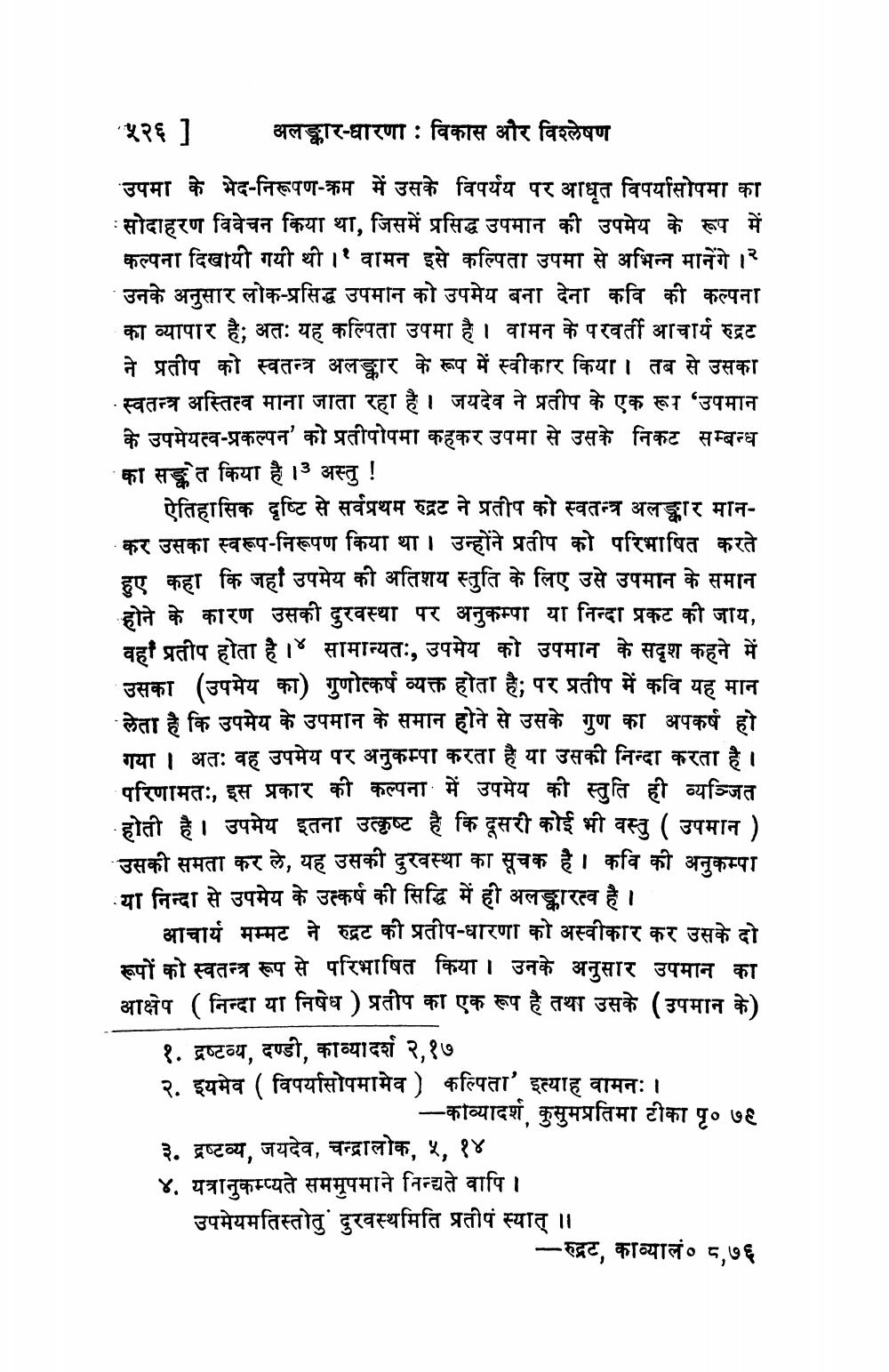________________
'५२६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण उपमा के भेद-निरूपण-क्रम में उसके विपर्यय पर आधृत विपर्यासोपमा का सोदाहरण विवेचन किया था, जिसमें प्रसिद्ध उपमान की उपमेय के रूप में कल्पना दिखायी गयी थी।' वामन इसे कल्पिता उपमा से अभिन्न मानेंगे। उनके अनुसार लोक-प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना कवि की कल्पना का व्यापार है; अतः यह कल्पिता उपमा है। वामन के परवर्ती आचार्य रुद्रट ने प्रतीप को स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में स्वीकार किया। तब से उसका • स्वतन्त्र अस्तित्व माना जाता रहा है। जयदेव ने प्रतीप के एक रूप 'उपमान के उपमेयत्व-प्रकल्पन' को प्रतीपोपमा कहकर उपमा से उसके निकट सम्बन्ध का सङ्कत किया है । 3 अस्तु !
ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम रुद्रट ने प्रतीप को स्वतन्त्र अलङ्कार मानकर उसका स्वरूप-निरूपण किया था। उन्होंने प्रतीप को परिभाषित करते हुए कहा कि जहां उपमेय की अतिशय स्तुति के लिए उसे उपमान के समान होने के कारण उसकी दुरवस्था पर अनुकम्पा या निन्दा प्रकट की जाय, वहाँ प्रतीप होता है। सामान्यतः, उपमेय को उपमान के सदृश कहने में उसका (उपमेय का) गुणोत्कर्ष व्यक्त होता है; पर प्रतीप में कवि यह मान लेता है कि उपमेय के उपमान के समान होने से उसके गुण का अपकर्ष हो गया। अतः वह उपमेय पर अनुकम्पा करता है या उसकी निन्दा करता है। परिणामतः, इस प्रकार की कल्पना में उपमेय की स्तुति ही व्यजित होती है। उपमेय इतना उत्कृष्ट है कि दूसरी कोई भी वस्तु ( उपमान ) उसकी समता कर ले, यह उसकी दुरवस्था का सूचक है। कवि की अनुकम्पा या निन्दा से उपमेय के उत्कर्ष की सिद्धि में ही अलङ्कारत्व है।
आचार्य मम्मट ने रुद्रट की प्रतीप-धारणा को अस्वीकार कर उसके दो रूपों को स्वतन्त्र रूप से परिभाषित किया। उनके अनुसार उपमान का आक्षेप (निन्दा या निषेध ) प्रतीप का एक रूप है तथा उसके (उपमान के)
१. द्रष्टव्य, दण्डी, काव्यादर्श २,१७ २. इयमेव ( विपर्यासोपमामेव ) कल्पिता' इत्याह वामनः ।
-काव्यादर्श, कुसुमप्रतिमा टीका पृ०७६ ३. द्रष्टव्य, जयदेव, चन्द्रालोक, ५, १४ ४. यत्रानुकम्प्यते सममुपमाने निन्द्यते वापि । उपमेयमतिस्तोतु दुरवस्थमिति प्रतीपं स्यात् ।।
-रुद्रट, काव्यालं० ८,७६