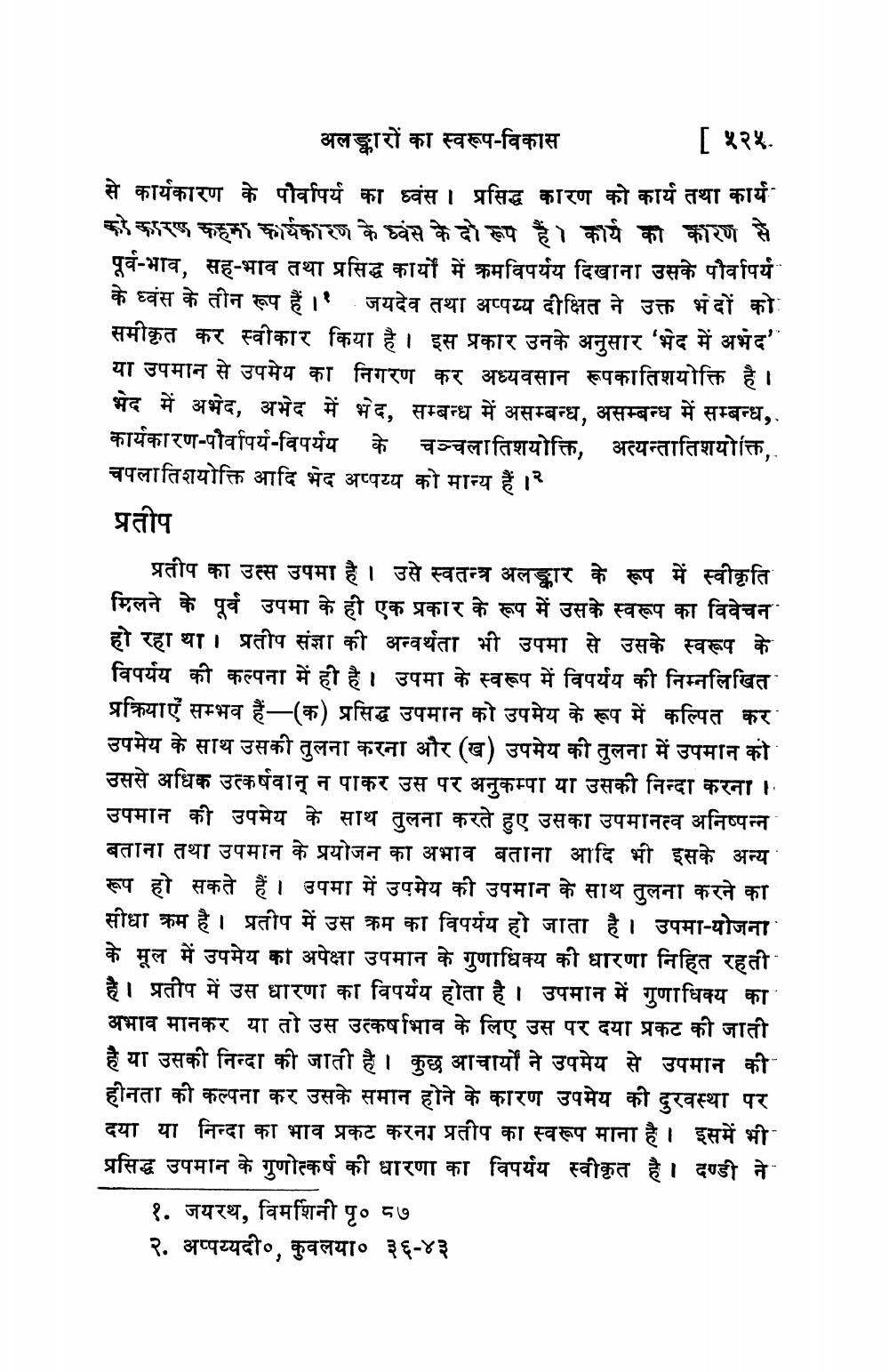________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास [ ५२५. से कार्यकारण के पौर्वापर्य का ध्वंस। प्रसिद्ध कारण को कार्य तथा कार्य को कारण कहना कार्यकारण के ध्वंस के दो रूप हैं। कार्य का कारण से पूर्व-भाव, सह-भाव तथा प्रसिद्ध कार्यों में क्रमविपर्यय दिखाना उसके पौर्वापर्य के ध्वंस के तीन रूप हैं।' जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित ने उक्त भेदों को समीकृत कर स्वीकार किया है। इस प्रकार उनके अनुसार 'भेद में अभेद' या उपमान से उपमेय का निगरण कर अध्यवसान रूपकातिशयोक्ति है। भेद में अभेद, अभेद में भेद, सम्बन्ध में असम्बन्ध, असम्बन्ध में सम्बन्ध, कार्यकारण-पौर्वापर्य-विपर्यय के चञ्चलातिशयोक्ति, अत्यन्तातिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति आदि भेद अप्पय्य को मान्य हैं । प्रतीप
प्रतीप का उत्स उपमा है। उसे स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में स्वीकृति मिलने के पूर्व उपमा के ही एक प्रकार के रूप में उसके स्वरूप का विवेचन हो रहा था। प्रतीप संज्ञा की अन्वर्थता भी उपमा से उसके स्वरूप के विपर्यय की कल्पना में ही है। उपमा के स्वरूप में विपर्यय की निम्नलिखित प्रक्रियाएँ सम्भव हैं—(क) प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित कर उपमेय के साथ उसकी तुलना करना और (ख) उपमेय की तुलना में उपमान को उससे अधिक उत्कर्षवान् न पाकर उस पर अनुकम्पा या उसकी निन्दा करना । उपमान की उपमेय के साथ तुलना करते हुए उसका उपमानत्व अनिष्पन्न बताना तथा उपमान के प्रयोजन का अभाव बताना आदि भी इसके अन्य रूप हो सकते हैं। उपमा में उपमेय की उपमान के साथ तुलना करने का सीधा क्रम है। प्रतीप में उस क्रम का विपर्यय हो जाता है। उपमा-योजना के मूल में उपमेय को अपेक्षा उपमान के गुणाधिक्य की धारणा निहित रहती है। प्रतीप में उस धारणा का विपर्यय होता है। उपमान में गुणाधिक्य का अभाव मानकर या तो उस उत्कर्षाभाव के लिए उस पर दया प्रकट की जाती है या उसकी निन्दा की जाती है। कुछ आचार्यों ने उपमेय से उपमान की हीनता की कल्पना कर उसके समान होने के कारण उपमेय की दुरवस्था पर दया या निन्दा का भाव प्रकट करना प्रतीप का स्वरूप माना है। इसमें भी प्रसिद्ध उपमान के गुणोत्कर्ष की धारणा का विपर्यय स्वीकृत है। दण्डी ने
१. जयरथ, विमशिनी पृ० ८७ २. अप्पय्यदी०, कुवलया० ३६-४३