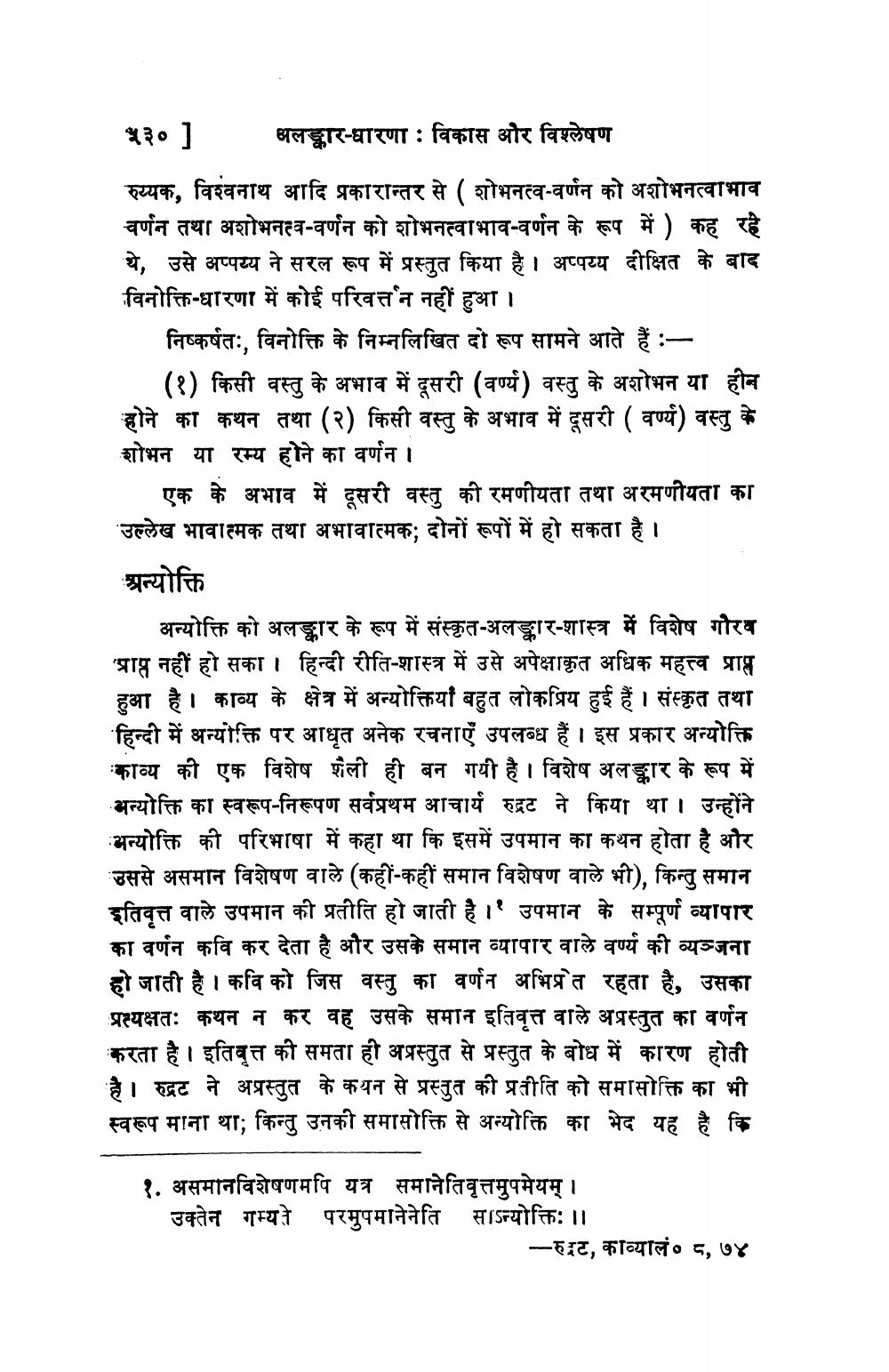________________
५३० ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण रुय्यक, विश्वनाथ आदि प्रकारान्तर से ( शोभनत्व-वर्णन को अशोभनत्वाभाव वर्णन तथा अशोभनत्व-वर्णन को शोभनत्वाभाव-वर्णन के रूप में ) कह रहे थे, उसे अप्पय्य ने सरल रूप में प्रस्तुत किया है। अप्पय्य दीक्षित के बाद विनोक्ति-धारणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
निष्कर्षतः, विनोक्ति के निम्नलिखित दो रूप सामने आते हैं :
(१) किसी वस्तु के अभाव में दूसरी (वर्ण्य) वस्तु के अशोभन या हीन होने का कथन तथा (२) किसी वस्तु के अभाव में दूसरी ( वर्ण्य) वस्तु के शोभन या रम्य होने का वर्णन । ___एक के अभाव में दूसरी वस्तु की रमणीयता तथा अरमणीयता का उल्लेख भावात्मक तथा अभावात्मक; दोनों रूपों में हो सकता है। अन्योक्ति ___ अन्योक्ति को अलङ्कार के रूप में संस्कृत-अलङ्कार-शास्त्र में विशेष गौरव 'प्राप्त नहीं हो सका। हिन्दी रीति-शास्त्र में उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है। काव्य के क्षेत्र में अन्योक्तियां बहुत लोकप्रिय हुई हैं । संस्कृत तथा हिन्दी में अन्योक्ति पर आधृत अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं । इस प्रकार अन्योक्ति काव्य की एक विशेष शैली ही बन गयी है। विशेष अलङ्कार के रूप में भन्योक्ति का स्वरूप-निरूपण सर्वप्रथम आचार्य रुद्रट ने किया था। उन्होंने अन्योक्ति की परिभाषा में कहा था कि इसमें उपमान का कथन होता है और उससे असमान विशेषण वाले (कहीं-कहीं समान विशेषण वाले भी), किन्तु समान इतिवृत्त वाले उपमान की प्रतीति हो जाती है।' उपमान के सम्पूर्ण व्यापार का वर्णन कवि कर देता है और उसके समान व्यापार वाले वर्ण्य की व्यञ्जना हो जाती है । कवि को जिस वस्तु का वर्णन अभिप्रेत रहता है, उसका प्रत्यक्षतः कथन न कर वह उसके समान इतिवृत्त वाले अप्रस्तुत का वर्णन करता है। इतिवृत्त की समता ही अप्रस्तुत से प्रस्तुत के बोध में कारण होती है। रुद्रट ने अप्रस्तुत के कयन से प्रस्तुत की प्रतीति को समासोक्ति का भी स्वरूप माना था; किन्तु उनकी समासोक्ति से अन्योक्ति का भेद यह है कि
१. असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम् । उक्तेन गम्यते परमपमानेनेति साऽन्योक्तिः ।।
-रुदट, काव्यालं०८, ७४