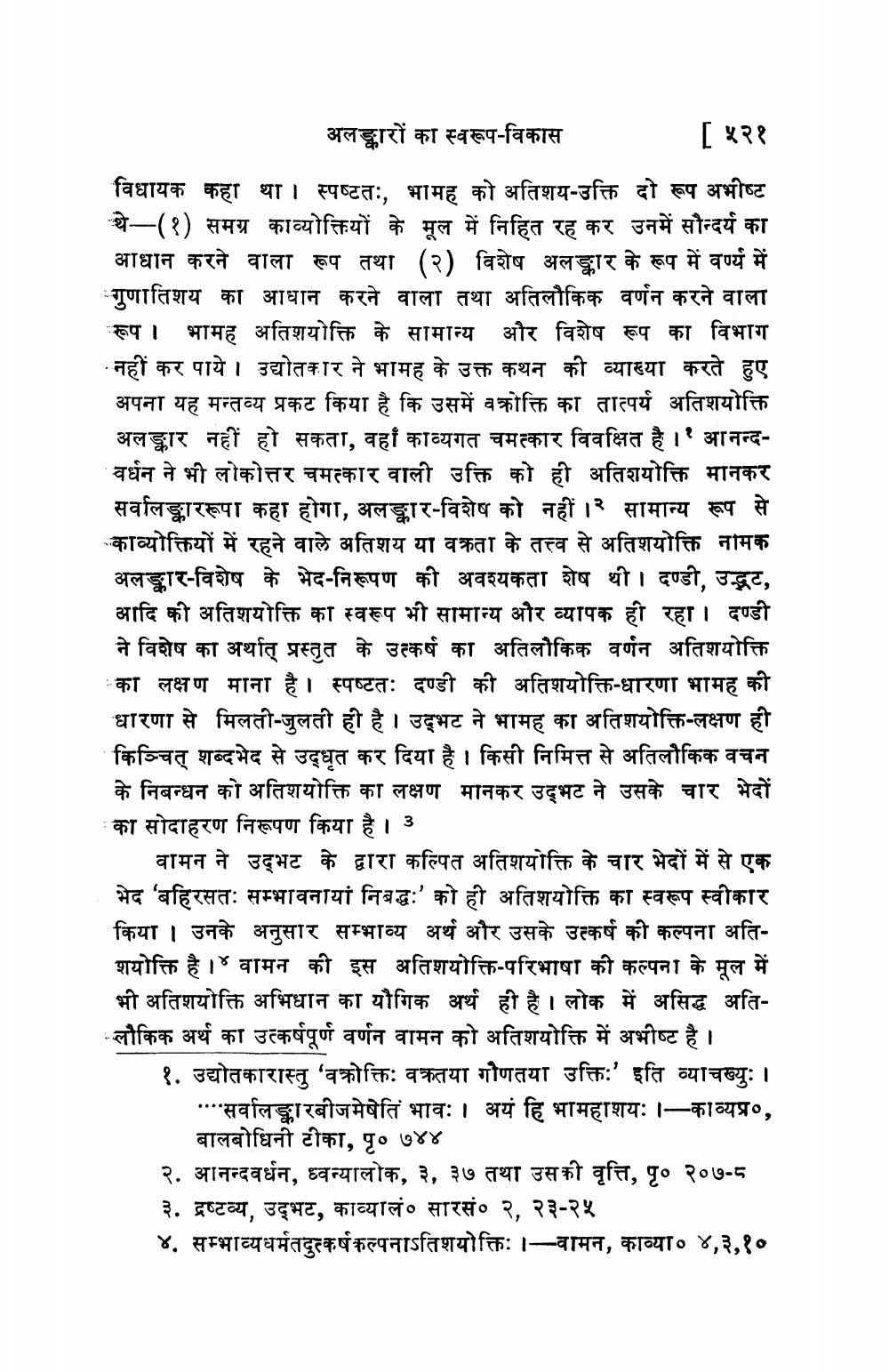________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[५२१ विधायक कहा था। स्पष्टतः, भामह को अतिशय-उक्ति दो रूप अभीष्ट थे—(१) समग्र काव्योक्तियों के मूल में निहित रह कर उनमें सौन्दर्य का आधान करने वाला रूप तथा (२) विशेष अलङ्कार के रूप में वर्ण्य में -गुणातिशय का आधान करने वाला तथा अतिलौकिक वर्णन करने वाला रूप। भामह अतिशयोक्ति के सामान्य और विशेष रूप का विभाग नहीं कर पाये। उद्योतकार ने भामह के उक्त कथन की व्याख्या करते हुए अपना यह मन्तव्य प्रकट किया है कि उसमें वक्रोक्ति का तात्पर्य अतिशयोक्ति अलङ्कार नहीं हो सकता, वहाँ काव्यगत चमत्कार विवक्षित है ।' आनन्दवर्धन ने भी लोकोत्तर चमत्कार वाली उक्ति को ही अतिशयोक्ति मानकर सर्वालङ्काररूपा कहा होगा, अलङ्कार-विशेष को नहीं ।२ सामान्य रूप से काव्योक्तियों में रहने वाले अतिशय या वक्रता के तत्त्व से अतिशयोक्ति नामक अलङ्कार-विशेष के भेद-निरूपण की अवश्यकता शेष थी। दण्डी, उद्भट, आदि की अतिशयोक्ति का स्वरूप भी सामान्य और व्यापक ही रहा। दण्डी ने विशेष का अर्थात् प्रस्तुत के उत्कर्ष का अतिलौकिक वर्णन अतिशयोक्ति का लक्षण माना है। स्पष्टतः दण्डी की अतिशयोक्ति-धारणा भामह की धारणा से मिलती-जुलती ही है । उद्भट ने भामह का अतिशयोक्ति-लक्षण ही किञ्चित् शब्दभेद से उद्धृत कर दिया है । किसी निमित्त से अतिलौकिक वचन के निबन्धन को अतिशयोक्ति का लक्षण मानकर उद्भट ने उसके चार भेदों का सोदाहरण निरूपण किया है। 3
वामन ने उद्भट के द्वारा कल्पित अतिशयोक्ति के चार भेदों में से एक भेद 'बहिरसतः सम्भावनायां निबद्धः' को ही अतिशयोक्ति का स्वरूप स्वीकार किया। उनके अनुसार सम्भाव्य अर्थ और उसके उत्कर्ष की कल्पना अतिशयोक्ति है।४ वामन की इस अतिशयोक्ति-परिभाषा की कल्पना के मूल में भी अतिशयोक्ति अभिधान का यौगिक अर्थ ही है । लोक में असिद्ध अतिलौकिक अर्थ का उत्कर्षपूर्ण वर्णन वामन को अतिशयोक्ति में अभीष्ट है। १. उद्योतकारास्तु 'वक्रोक्तिः वक्रतया गौणतया उक्तिः' इति व्याचख्युः ।
""सर्वालङ्कारबीजमेषेति भावः । अयं हि भामहाशयः ।-काव्यप्र०, बालबोधिनी टीका, पृ० ७४४ २. आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक, ३, ३७ तथा उसकी वृत्ति, पृ० २०७-८ ३. द्रष्टव्य, उद्भट, काव्यालं० सारसं० २, २३-२५ । ४. सम्भाव्यधर्मतदुत्कर्षकल्पनाऽतिशयोक्तिः । -वामन, काव्या० ४,३,१०