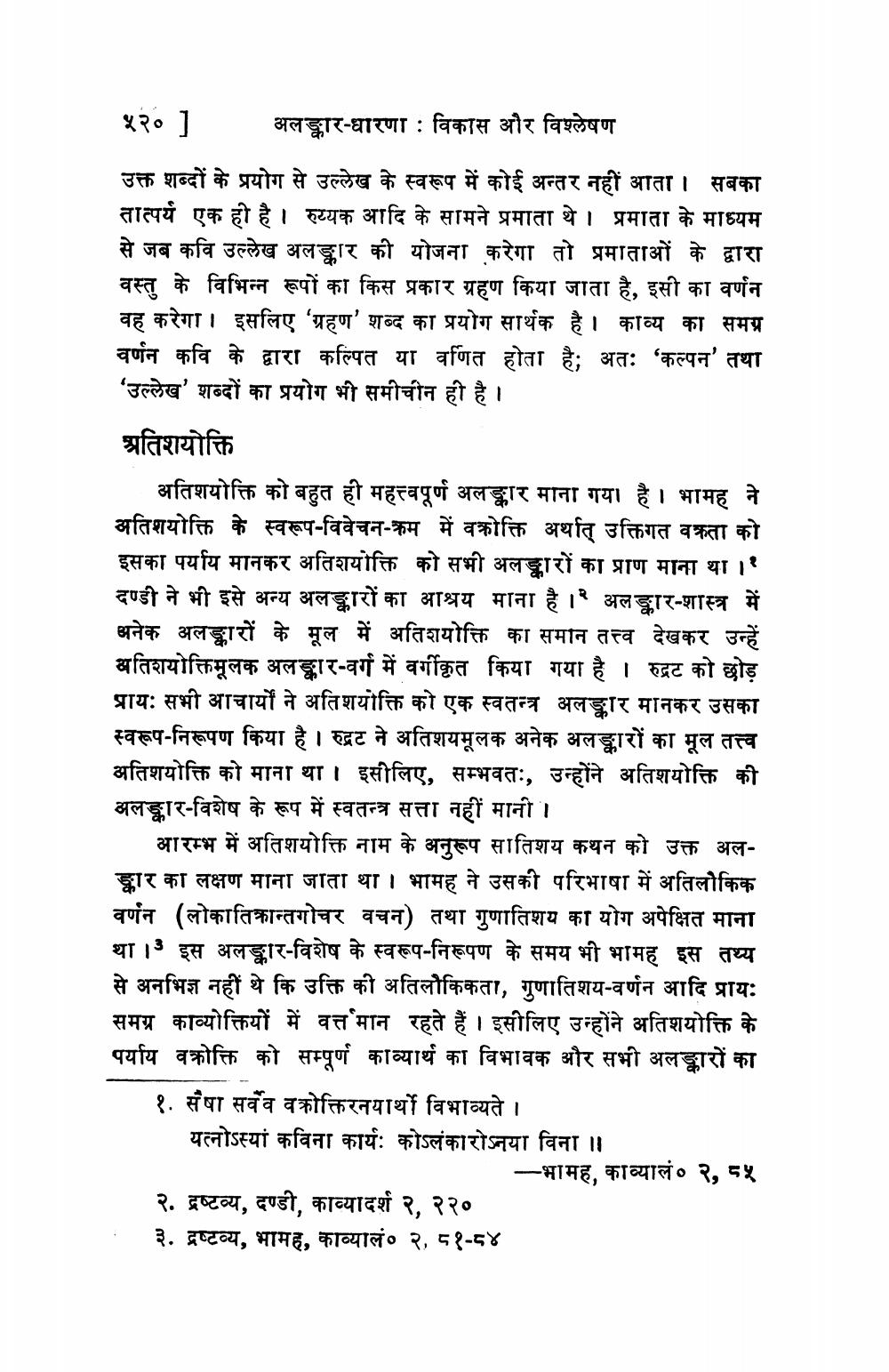________________
५२० ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
उक्त शब्दों के प्रयोग से उल्लेख के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता। सबका तात्पर्य एक ही है। रुय्यक आदि के सामने प्रमाता थे। प्रमाता के माध्यम से जब कवि उल्लेख अलङ्कार की योजना करेगा तो प्रमाताओं के द्वारा वस्तु के विभिन्न रूपों का किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, इसी का वर्णन वह करेगा। इसलिए 'ग्रहण' शब्द का प्रयोग सार्थक है। काव्य का समग्र वर्णन कवि के द्वारा कल्पित या वर्णित होता है; अतः 'कल्पन' तथा 'उल्लेख' शब्दों का प्रयोग भी समीचीन ही है । अतिशयोक्ति
अतिशयोक्ति को बहुत ही महत्त्वपूर्ण अलङ्कार माना गया है। भामह ने अतिशयोक्ति के स्वरूप-विवेचन-क्रम में वक्रोक्ति अर्थात् उक्तिगत वक्रता को इसका पर्याय मानकर अतिशयोक्ति को सभी अलङ्कारों का प्राण माना था।' दण्डी ने भी इसे अन्य अलङ्कारों का आश्रय माना है । २ अलङ्कार-शास्त्र में अनेक अलङ्कारों के मूल में अतिशयोक्ति का समान तत्त्व देखकर उन्हें अतिशयोक्तिमूलक अलङ्कार-वर्ग में वर्गीकृत किया गया है । रुद्रट को छोड़ प्रायः सभी आचार्यों ने अतिशयोक्ति को एक स्वतन्त्र अलङ्कार मानकर उसका स्वरूप-निरूपण किया है । रुद्रट ने अतिशयमूलक अनेक अलङ्कारों का मूल तत्त्व अतिशयोक्ति को माना था। इसीलिए, सम्भवतः, उन्होंने अतिशयोक्ति की अलङ्कार-विशेष के रूप में स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी। ___आरम्भ में अतिशयोक्ति नाम के अनुरूप सातिशय कथन को उक्त अलङ्कार का लक्षण माना जाता था। भामह ने उसकी परिभाषा में अतिलौकिक वर्णन (लोकातिक्रान्तगोचर वचन) तथा गुणातिशय का योग अपेक्षित माना था।' इस अलङ्कार-विशेष के स्वरूप-निरूपण के समय भी भामह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि उक्ति की अतिलौकिकता, गुणातिशय-वर्णन आदि प्रायः समग्र काव्योक्तियों में वत्त मान रहते हैं । इसीलिए उन्होंने अतिशयोक्ति के पर्याय वक्रोक्ति को सम्पूर्ण काव्यार्थ का विभावक और सभी अलङ्कारों का १. सैषा सर्वव वक्रोक्तिरनयार्थी विभाव्यते । यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥
-भामह, काव्यालं० २, ८५ २. द्रष्टव्य, दण्डी, काव्यादर्श २, २२० ३. द्रष्टव्य, भामह, काव्यालं० २, ८१-८४