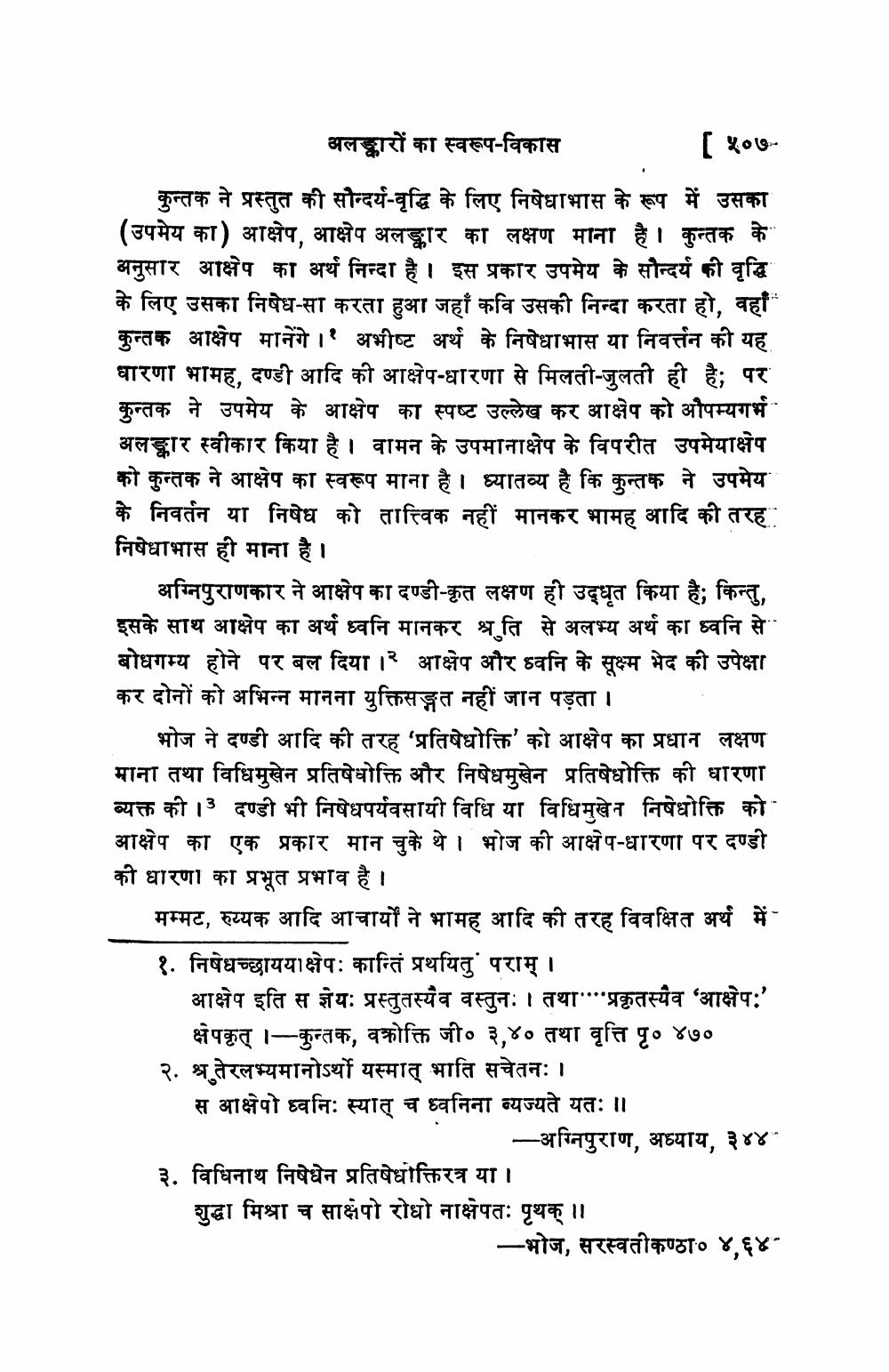________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[५०७.
कुन्तक ने प्रस्तुत की सौन्दर्य-वृद्धि के लिए निषेधाभास के रूप में उसका (उपमेय का) आक्षेप, आक्षेप अलङ्कार का लक्षण माना है। कुन्तक के अनुसार आक्षेप का अर्थ निन्दा है। इस प्रकार उपमेय के सौन्दर्य की वृद्धि के लिए उसका निषेध-सा करता हुआ जहाँ कवि उसकी निन्दा करता हो, वहाँ कुन्तक आक्षेप मानेंगे।' अभीष्ट अर्थ के निषेधाभास या निवर्तन की यह धारणा भामह, दण्डी आदि की आक्षेप-धारणा से मिलती-जुलती ही है; पर कुन्तक ने उपमेय के आक्षेप का स्पष्ट उल्लेख कर आक्षेप को औपम्यगर्भ अलङ्कार स्वीकार किया है। वामन के उपमानाक्षेप के विपरीत उपमेयाक्षेप को कुन्तक ने आक्षेप का स्वरूप माना है। ध्यातव्य है कि कुन्तक ने उपमेय के निवर्तन या निषेध को तात्त्विक नहीं मानकर भामह आदि की तरह निषेधाभास ही माना है। ___अग्निपुराणकार ने आक्षेप का दण्डी-कृत लक्षण ही उद्धृत किया है; किन्तु, इसके साथ आक्षेप का अर्थ ध्वनि मानकर श्रुति से अलभ्य अर्थ का ध्वनि से बोधगम्य होने पर बल दिया ।२ आक्षेप और ध्वनि के सूक्ष्म भेद की उपेक्षा कर दोनों को अभिन्न मानना युक्तिसङ्गत नहीं जान पड़ता।
भोज ने दण्डी आदि की तरह 'प्रतिषेधोक्ति' को आक्षेप का प्रधान लक्षण माना तथा विधिमुखेन प्रतिषेधोक्ति और निषेधमुखेन प्रतिषेधोक्ति की धारणा व्यक्त की। दण्डी भी निषेधपर्यवसायी विधि या विधिमुखेन निषेधोक्ति को आक्षेप का एक प्रकार मान चुके थे। भोज की आक्षेप-धारणा पर दण्डी की धारणा का प्रभूत प्रभाव है। ___ मम्मट, रुय्यक आदि आचार्यों ने भामह आदि की तरह विवक्षित अर्थ में१. निषेधच्छाययाक्षेपः कान्तिं प्रथयितु पराम् ।
आक्षेप इति स ज्ञेयः प्रस्तुतस्यैव वस्तुनः । तथा'."प्रकृतस्यैव 'आक्षेपः'
क्षेपकृत् । -कुन्तक, वक्रोक्ति जी० ३,४० तथा वृत्ति पृ० ४७० २. श्र तेरलभ्यमानोऽर्थो यस्मात् भाति सचेतनः। स आक्षेपो ध्वनिः स्यात् च ध्वनिना व्यज्यते यतः ॥
-अग्निपुराण, अध्याय, ३४४" ३. विधिनाथ निषेधेन प्रतिषेधोक्तिरत्र या। शुद्धा मिश्रा च साक्षेपो रोधो नाक्षेपतः पृथक् ।।
-भोज, सरस्वतीकण्ठा० ४,६४