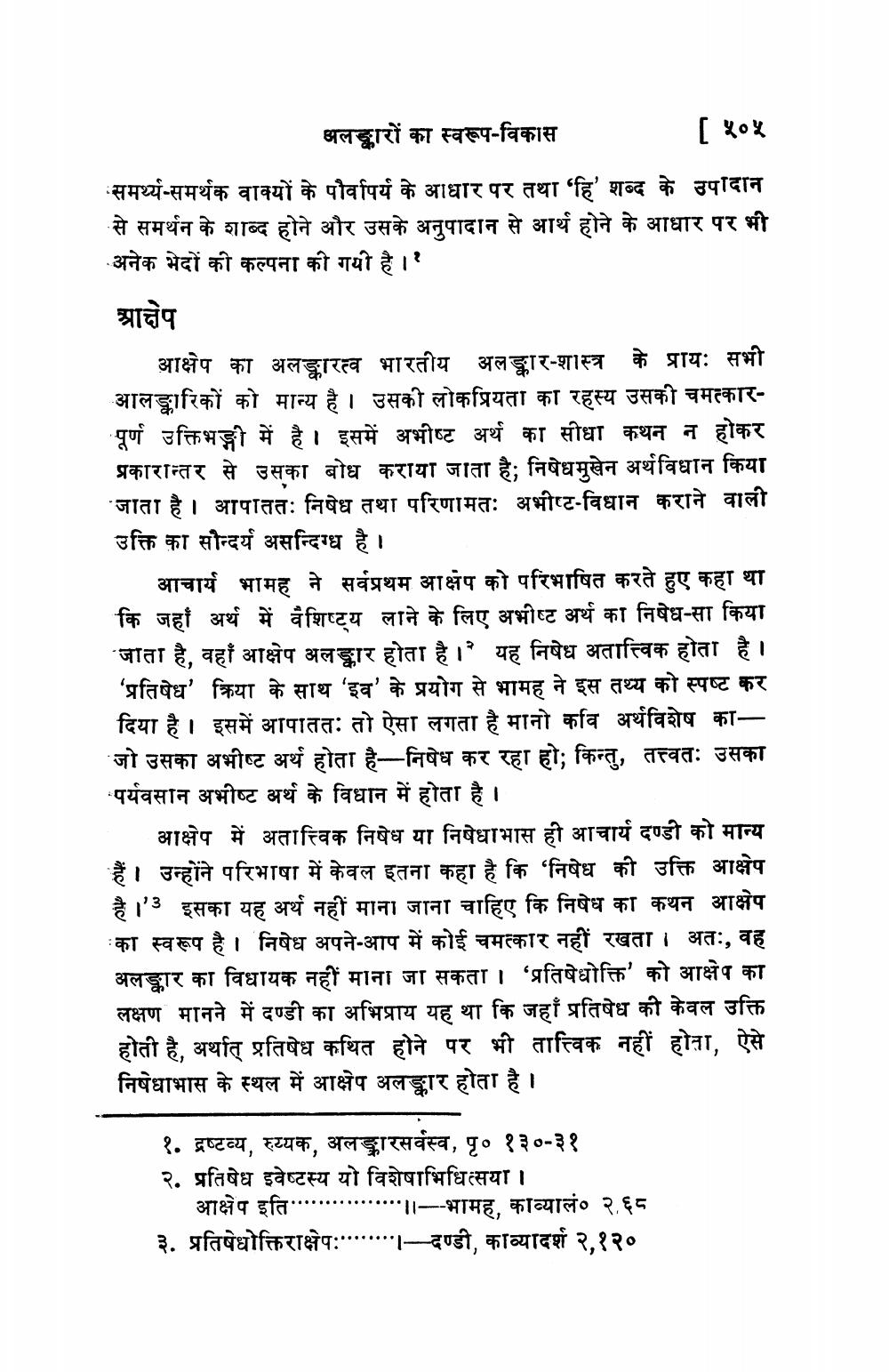________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[५०५
समर्थ्य-समर्थक वाक्यों के पौर्वापर्य के आधार पर तथा 'हि' शब्द के उपादान से समर्थन के शाब्द होने और उसके अनुपादान से आर्थ होने के आधार पर भी अनेक भेदों की कल्पना की गयी है।' आक्षेप
आक्षेप का अलङ्कारत्व भारतीय अलङ्कार-शास्त्र के प्रायः सभी आलङ्कारिकों को मान्य है। उसकी लोकप्रियता का रहस्य उसकी चमत्कारपूर्ण उक्तिभङ्गी में है। इसमें अभीष्ट अर्थ का सीधा कथन न होकर प्रकारान्तर से उसका बोध कराया जाता है; निषेधमुखेन अर्थविधान किया जाता है। आपाततः निषेध तथा परिणामतः अभीष्ट-विधान कराने वाली उक्ति का सौन्दर्य असन्दिग्ध है।
आचार्य भामह ने सर्वप्रथम आक्षेप को परिभाषित करते हुए कहा था कि जहाँ अर्थ में वैशिष्ट्य लाने के लिए अभीष्ट अर्थ का निषेध-सा किया जाता है, वहाँ आक्षेप अलङ्कार होता है। यह निषेध अतात्त्विक होता है। 'प्रतिषेध' क्रिया के साथ 'इव' के प्रयोग से भामह ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है। इसमें आपाततः तो ऐसा लगता है मानो कवि अर्थविशेष काजो उसका अभीष्ट अर्थ होता है-निषेध कर रहा हो; किन्तु, तत्त्वतः उसका पर्यवसान अभीष्ट अर्थ के विधान में होता है ।
__आक्षेप में अतात्त्विक निषेध या निषेधाभास ही आचार्य दण्डी को मान्य हैं। उन्होंने परिभाषा में केवल इतना कहा है कि 'निषेध की उक्ति आक्षेप है।'3 इसका यह अर्थ नहीं माना जाना चाहिए कि निषेध का कथन आक्षेप का स्वरूप है। निषेध अपने-आप में कोई चमत्कार नहीं रखता। अतः, वह अलङ्कार का विधायक नहीं माना जा सकता। 'प्रतिषेधोक्ति' को आक्षेप का लक्षण मानने में दण्डी का अभिप्राय यह था कि जहाँ प्रतिषेध की केवल उक्ति होती है, अर्थात् प्रतिषेध कथित होने पर भी तात्त्विक नहीं होता, ऐसे निषेधाभास के स्थल में आक्षेप अलङ्कार होता है।
१. द्रष्टव्य, रुय्यक, अलङ्कारसर्वस्व, पृ० १३०-३१ २. प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया।
आक्षेप इति.............."||--भामह, काव्यालं० २.६८ ३. प्रतिषेधोक्तिराक्षेपः.......|दण्डी, काव्यादर्श २,१२०