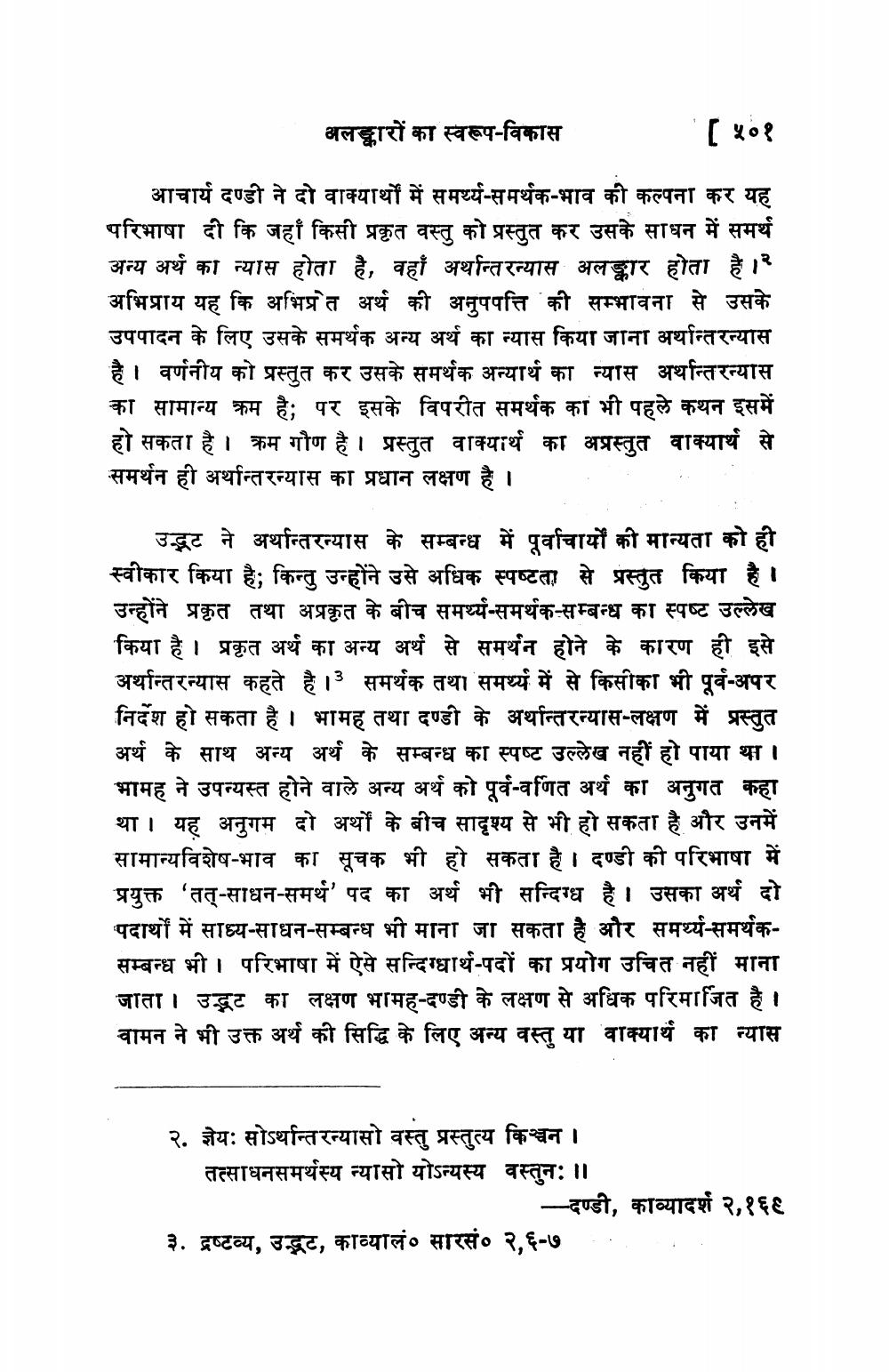________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[५०१
आचार्य दण्डी ने दो वाक्यार्थों में समर्थ्य-समर्थक-भाव की कल्पना कर यह परिभाषा दी कि जहाँ किसी प्रकृत वस्तु को प्रस्तुत कर उसके साधन में समर्थ अन्य अर्थ का न्यास होता है, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार होता है। अभिप्राय यह कि अभिप्रेत अर्थ की अनुपपत्ति की सम्भावना से उसके उपपादन के लिए उसके समर्थक अन्य अर्थ का न्यास किया जाना अर्थान्तरन्यास है। वर्णनीय को प्रस्तुत कर उसके समर्थक अन्यार्थ का न्यास अर्थान्तरन्यास का सामान्य क्रम है; पर इसके विपरीत समर्थक का भी पहले कथन इसमें हो सकता है। क्रम गौण है। प्रस्तुत वाक्यार्थ का अप्रस्तुत वाक्यार्थ से समर्थन ही अर्थान्तरन्यास का प्रधान लक्षण है।
___ उद्भट ने अर्थान्तरन्यास के सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों की मान्यता को ही स्वीकार किया है; किन्तु उन्होंने उसे अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रकृत तथा अप्रकृत के बीच समर्थ्य-समर्थक-सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रकृत अर्थ का अन्य अर्थ से समर्थन होने के कारण ही इसे अर्थान्तरन्यास कहते है। समर्थक तथा समर्थ्य में से किसीका भी पूर्व-अपर निर्देश हो सकता है। भामह तथा दण्डी के अर्थान्तरन्यास-लक्षण में प्रस्तुत अर्थ के साथ अन्य अर्थ के सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो पाया था। भामह ने उपन्यस्त होने वाले अन्य अर्थ को पूर्व-वणित अर्थ का अनुगत कहा था। यह अनुगम दो अर्थों के बीच सादृश्य से भी हो सकता है और उनमें सामान्यविशेष-भाव का सूचक भी हो सकता है। दण्डी की परिभाषा में प्रयुक्त 'तत्-साधन-समर्थ' पद का अर्थ भी सन्दिग्ध है। उसका अर्थ दो पदार्थों में साध्य-साधन-सम्बन्ध भी माना जा सकता है और समर्थ्य-समर्थकसम्बन्ध भी। परिभाषा में ऐसे सन्दिग्धार्थ-पदों का प्रयोग उचित नहीं माना जाता। उद्भट का लक्षण भामह-दण्डी के लक्षण से अधिक परिमार्जित है। वामन ने भी उक्त अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य वस्तु या वाक्यार्थ का न्यास
२. ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ।।
-दण्डी, काव्यादर्श २,१६६ ३. द्रष्टव्य, उद्भट, काव्यालं. सारसं० २,६-७