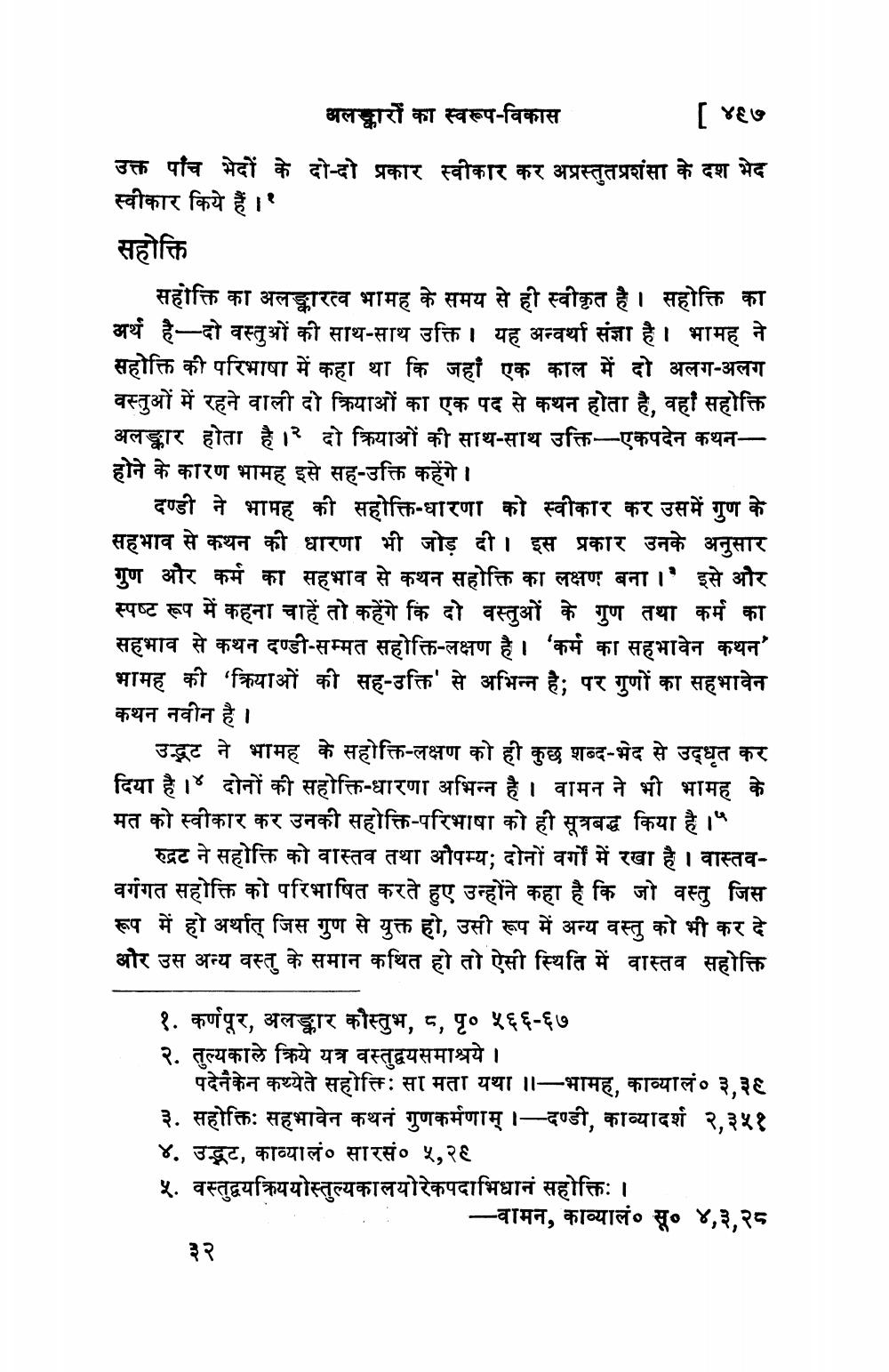________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ४६७
उक्त पाँच भेदों के दो-दो प्रकार स्वीकार कर अप्रस्तुतप्रशंसा के दश भेद स्वीकार किये हैं ।
सहोक्ति
सहोक्ति का अलङ्कारत्व भामह के समय से ही स्वीकृत है । सहोक्ति का अर्थ है - दो वस्तुओं की साथ-साथ उक्ति । यह अन्वर्था संज्ञा है । भामह ने सहोक्ति की परिभाषा में कहा था कि जहाँ एक काल में दो अलग-अलग वस्तुओं में रहने वाली दो क्रियाओं का एक पद से कथन होता है, वहाँ सहोक्ति अलङ्कार होता है । २ दो क्रियाओं की साथ-साथ उक्ति - एकपदेन कथन - होने के कारण भामह इसे सह उक्ति कहेंगे ।
३
दण्डी ने भामह की सहोक्ति-धारणा को स्वीकार कर उसमें गुण के सहभाव से कथन की धारणा भी जोड़ दी। इस प्रकार उनके अनुसार गुण और कर्म का सहभाव से कथन सहोक्ति का लक्षण बना । इसे और स्पष्ट रूप में कहना चाहें तो कहेंगे कि दो वस्तुओं के गुण तथा कर्म का सहभाव से कथन दण्डी - सम्मत सहोक्ति-लक्षण है । 'कर्म का सहभावेन कथन' भामह की 'क्रियाओं की सह-उक्ति से अभिन्न है; पर गुणों का सहभावेन कथन नवीन है ।
उद्भट ने भामह के सहोक्ति-लक्षण को ही कुछ शब्द भेद से उद्धृत कर दिया है । दोनों की सहोक्ति-धारणा अभिन्न है । वामन ने भी भामह के मत को स्वीकार कर उनकी सहोक्ति- परिभाषा को ही सूत्रबद्ध किया है । ५
रुद्रट ने सहोक्ति को वास्तव तथा औपम्य; दोनों वर्गों में रखा है । वास्तव - वर्गगत सहोक्ति को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो वस्तु जिस रूप में हो अर्थात् जिस गुण से युक्त हो, उसी रूप में अन्य वस्तु को भी कर दे और उस अन्य वस्तु के समान कथित हो तो ऐसी स्थिति में वास्तव सहोक्ति
१. कर्णपूर, अलङ्कार कौस्तुभ, ८, पृ० ५६६-६७
२. तुल्यकाले क्रिये यत्र वस्तुद्वयसमाश्रये ।
पथ्ये सहोक्तिः सा मता यथा ॥ - भामह, काव्यालं ० ३,३६ ३. सहोक्तिः सहभावेन कथनं गुणकर्मणाम् । —दण्डी, काव्यादर्श २, ३५१
४. उद्भट, काव्यालं० सारसं० ५,२६
५. वस्तुद्वयक्रिययोस्तुल्यकालयोरेकपदाभिधानं सहोक्तिः ।
३२
— वामन, काव्यालं० सू० ४,३,२८