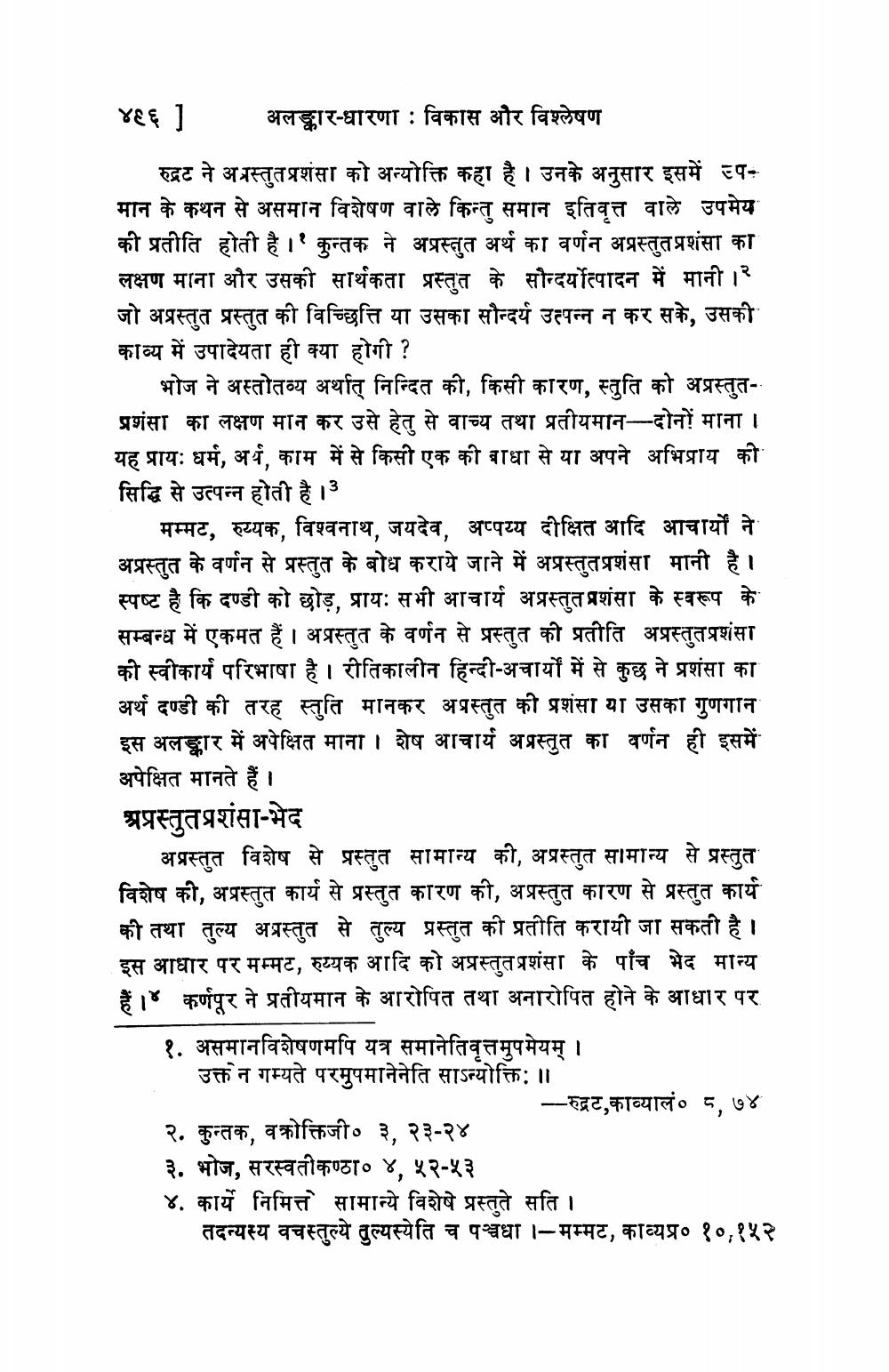________________
४६६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
रुद्रट ने अप्रस्तुतप्रशंसा को अन्योक्ति कहा है। उनके अनुसार इसमें उपमान के कथन से असमान विशेषण वाले किन्तु समान इतिवृत्त वाले उपमेय की प्रतीति होती है । ' कुन्तक ने अप्रस्तुत अर्थ का वर्णन अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण माना और उसकी सार्थकता प्रस्तुत के सौन्दर्योत्पादन में मानी।२ जो अप्रस्तुत प्रस्तुत की विच्छित्ति या उसका सौन्दर्य उत्पन्न न कर सके, उसकी काव्य में उपादेयता ही क्या होगी?
भोज ने अस्तोतव्य अर्थात् निन्दित की, किसी कारण, स्तुति को अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण मान कर उसे हेतु से वाच्य तथा प्रतीयमान-दोनों माना । यह प्रायः धर्म, अर्थ, काम में से किसी एक की बाधा से या अपने अभिप्राय की सिद्धि से उत्पन्न होती है।
मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पय्य दीक्षित आदि आचार्यों ने अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत के बोध कराये जाने में अप्रस्तुतप्रशंसा मानी है। स्पष्ट है कि दण्डी को छोड़, प्रायः सभी आचार्य अप्रस्तुत प्रशंसा के स्वरूप के सम्बन्ध में एकमत हैं । अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत की प्रतीति अप्रस्तुतप्रशंसा को स्वीकार्य परिभाषा है। रीतिकालीन हिन्दी-अचार्यों में से कुछ ने प्रशंसा का अर्थ दण्डी की तरह स्तुति मानकर अप्रस्तुत की प्रशंसा या उसका गुणगान इस अलङ्कार में अपेक्षित माना। शेष आचार्य अप्रस्तुत का वर्णन ही इसमें अपेक्षित मानते हैं। अप्रस्तुतप्रशंसा-भेद
अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य की, अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की, अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की, अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य की तथा तुल्य अप्रस्तुत से तुल्य प्रस्तुत की प्रतीति करायी जा सकती है। इस आधार पर मम्मट, रुय्यक आदि को अप्रस्तुतप्रशंसा के पाँच भेद मान्य हैं। कर्णपूर ने प्रतीयमान के आरोपित तथा अनारोपित होने के आधार पर १. असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवत्तमपमेयम । उक्त न गम्यते परमुपमानेनेति साऽन्योक्तिः ॥
-रुद्रट,काव्यालं० ८, ७४ २. कुन्तक, वक्रोक्तिजी० ३, २३-२४ ३. भोज, सरस्वतीकण्ठा० ४, ५२-५३ ४. कार्ये निमित्त सामान्ये विशेष प्रस्तुते सति ।
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ।- मम्मट, काव्यप्र० १०,१५२