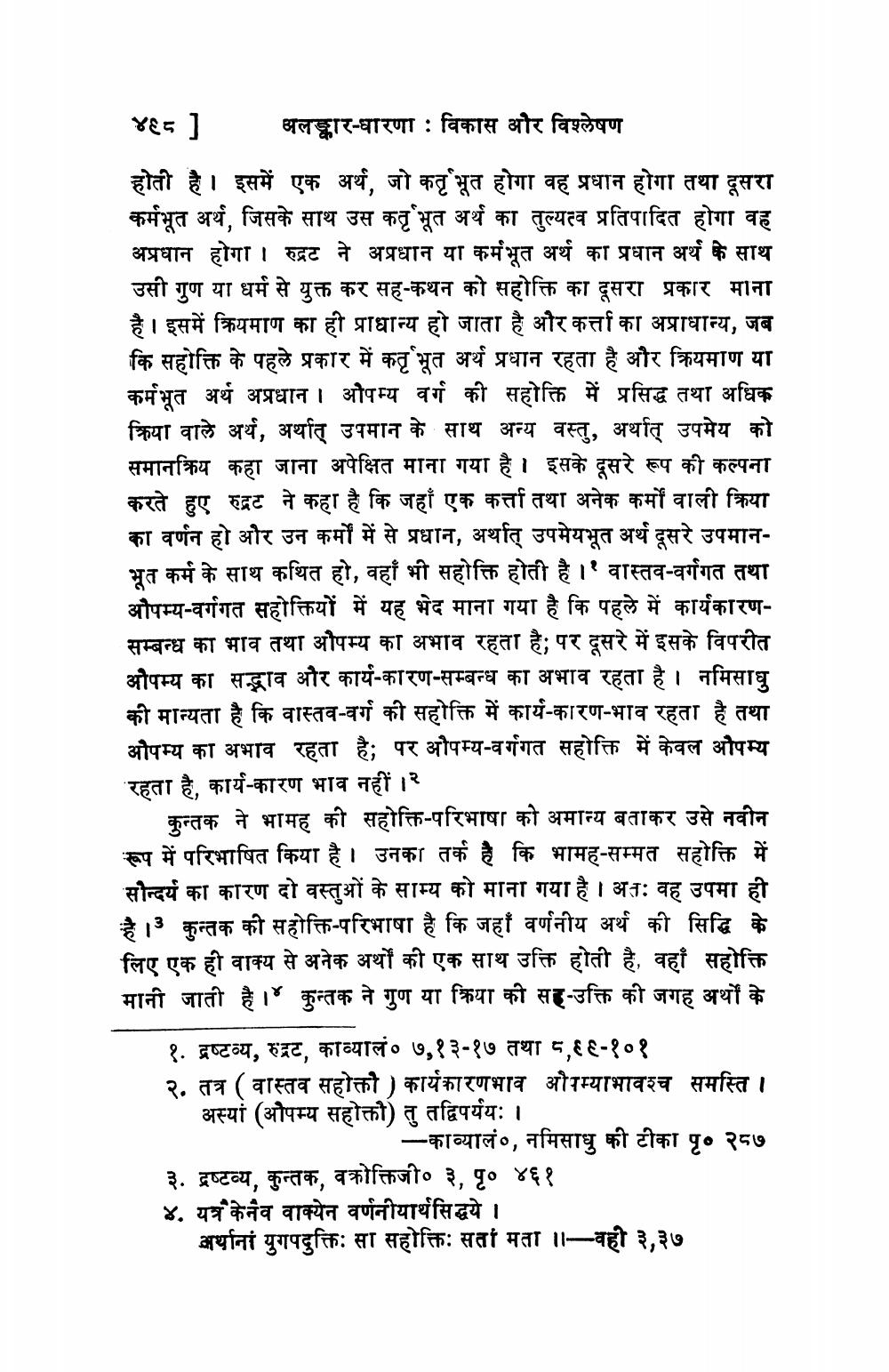________________
४६८ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
होती है । इसमें एक अर्थ, जो कर्तृभूत होगा वह प्रधान होगा तथा दूसरा कर्मभूत अर्थ, जिसके साथ उस कर्तृभूत अर्थ का तुल्यत्व प्रतिपादित होगा वह अप्रधान होगा । रुद्रट ने अप्रधान या कर्मभूत अर्थ का प्रधान अर्थ के साथ उसी गुण या धर्म से युक्त कर सह-कथन को सहोक्ति का दूसरा प्रकार माना है । इसमें क्रियमाण का ही प्राधान्य हो जाता है और कर्त्ता का अप्राधान्य, जब कि सहोक्ति के पहले प्रकार में कर्तृभूत अर्थ प्रधान रहता है और क्रियमाण या कर्मभूत अर्थ अप्रधान । औपम्य वर्ग की सहोक्ति में प्रसिद्ध तथा अधिक क्रिया वाले अर्थ, अर्थात् उपमान के साथ अन्य वस्तु, अर्थात् उपमेय को समानक्रिय कहा जाना अपेक्षित माना गया है । इसके दूसरे रूप की कल्पना करते हुए रुद्रट ने कहा है कि जहाँ एक कर्त्ता तथा अनेक कर्मों वाली क्रिया का वर्णन हो और उन कर्मों में से प्रधान, अर्थात् उपमेयभूत अर्थ दूसरे उपमानभूत कर्म के साथ कथित हो, वहाँ भी सहोक्ति होती है ।' वास्तव वर्गगत तथा औपम्य वर्गगत सहोक्तियों में यह भेद माना गया है कि पहले में कार्यकारणसम्बन्ध का भाव तथा औपम्य का अभाव रहता है; पर दूसरे में इसके विपरीत औपम्य का सद्भाव और कार्य-कारण-सम्बन्ध का अभाव रहता है । नमिसाधु की मान्यता है कि वास्तव वर्ग की सहोक्ति में कार्य-कारण-भाव रहता है तथा औपम्य का अभाव रहता है; पर औपम्य वर्गगत सहोक्ति में केवल औपम्य रहता है, कार्य-कारण भाव नहीं । २
कुन्तक ने भामह की सहोक्ति - परिभाषा को अमान्य बताकर उसे नवीन रूप में परिभाषित किया है । उनका तर्क है कि भामह - सम्मत सहोक्ति में सौन्दर्य का कारण दो वस्तुओं के साम्य को माना गया है । अतः वह उपमा ही है । 3 कुन्तक की सहोक्ति - परिभाषा है कि जहाँ वर्णनीय अर्थ की सिद्धि के लिए एक ही वाक्य से अनेक अर्थों की एक साथ उक्ति होती है, वहाँ सहोक्ति मानी जाती है । कुन्तक ने गुण या क्रिया की सह उक्ति की जगह अर्थों के
१. द्रष्टव्य, रुद्रट, काव्यालं० ७,१३ - १७ तथा ८, ६६-१०१ २. तत्र ( वास्तव सहोक्ती ) कार्यकारणभाव औपम्याभावश्च समस्ति । अस्यां (औपम्य सहोक्ती) तु तद्विपर्ययः ।
- काव्यालं०, नमिसाधु की टीका पृ० २८७
३. द्रष्टव्य, कुन्तक, वक्रोक्तिजी० ३, पृ० ४६१ ४. यत्र केनैव वाक्येन वर्णनीयार्थसिद्धये ।
अर्थानां युगपदुक्तिः सा सहोक्तिः सतां मता ॥ - वही ३,३७
--