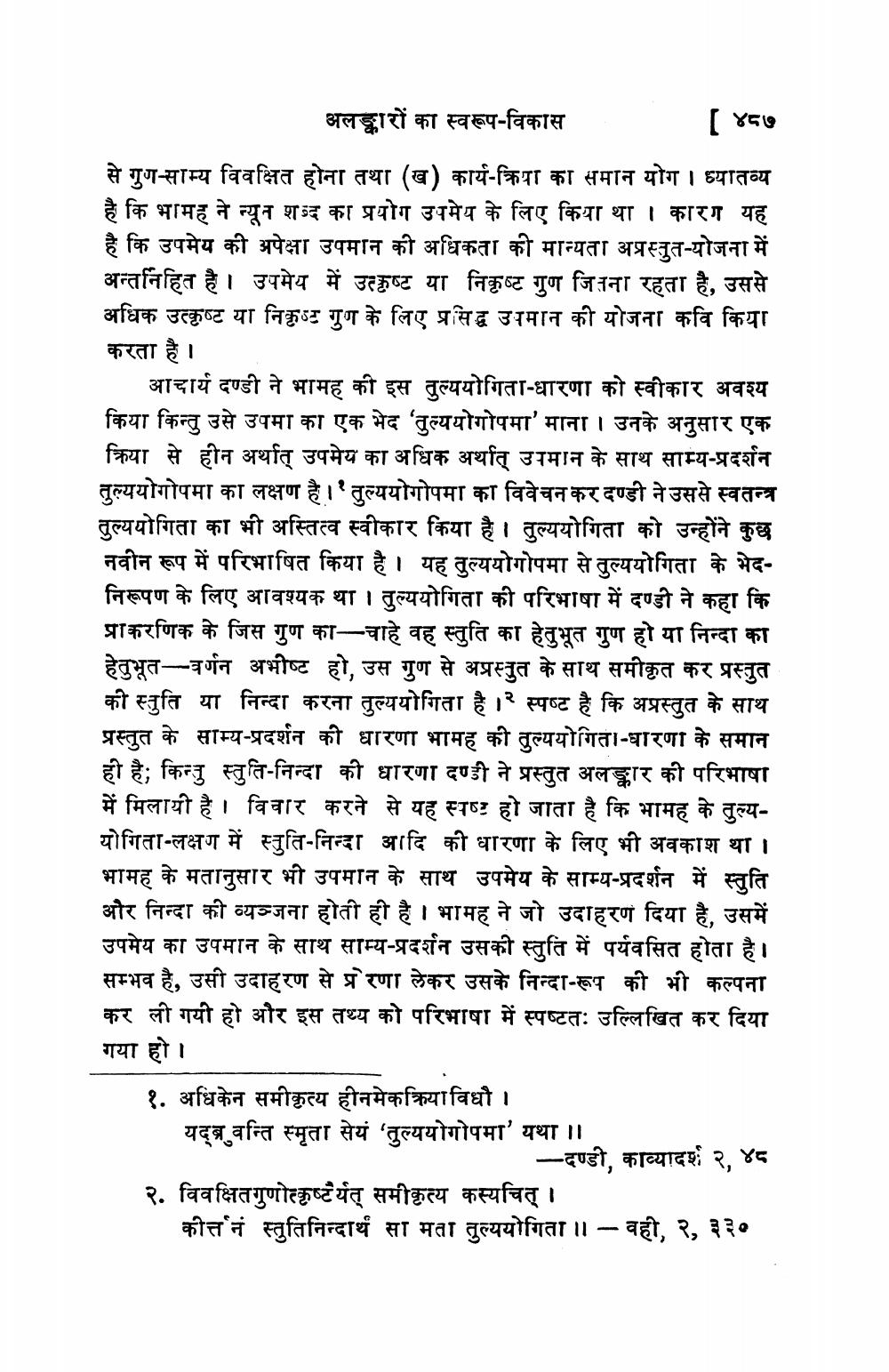________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[४८७ से गुण-साम्य विवक्षित होना तथा (ख) कार्य-क्रिया का समान योग । ध्यातव्य है कि भामह ने न्यून शब्द का प्रयोग उपमेय के लिए किया था । कारग यह है कि उपमेय की अपेक्षा उपमान की अधिकता की मान्यता अप्रस्तुत-योजना में अन्तनिहित है। उपमेय में उत्कृष्ट या निकृष्ट गुण जितना रहता है, उससे अधिक उत्कृष्ट या निकृष्ट गुण के लिए प्रसिद्ध उपमान की योजना कवि किया करता है।
आचार्य दण्डी ने भामह की इस तुल्ययोगिता-धारणा को स्वीकार अवश्य किया किन्तु उसे उपमा का एक भेद 'तुल्ययोगोपमा' माना। उनके अनुसार एक क्रिया से हीन अर्थात् उपमेय का अधिक अर्थात् उपमान के साथ साम्य-प्रदर्शन तुल्ययोगोपमा का लक्षण है। तुल्ययोगोपमा का विवेचन कर दण्डी ने उससे स्वतन्त्र तुल्ययोगिता का भी अस्तित्व स्वीकार किया है। तुल्ययोगिता को उन्होंने कुछ नवीन रूप में परिभाषित किया है। यह तुल्ययोगोपमा से तुल्ययोगिता के भेदनिरूपण के लिए आवश्यक था । तुल्ययोगिता की परिभाषा में दण्डी ने कहा कि प्राकरणिक के जिस गुण का-चाहे वह स्तुति का हेतुभूत गुण हो या निन्दा का हेतुभूत-वर्णन अभीष्ट हो, उस गुण से अप्रस्तुत के साथ समीकृत कर प्रस्तुत की स्तुति या निन्दा करना तुल्ययोगिता है । २ स्पष्ट है कि अप्रस्तुत के साथ प्रस्तुत के साम्य-प्रदर्शन की धारणा भामह की तुल्ययोगिता-धारणा के समान ही है; किन्तु स्तुति-निन्दा की धारणा दण्डी ने प्रस्तुत अलङ्कार की परिभाषा में मिलायी है। विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भामह के तुल्ययोगिता-लक्षण में स्तुति-निन्दा आदि की धारणा के लिए भी अवकाश था। भामह के मतानुसार भी उपमान के साथ उपमेय के साम्य-प्रदर्शन में स्तुति और निन्दा की व्यञ्जना होती ही है । भामह ने जो उदाहरण दिया है, उसमें उपमेय का उपमान के साथ साम्य-प्रदर्शन उसकी स्तुति में पर्यवसित होता है। सम्भव है, उसी उदाहरण से प्रेरणा लेकर उसके निन्दा-रूप की भी कल्पना कर ली गयी हो और इस तथ्य को परिभाषा में स्पष्टतः उल्लिखित कर दिया गया हो। १. अधिकेन समीकृत्य हीनमेकक्रिया विधौ । यद्व वन्ति स्मृता सेयं 'तुल्ययोगोपमा' यथा ।।
-दण्डी, काव्यादर्श २, ४८ २. विवक्षितगुणोत्कृष्टर्यत् समीकृत्य कस्यचित् ।
कीतनं स्तुतिनिन्दार्थं सा मता तुल्ययोगिता ॥ - वही, २, ३३०