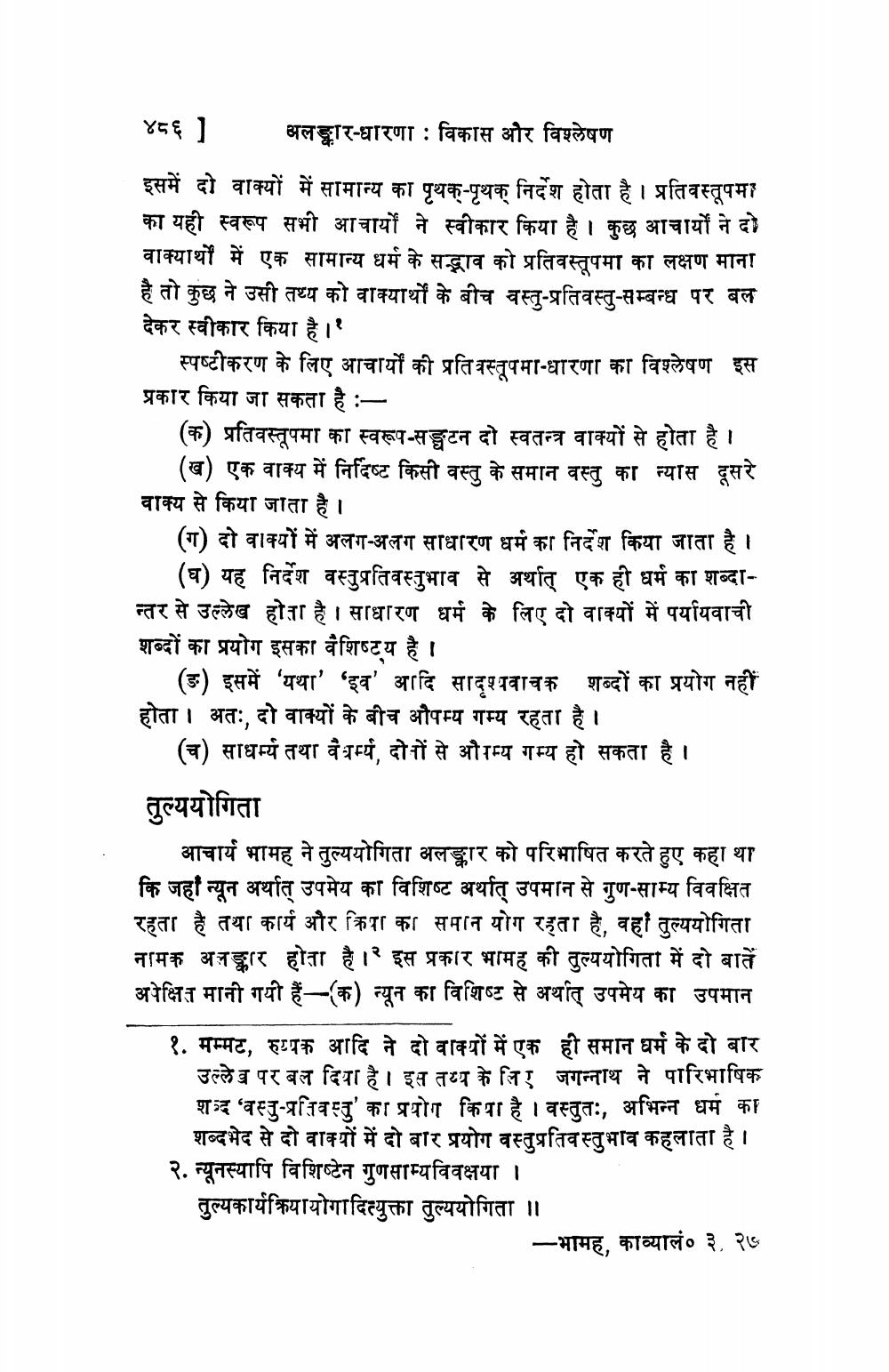________________
४८६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण इसमें दो वाक्यों में सामान्य का पृथक्-पृथक् निर्देश होता है । प्रतिवस्तूपमा का यही स्वरूप सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। कुछ आचार्यों ने दो वाक्यार्थों में एक सामान्य धर्म के सद्भाव को प्रतिवस्तूपमा का लक्षण माना है तो कुछ ने उसी तथ्य को वाक्यार्थों के बीच वस्तु-प्रतिवस्तु-सम्बन्ध पर बल देकर स्वीकार किया है। ___ स्पष्टीकरण के लिए आचार्यों की प्रति वस्तूपमा-धारणा का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है :
(क) प्रतिवस्तूपमा का स्वरूप-सङ्घटन दो स्वतन्त्र वाक्यों से होता है ।
(ख) एक वाक्य में निर्दिष्ट किसी वस्तु के समान वस्तु का न्यास दूसरे वाक्य से किया जाता है।
(ग) दो वाक्यों में अलग-अलग साधारण धर्म का निर्देश किया जाता है ।
(घ) यह निर्देश वस्तुप्रतिवस्तुभाव से अर्थात् एक ही धर्म का शब्दान्तर से उल्लेख होता है । साधारण धर्म के लिए दो वाक्यों में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग इसका वैशिष्ट्य है।
(ङ) इसमें 'यथा' 'इव' आदि सादृश्यवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अतः, दो वाक्यों के बीच औपम्य गम्य रहता है।
(च) साधर्म्य तथा वैधर्म्य, दोनों से औषम्य गम्य हो सकता है। तुल्ययोगिता
आचार्य भामह ने तुल्ययोगिता अलङ्कार को परिभाषित करते हुए कहा था कि जहां न्यून अर्थात् उपमेय का विशिष्ट अर्थात् उपमान से गुण-साम्य विवक्षित रहता है तथा कार्य और क्रिया का समान योग रहता है, वहाँ तुल्ययोगिता नामक अलङ्कार होता है। इस प्रकार भामह की तुल्ययोगिता में दो बातें अपेक्षित मानी गयी हैं—(क) न्यून का विशिष्ट से अर्थात् उपमेय का उपमान १. मम्मट, रुय्यक आदि ने दो वाक्यों में एक ही समान धर्म के दो बार
उल्लेब पर बल दिया है। इस तथ्य के लिए जगन्नाथ ने पारिभाषिक शब्द 'वस्तु-प्रतिवस्तु' का प्रयोग किया है । वस्तुतः, अभिन्न धर्म का
शब्दभेद से दो वाक्यों में दो बार प्रयोग वस्तुप्रतिवस्तुभाव कहलाता है । २. न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया । तुल्यकार्यक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥
-भामह, काव्यालं० ३, २७