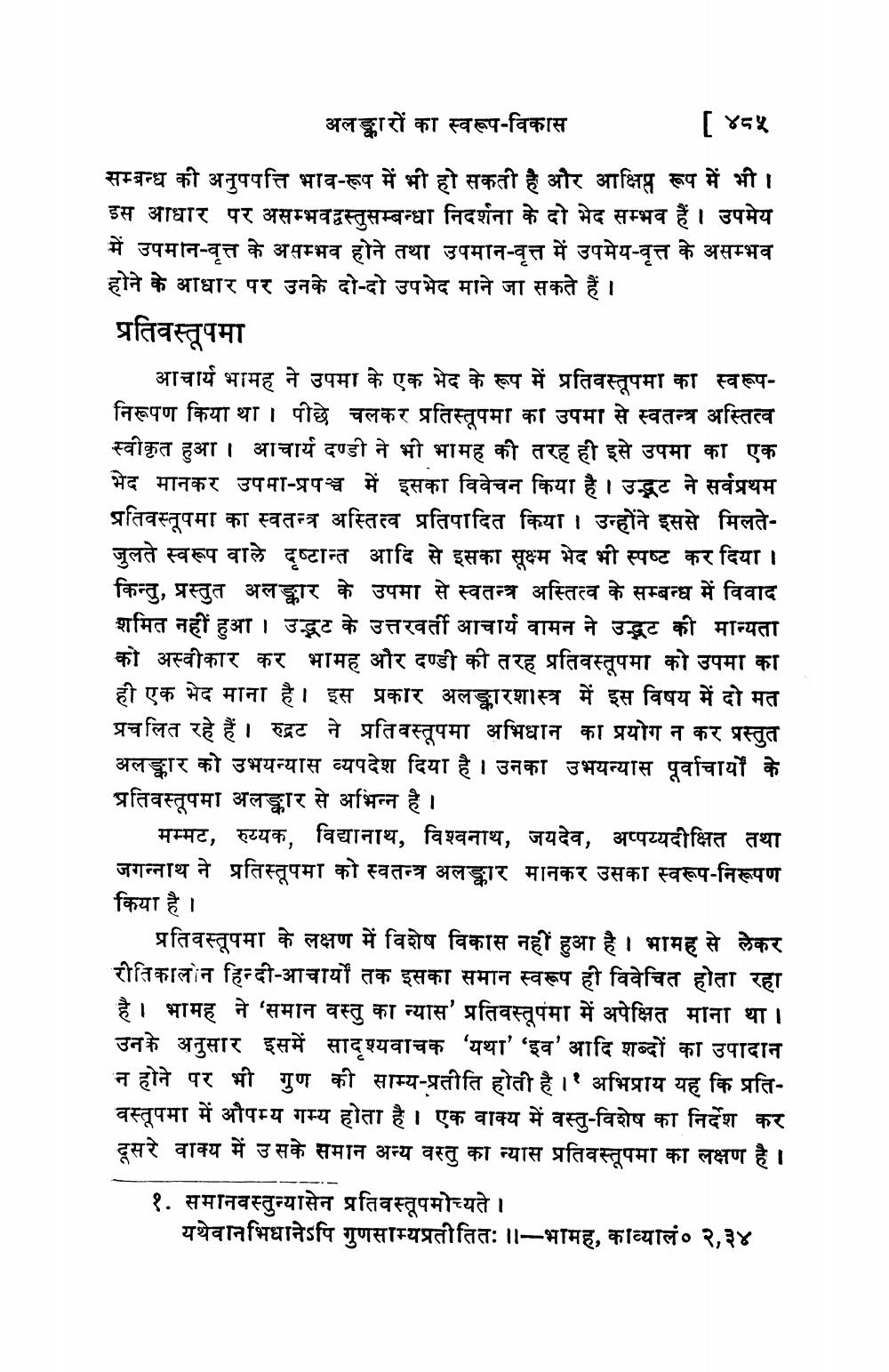________________
अलङ्कारों का स्वरूप - विकास
[ ४८५ सम्बन्ध की अनुपपत्ति भाव-रूप में भी हो सकती है और आक्षिप्त रूप में भी । इस आधार पर असम्भवद्वस्तुसम्बन्धा निदर्शना के दो भेद सम्भव हैं । उपमेय में उपमान-वृत्त के असम्भव होने तथा उपमान-वृत्त में उपमेय-वृत्त के असम्भव होने के आधार पर उनके दो-दो उपभेद माने जा सकते हैं ।
प्रतिवस्तूपमा
आचार्य भामह ने उपमा के एक भेद के रूप में प्रतिवस्तूपमा का स्वरूपनिरूपण किया था । पीछे चलकर प्रतिस्तूपमा का उपमा से स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकृत हुआ । आचार्य दण्डी ने भी भामह की तरह ही इसे उपमा का एक भेद मानकर उपमा-प्रपञ्च में इसका विवेचन किया है । उद्भट ने सर्वप्रथम प्रतिवस्तूपमा का स्वतन्त्र अस्तित्व प्रतिपादित किया । उन्होंने इससे मिलतेजुलते स्वरूप वाले दृष्टान्त आदि से इसका सूक्ष्म भेद भी स्पष्ट कर दिया । किन्तु, प्रस्तुत अलङ्कार के उपमा से स्वतन्त्र अस्तित्व के सम्बन्ध में विवाद शमित नहीं हुआ । उद्भट के उत्तरवर्ती आचार्य वामन ने उद्भट की मान्यता को अस्वीकार कर भामह और दण्डी की तरह प्रतिवस्तूपमा को उपमा का ही एक भेद माना है । इस प्रकार अलङ्कारशास्त्र में इस विषय में दो मत प्रचलित रहे हैं । रुद्रट ने प्रतिवस्तूपमा अभिधान का प्रयोग न कर प्रस्तुत अलङ्कार को उभयन्यास व्यपदेश दिया है । उनका उभयन्यास पूर्वाचार्यों के प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार से अभिन्न है ।
मम्मट, रुय्यक, विद्यानाथ, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पय्यदीक्षित तथा जगन्नाथ ने प्रतिस्तूपमा को स्वतन्त्र अलङ्कार मानकर उसका स्वरूप- निरूपण किया है ।
प्रतिवस्तूपमा के लक्षण में विशेष विकास नहीं हुआ है । भामह से लेकर रीतिकालोन हिन्दी - आचार्यों तक इसका समान स्वरूप ही विवेचित होता रहा है । भामह ने 'समान वस्तु का न्यास' प्रतिवस्तूपमा में अपेक्षित माना था । उनके अनुसार इसमें सादृश्यवाचक 'यथा' 'इव' आदि शब्दों का उपादान न होने पर भी गुण की साम्य प्रतीति होती है ।' अभिप्राय यह कि प्रतिवस्तूपमा में औपम्य गम्य होता है । एक वाक्य में वस्तु- विशेष का निर्देश कर दूसरे वाक्य में उसके समान अन्य वस्तु का न्यास प्रतिवस्तूपमा का लक्षण है ।
१. समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते ।
यथेवानभिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः ॥ - भामह, काव्यालं० २,३४