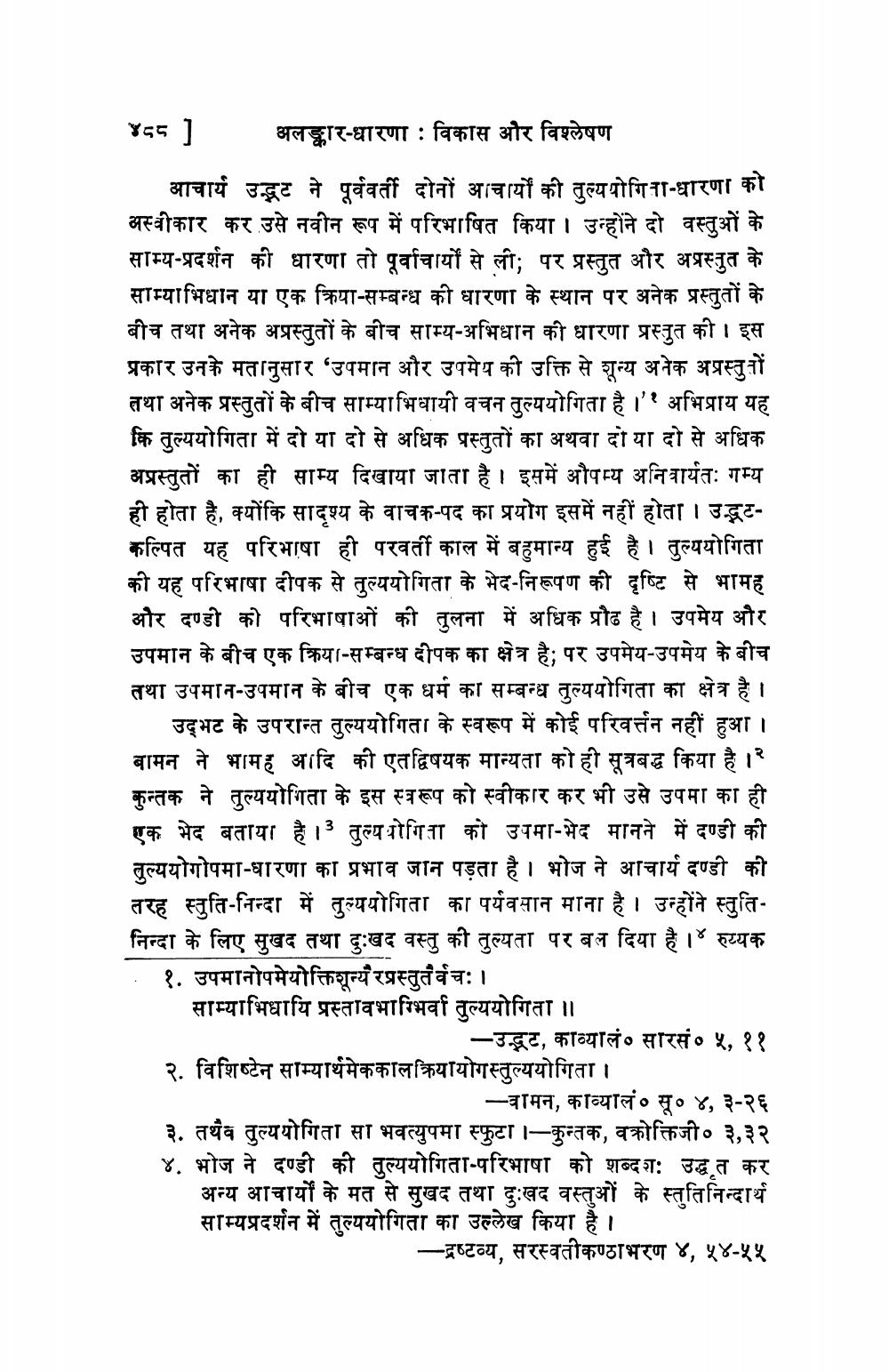________________
४८८ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
आचार्य उद्भट ने पूर्ववर्ती दोनों आचार्यों की तुल्ययोगिता-धारणा को अस्वीकार कर उसे नवीन रूप में परिभाषित किया। उन्होंने दो वस्तुओं के साम्य-प्रदर्शन की धारणा तो पूर्वाचार्यों से ली; पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत के साम्याभिधान या एक क्रिया-सम्बन्ध की धारणा के स्थान पर अनेक प्रस्तुतों के बीच तथा अनेक अप्रस्तुतों के बीच साम्य-अभिधान की धारणा प्रस्तुत की। इस प्रकार उनके मतानुसार 'उपमान और उपमेय की उक्ति से शून्य अनेक अप्रस्तुतों तथा अनेक प्रस्तुतों के बीच साम्याभिधायी वचन तुल्ययोगिता है।'' अभिप्राय यह कि तुल्ययोगिता में दो या दो से अधिक प्रस्तुतों का अथवा दो या दो से अधिक अप्रस्तुतों का ही साम्य दिखाया जाता है। इसमें औपम्य अनिवार्यतः गम्य ही होता है, क्योंकि सादृश्य के वाचक-पद का प्रयोग इस में नहीं होता। उद्भटकल्पित यह परिभाषा ही परवर्ती काल में बहुमान्य हुई है। तुल्ययोगिता की यह परिभाषा दीपक से तुल्ययोगिता के भेद-निरूपण की दृष्टि से भामह और दण्डी को परिभाषाओं की तुलना में अधिक प्रौढ है। उपमेय और उपमान के बीच एक क्रिया-सम्बन्ध दीपक का क्षेत्र है; पर उपमेय-उपमेय के बीच तथा उपमान-उपमान के बीच एक धर्म का सम्बन्ध तुल्ययोगिता का क्षेत्र है।
उद्भट के उपरान्त तुल्ययोगिता के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बामन ने भामह आदि की एतद्विषयक मान्यता को ही सूत्रबद्ध किया है ।२ कुन्तक ने तुल्ययोगिता के इस स्वरूप को स्वीकार कर भी उसे उपमा का ही एक भेद बताया है। तुल्ययोगिता को उपमा-भेद मानने में दण्डी की तुल्ययोगोपमा-धारणा का प्रभाव जान पड़ता है। भोज ने आचार्य दण्डी की तरह स्तुति-निन्दा में तुल्ययोगिता का पर्यवसान माना है। उन्होंने स्तुतिनिन्दा के लिए सुखद तथा दुःखद वस्तु की तुल्यता पर बल दिया है । रुय्यक
१. उपमानोपमेयोक्तिशून्य रप्रस्तुतैर्वचः । __ साम्याभिधायि प्रस्तावभाग्भिर्वा तुल्ययोगिता ॥
-उद्भट, काव्यालं० सारसं० ५, ११ २. विशिष्टेन साम्यार्थमेककाल क्रियायोगस्तुल्ययोगिता।
-वामन, काव्यालं० सू० ४, ३-२६ ३. तथैव तुल्ययोगिता सा भवत्युपमा स्फुटा। कुन्तक, वक्रोक्तिजी० ३,३२ ४. भोज ने दण्डी की तुल्ययोगिता-परिभाषा को शब्दश: उद्धत कर
अन्य आचार्यों के मत से सुखद तथा दुःखद वस्तुओं के स्तुतिनिन्दार्थ साम्यप्रदर्शन में तुल्ययोगिता का उल्लेख किया है।
-द्रष्टव्य, सरस्वतीकण्ठाभरण ४, ५४-५५