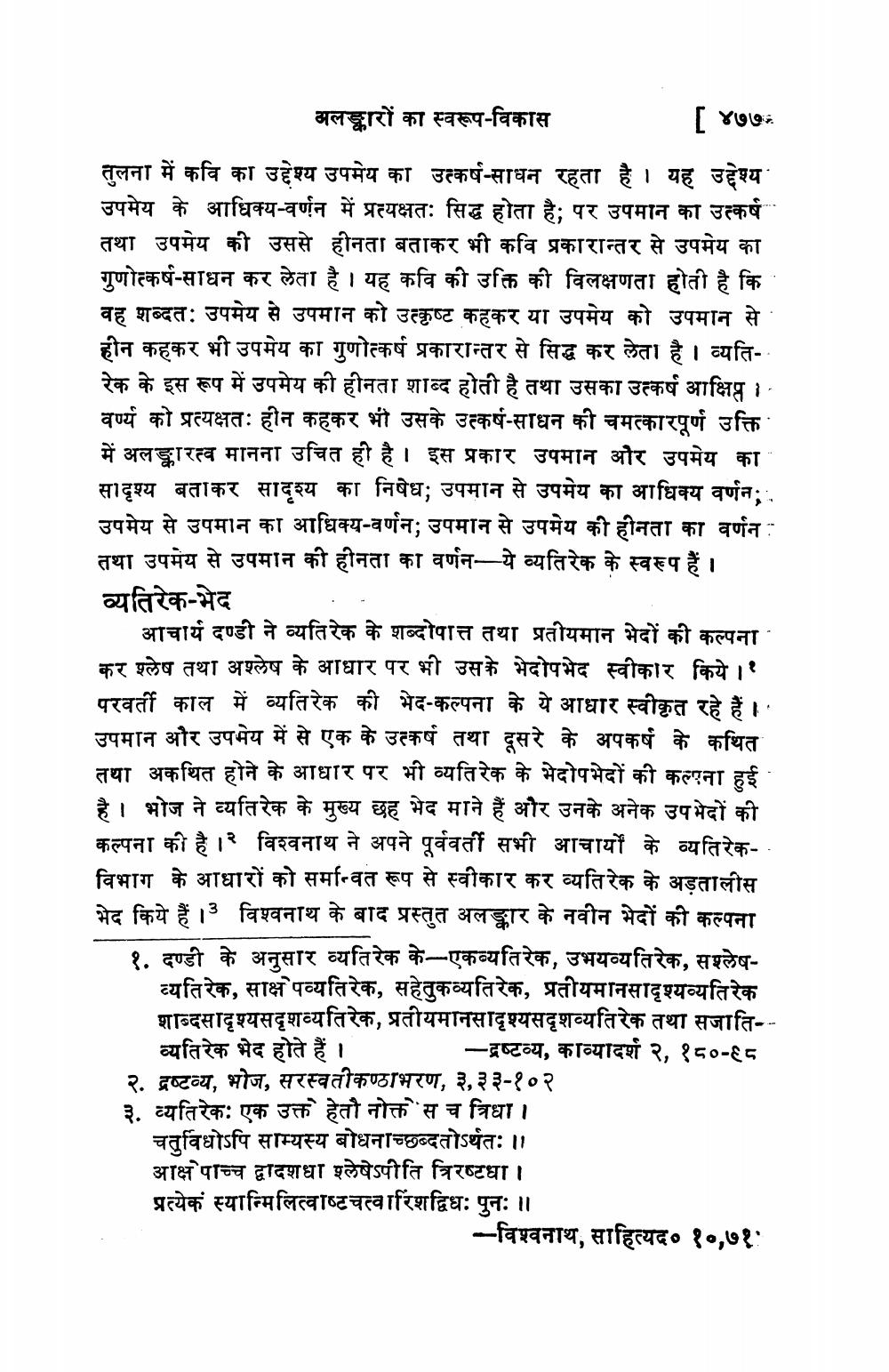________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[४७७
तुलना में कवि का उद्देश्य उपमेय का उत्कर्ष-साधन रहता है । यह उद्देश्य उपमेय के आधिक्य-वर्णन में प्रत्यक्षतः सिद्ध होता है; पर उपमान का उत्कर्ष तथा उपमेय की उससे हीनता बताकर भी कवि प्रकारान्तर से उपमेय का गुणोत्कर्ष-साधन कर लेता है । यह कवि की उक्ति की विलक्षणता होती है कि वह शब्दत: उपमेय से उपमान को उत्कृष्ट कहकर या उपमेय को उपमान से हीन कहकर भी उपमेय का गुणोत्कर्ष प्रकारान्तर से सिद्ध कर लेता है । व्यतिरेक के इस रूप में उपमेय की हीनता शाब्द होती है तथा उसका उत्कर्ष आक्षिप्त । वर्ण्य को प्रत्यक्षतः हीन कहकर भी उसके उत्कर्ष-साधन की चमत्कारपूर्ण उक्ति में अलङ्कारत्व मानना उचित ही है। इस प्रकार उपमान और उपमेय का सादृश्य बताकर सादृश्य का निषेध; उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन;; उपमेय से उपमान का आधिक्य-वर्णन; उपमान से उपमेय की हीनता का वर्णन :: तथा उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन-ये व्यतिरेक के स्वरूप हैं। व्यतिरेक-भेद
आचार्य दण्डी ने व्यतिरेक के शब्दोपात्त तथा प्रतीयमान भेदों की कल्पना कर श्लेष तथा अश्लेष के आधार पर भी उसके भेदोपभेद स्वीकार किये ।। परवर्ती काल में व्यतिरेक की भेद-कल्पना के ये आधार स्वीकृत रहे हैं। उपमान और उपमेय में से एक के उत्कर्ष तथा दूसरे के अपकर्ष के कथित तथा अकथित होने के आधार पर भी व्यतिरेक के भेदोपभेदों की कल्पना हई है। भोज ने व्यतिरेक के मुख्य छह भेद माने हैं और उनके अनेक उपभेदों की कल्पना की है ।२ विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के व्यतिरेकविभाग के आधारों को समन्वित रूप से स्वीकार कर व्यतिरेक के अड़तालीस भेद किये हैं। विश्वनाथ के बाद प्रस्तुत अलङ्कार के नवीन भेदों की कल्पना १. दण्डी के अनुसार व्यतिरेक के-एकव्यतिरेक, उभयव्यतिरेक, सश्लेष
व्यतिरेक, साक्ष पव्यतिरेक, सहेतुकव्यतिरेक, प्रतीयमानसादृश्यव्यतिरेक शाब्दसादृश्यसदृशव्यतिरेक, प्रतीयमानसादृश्यसदृशव्यतिरेक तथा सजातिव्यतिरेक भेद होते हैं ।
-द्रष्टव्य, काव्यादर्श २, १८०-६८ २. द्रष्टव्य, भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण, ३,३३-१०२ ३. व्यतिरेकः एक उक्त हेतौ नोक्त स च त्रिधा।
चतुर्विधोऽपि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतोऽर्थतः ।। आक्षेपाच्च द्वादशधा श्लेषेऽपीति त्रिरष्टधा। प्रत्येकं स्यान्मिलित्वाष्टचत्वारिंशद्विधः पुनः ॥
-विश्वनाथ, साहित्यद० १०,७१'