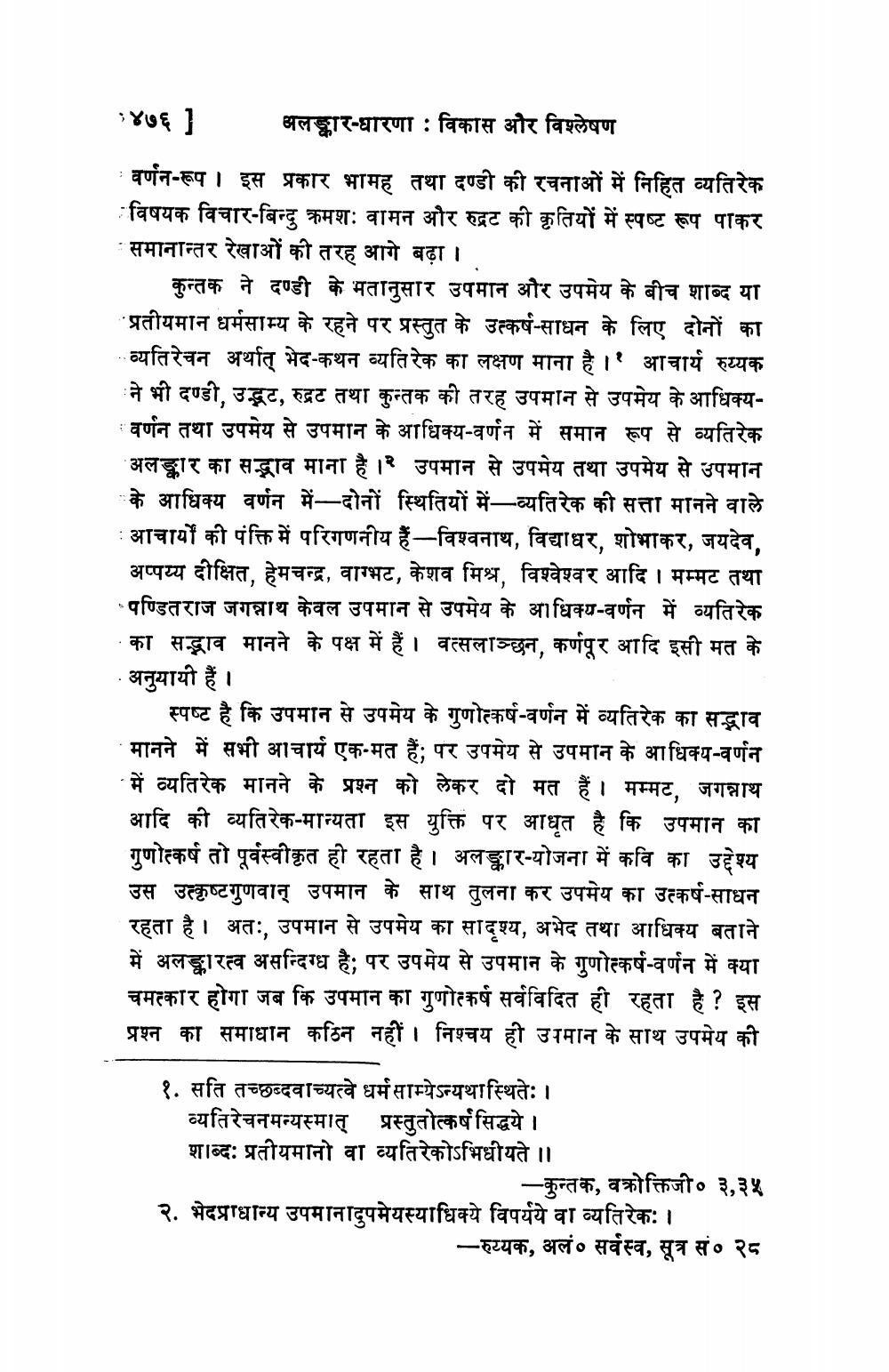________________
४७६ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
वर्णन-रूप । इस प्रकार भामह तथा दण्डी की रचनाओं में निहित व्यतिरेक विषयक विचार-बिन्दु क्रमशः वामन और रुद्रट की कृतियों में स्पष्ट रूप पाकर समानान्तर रेखाओं की तरह आगे बढ़ा।
कुन्तक ने दण्डी के मतानुसार उपमान और उपमेय के बीच शाब्द या 'प्रतीयमान धर्मसाम्य के रहने पर प्रस्तुत के उत्कर्ष-साधन के लिए दोनों का व्यतिरेचन अर्थात् भेद-कथन व्यतिरेक का लक्षण माना है।' आचार्य रुय्यक ने भी दण्डी, उद्भट, रुद्रट तथा कुन्तक की तरह उपमान से उपमेय के आधिक्यवर्णन तथा उपमेय से उपमान के आधिक्य-वर्णन में समान रूप से व्यतिरेक अलङ्कार का सद्भाव माना है ।२ उपमान से उपमेय तथा उपमेय से उपमान के आधिक्य वर्णन में-दोनों स्थितियों में व्यतिरेक की सत्ता मानने वाले : आचार्यों की पंक्ति में परिगणनीय हैं-विश्वनाथ, विद्याधर, शोभाकर, जयदेव, अप्पय्य दीक्षित, हेमचन्द्र, वाग्भट, केशव मिश्र, विश्वेश्वर आदि । मम्मट तथा पण्डितराज जगन्नाथ केवल उपमान से उपमेय के आधिक्य-वर्णन में व्यतिरेक · का सद्भाव मानने के पक्ष में हैं। वत्सलाञ्छन, कर्णपूर आदि इसी मत के . अनुयायी हैं।
स्पष्ट है कि उपमान से उपमेय के गुणोत्कर्ष-वर्णन में व्यतिरेक का सद्भाव मानने में सभी आचार्य एक-मत हैं; पर उपमेय से उपमान के आधिक्य-वर्णन में व्यतिरेक मानने के प्रश्न को लेकर दो मत हैं। मम्मट, जगन्नाथ आदि की व्यतिरेक-मान्यता इस युक्ति पर आधृत है कि उपमान का गुणोत्कर्ष तो पूर्वस्वीकृत ही रहता है। अलङ्कार-योजना में कवि का उद्देश्य उस उत्कृष्टगुणवान् उपमान के साथ तुलना कर उपमेय का उत्कर्ष-साधन रहता है। अतः, उपमान से उपमेय का सादृश्य, अभेद तथा आधिक्य बताने में अलङ्कारत्व असन्दिग्ध है; पर उपमेय से उपमान के गुणोत्कर्ष-वर्णन में क्या चमत्कार होगा जब कि उपमान का गुणोत्कर्ष सर्वविदित ही रहता है ? इस प्रश्न का समाधान कठिन नहीं। निश्चय ही उपमान के साथ उपमेय की
१. सति तच्छब्दवाच्यत्वे धर्म साम्येऽन्यथास्थितेः। व्यतिरेचनमन्यस्मात् प्रस्तुतोत्कर्ष सिद्धये । शाब्दः प्रतीयमानो वा व्यतिरेकोऽभिधीयते ॥
–कुन्तक, वक्रोक्तिजी० ३,३५ २. भेदप्राधान्य उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः ।
-रुय्यक, अलं० सर्वस्व, सूत्र सं० २८