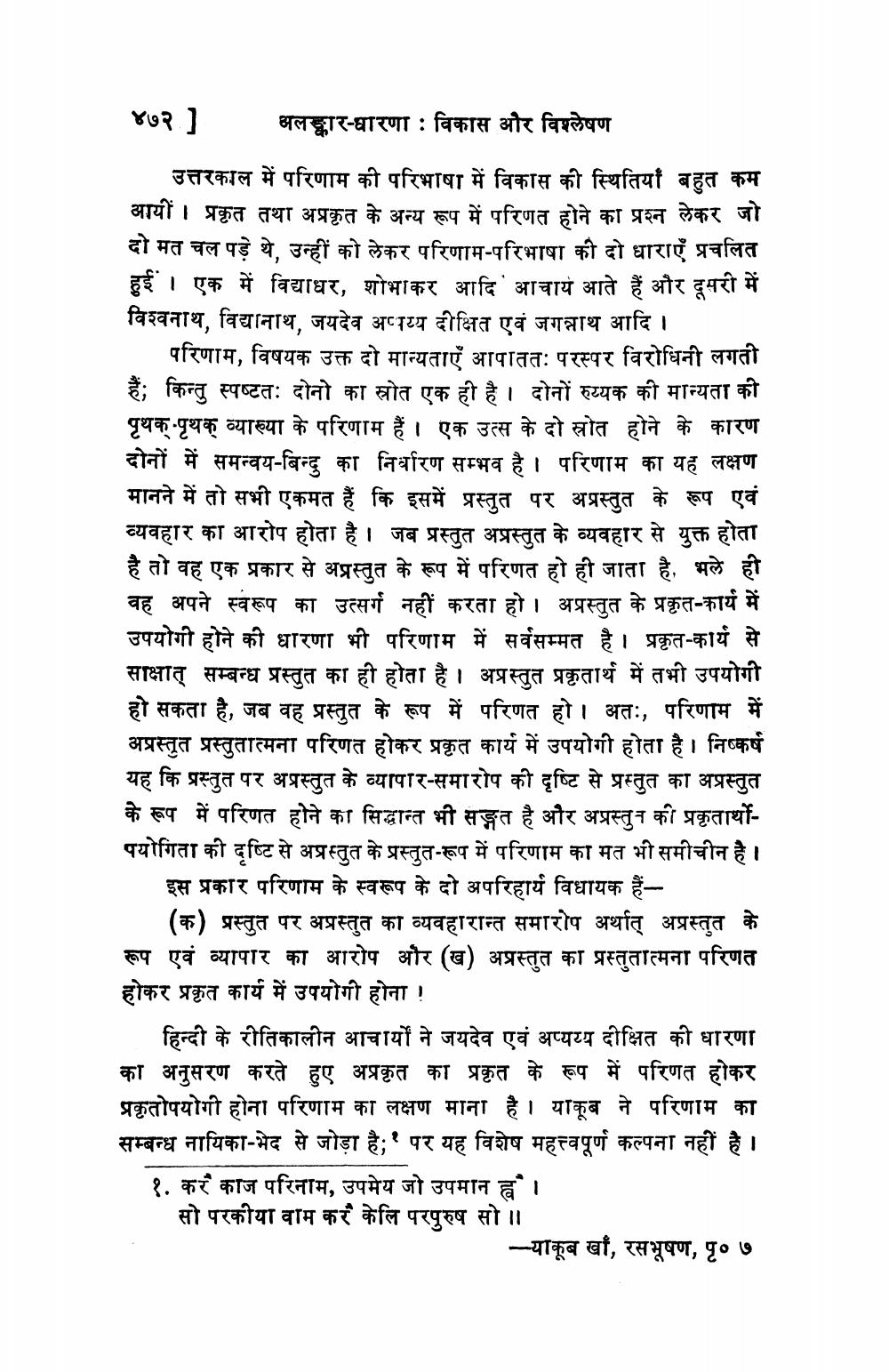________________
४७२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
उत्तरकाल में परिणाम की परिभाषा में विकास की स्थितियाँ बहुत कम आयीं। प्रकृत तथा अप्रकृत के अन्य रूप में परिणत होने का प्रश्न लेकर जो दो मत चल पड़े थे, उन्हीं को लेकर परिणाम-परिभाषा की दो धाराएँ प्रचलित हुई। एक में विद्याधर, शोभाकर आदि आचार्य आते हैं और दूसरी में विश्वनाथ, विद्यानाथ, जयदेव अप्पय्य दीक्षित एवं जगन्नाथ आदि ।
परिणाम, विषयक उक्त दो मान्यताएँ आपाततः परस्पर विरोधिनी लगती हैं; किन्तु स्पष्टतः दोनो का स्रोत एक ही है। दोनों रुय्यक की मान्यता की पृथक्-पृथक् व्याख्या के परिणाम हैं। एक उत्स के दो स्रोत होने के कारण दोनों में समन्वय-बिन्दु का निर्धारण सम्भव है। परिणाम का यह लक्षण मानने में तो सभी एकमत हैं कि इसमें प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के रूप एवं व्यवहार का आरोप होता है। जब प्रस्तुत अप्रस्तुत के व्यवहार से युक्त होता है तो वह एक प्रकार से अप्रस्तुत के रूप में परिणत हो ही जाता है, भले ही वह अपने स्वरूप का उत्सर्ग नहीं करता हो। अप्रस्तुत के प्रकृत-कार्य में उपयोगी होने की धारणा भी परिणाम में सर्वसम्मत है। प्रकृत-कार्य से साक्षात् सम्बन्ध प्रस्तुत का ही होता है। अप्रस्तुत प्रकृतार्थ में तभी उपयोगी हो सकता है, जब वह प्रस्तुत के रूप में परिणत हो। अतः, परिणाम में अप्रस्तुत प्रस्तुतात्मना परिणत होकर प्रकृत कार्य में उपयोगी होता है। निष्कर्ष यह कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के व्यापार-समारोप की दृष्टि से प्रस्तुत का अप्रस्तुत के रूप में परिणत होने का सिद्धान्त भी सङ्गत है और अप्रस्तुत की प्रकृतार्थोंपयोगिता की दृष्टि से अप्रस्तुत के प्रस्तुत-रूप में परिणाम का मत भी समीचीन है।
इस प्रकार परिणाम के स्वरूप के दो अपरिहार्य विधायक हैं
(क) प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का व्यवहारान्त समारोप अर्थात् अप्रस्तुत के रूप एवं व्यापार का आरोप और (ख) अप्रस्तुत का प्रस्तुतात्मना परिणत होकर प्रकृत कार्य में उपयोगी होना ।
हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों ने जयदेव एवं अप्यय्य दीक्षित की धारणा का अनुसरण करते हुए अप्रकृत का प्रकृत के रूप में परिणत होकर प्रकृतोपयोगी होना परिणाम का लक्षण माना है। याकूब ने परिणाम का सम्बन्ध नायिका-भेद से जोड़ा है;' पर यह विशेष महत्त्वपूर्ण कल्पना नहीं है। १. कर काज परिनाम, उपमेय जो उपमान ह्व। सो परकीया वाम कर केलि परपुरुष सो॥
-याकूब खां, रसभूषण, पृ०७