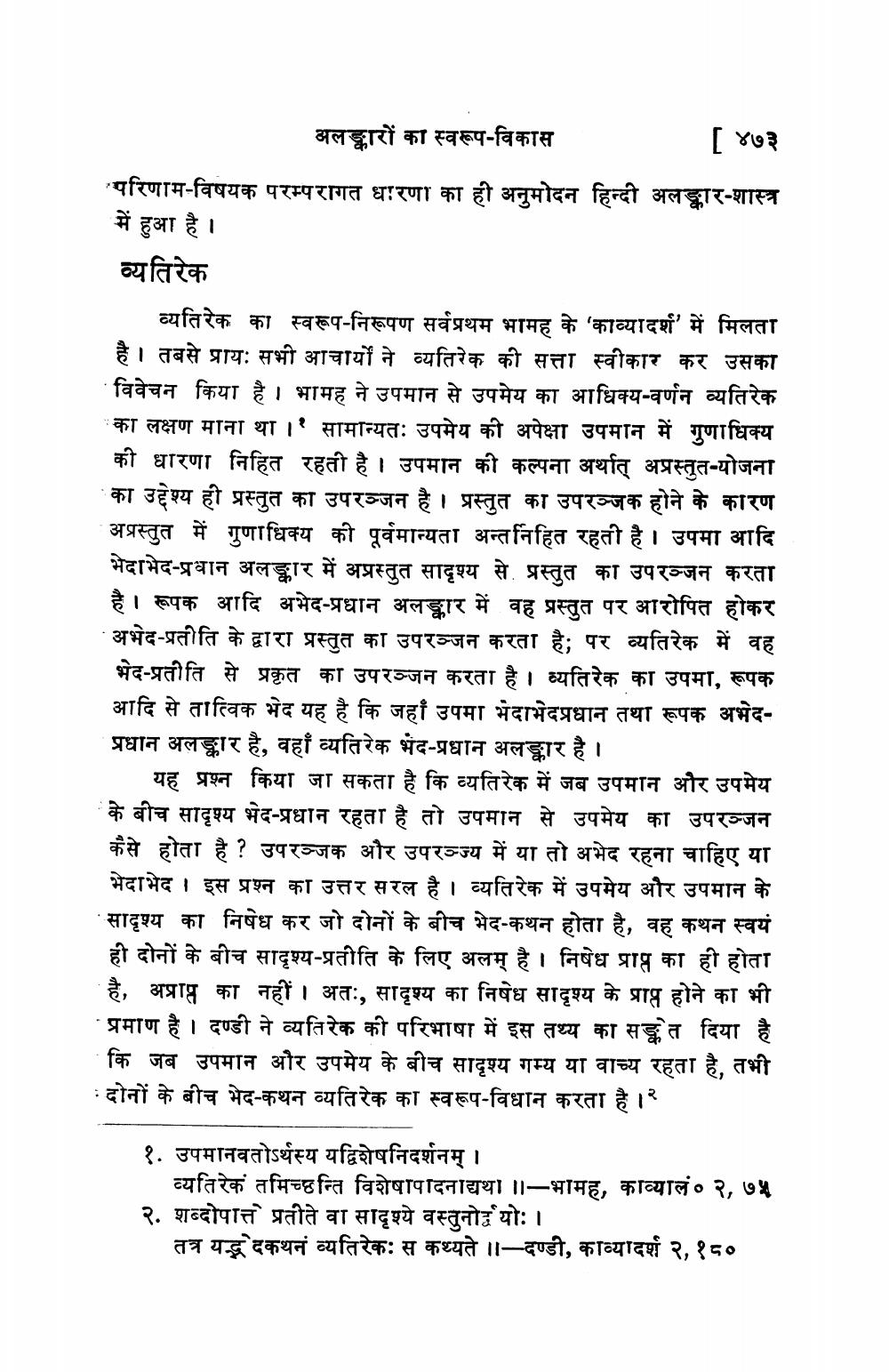________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ४७३ परिणाम-विषयक परम्परागत धारणा का ही अनुमोदन हिन्दी अलङ्कार-शास्त्र में हुआ है। व्यतिरेक
व्यतिरेक का स्वरूप-निरूपण सर्वप्रथम भामह के 'काव्यादर्श' में मिलता है। तबसे प्रायः सभी आचार्यों ने व्यतिरेक की सत्ता स्वीकार कर उसका विवेचन किया है। भामह ने उपमान से उपमेय का आधिक्य-वर्णन व्यतिरेक का लक्षण माना था ।' सामान्यतः उपमेय की अपेक्षा उपमान में गुणाधिक्य की धारणा निहित रहती है। उपमान की कल्पना अर्थात् अप्रस्तुत-योजना का उद्देश्य ही प्रस्तुत का उपरञ्जन है। प्रस्तुत का उपरञ्जक होने के कारण अप्रस्तुत में गुणाधिक्य की पूर्वमान्यता अन्तनिहित रहती है। उपमा आदि भेदाभेद-प्रवान अलङ्कार में अप्रस्तुत सादृश्य से प्रस्तुत का उपरञ्जन करता है। रूपक आदि अभेद-प्रधान अलङ्कार में वह प्रस्तुत पर आरोपित होकर अभेद-प्रतीति के द्वारा प्रस्तुत का उपरञ्जन करता है; पर व्यतिरेक में वह भेद-प्रतीति से प्रकृत का उपरञ्जन करता है। व्यतिरेक का उपमा, रूपक आदि से तात्विक भेद यह है कि जहाँ उपमा भेदाभेदप्रधान तथा रूपक अभेदप्रधान अलङ्कार है, वहाँ व्यतिरेक भंद-प्रधान अलङ्कार है।
यह प्रश्न किया जा सकता है कि व्यतिरेक में जब उपमान और उपमेय के बीच सादृश्य भेद-प्रधान रहता है तो उपमान से उपमेय का उपरञ्जन कैसे होता है ? उपरञ्जक और उपरञ्ज्य में या तो अभेद रहना चाहिए या भेदाभेद । इस प्रश्न का उत्तर सरल है। व्यतिरेक में उपमेय और उपमान के सादृश्य का निषेध कर जो दोनों के बीच भेद-कथन होता है, वह कथन स्वयं ही दोनों के बीच सादृश्य-प्रतीति के लिए अलम् है। निषेध प्राप्त का ही होता है, अप्राप्त का नहीं। अतः, सादृश्य का निषेध सादृश्य के प्राप्त होने का भी प्रमाण है । दण्डी ने व्यतिरेक की परिभाषा में इस तथ्य का सङ्कत दिया है कि जब उपमान और उपमेय के बीच सादृश्य गम्य या वाच्य रहता है, तभी दोनों के बीच भेद-कथन व्यतिरेक का स्वरूप-विधान करता है।
१. उपमानवतोऽर्थस्य यद्विशेषनिदर्शनम् ।
व्यतिरेक तमिच्छन्ति विशेषापादनाद्यथा ॥–भामह, काव्यालं० २, ७५ २. शब्दोपात्त प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनोई योः।
तत्र यद्भ दकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥-दण्डी, काव्यादर्श २,१८०