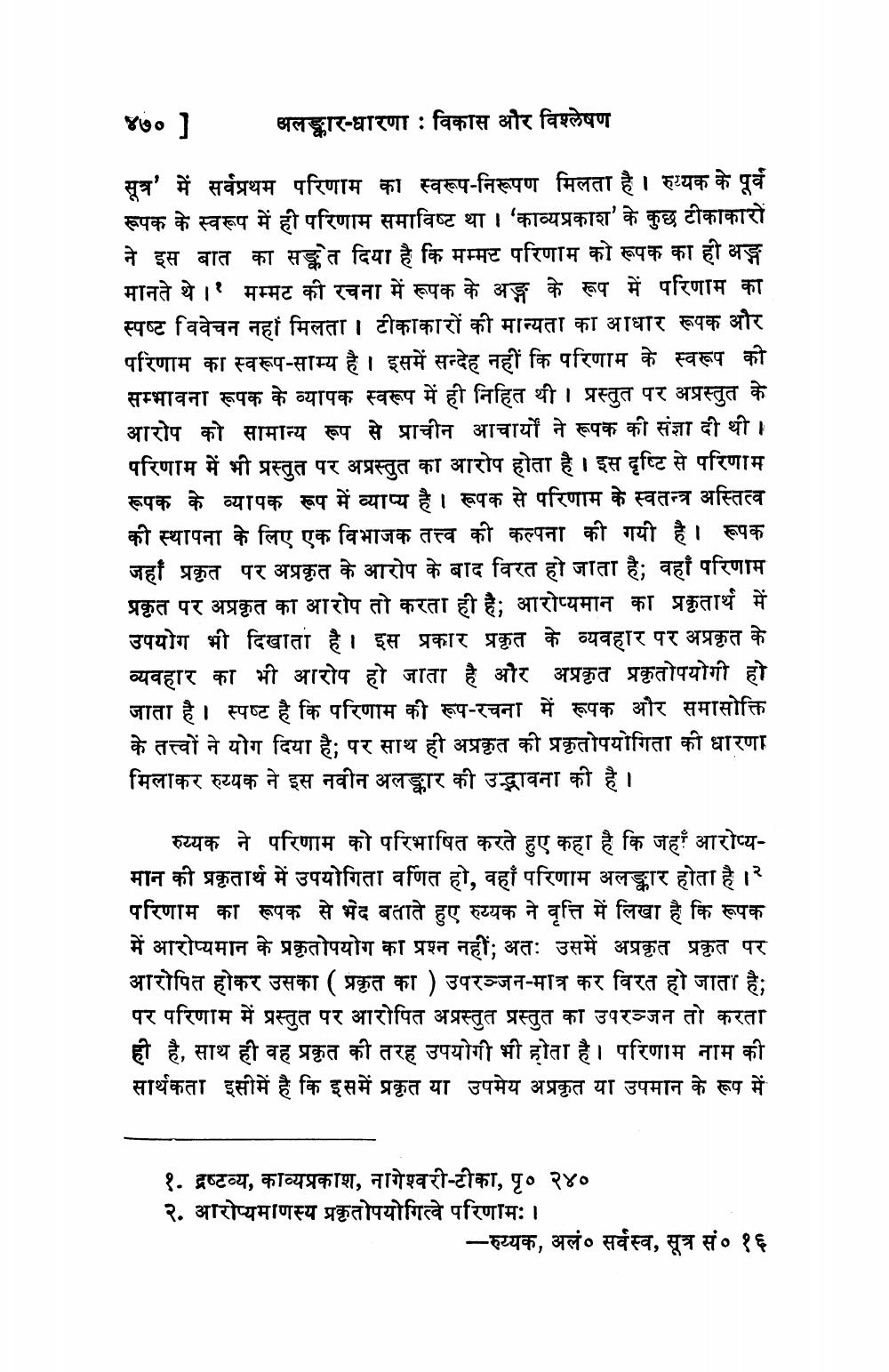________________
४७० ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
सूत्र' में सर्वप्रथम परिणाम का स्वरूप-निरूपण मिलता है। रुय्यक के पूर्व रूपक के स्वरूप में ही परिणाम समाविष्ट था । 'काव्यप्रकाश' के कुछ टीकाकारों ने इस बात का सङ्केत दिया है कि मम्मट परिणाम को रूपक का ही अङ्ग मानते थे। मम्मट की रचना में रूपक के अङ्ग के रूप में परिणाम का स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता। टीकाकारों की मान्यता का आधार रूपक और परिणाम का स्वरूप-साम्य है। इसमें सन्देह नहीं कि परिणाम के स्वरूप को सम्भावना रूपक के व्यापक स्वरूप में ही निहित थी। प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के आरोप को सामान्य रूप से प्राचीन आचार्यों ने रूपक की संज्ञा दी थी। परिणाम में भी प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप होता है । इस दृष्टि से परिणाम रूपक के व्यापक रूप में व्याप्य है। रूपक से परिणाम के स्वतन्त्र अस्तित्व की स्थापना के लिए एक विभाजक तत्त्व की कल्पना की गयी है। रूपक जहां प्रकृत पर अप्रकृत के आरोप के बाद विरत हो जाता है; वहाँ परिणाम प्रकृत पर अप्रकृत का आरोप तो करता ही है; आरोप्यमान का प्रकृतार्थ में उपयोग भी दिखाता है। इस प्रकार प्रकृत के व्यवहार पर अप्रकृत के व्यवहार का भी आरोप हो जाता है और अप्रकृत प्रकृतोपयोगी हो जाता है। स्पष्ट है कि परिणाम की रूप-रचना में रूपक और समासोक्ति के तत्त्वों ने योग दिया है; पर साथ ही अप्रकृत की प्रकृतोपयोगिता की धारणा मिलाकर रुय्यक ने इस नवीन अलङ्कार की उद्भावना की है।
रुय्यक ने परिणाम को परिभाषित करते हुए कहा है कि जहाँ आरोप्यमान की प्रकृतार्थ में उपयोगिता वणित हो, वहाँ परिणाम अलङ्कार होता है ।। परिणाम का रूपक से भेद बताते हुए रुय्यक ने वृत्ति में लिखा है कि रूपक में आरोप्यमान के प्रकृतोपयोग का प्रश्न नहीं; अतः उसमें अप्रकृत प्रकृत पर आरोपित होकर उसका (प्रकृत का ) उपरञ्जन-मात्र कर विरत हो जाता है; पर परिणाम में प्रस्तुत पर आरोपित अप्रस्तुत प्रस्तुत का उपरञ्जन तो करता ही है, साथ ही वह प्रकृत की तरह उपयोगी भी होता है। परिणाम नाम की सार्थकता इसीमें है कि इसमें प्रकृत या उपमेय अप्रकृत या उपमान के रूप में
१. द्रष्टव्य, काव्यप्रकाश, नागेश्वरी-टीका, पृ० २४० २. आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः।
-रुय्यक, अलं० सर्वस्व, सूत्र सं० १६