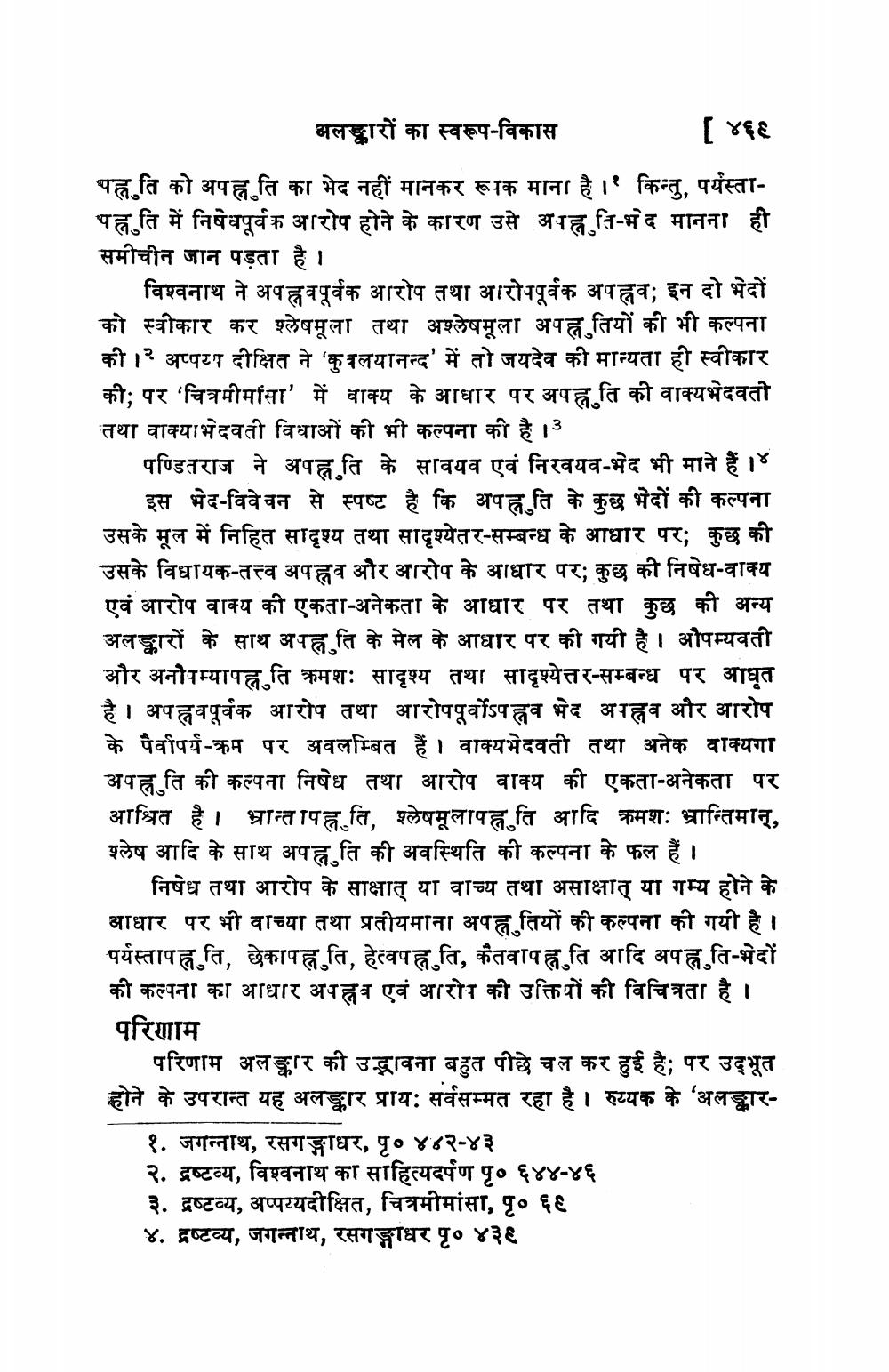________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ४६६ पह्नति को अपह्नति का भेद नहीं मानकर रूपक माना है।' किन्तु, पर्यस्तापह्नति में निषेवपूर्वक आरोप होने के कारण उसे अपह्नति-भेद मानना ही समीचीन जान पड़ता है।
विश्वनाथ ने अपह्नवपूर्वक आरोप तथा आरोपपूर्वक अपह्नव; इन दो भेदों को स्वीकार कर श्लेषमूला तथा अश्लेषमूला अपह्न तियों की भी कल्पना की। अप्पय्ण दीक्षित ने 'कुवलयानन्द' में तो जयदेव की मान्यता ही स्वीकार की; पर 'चित्रमीमांसा' में वाक्य के आधार पर अपह्न ति की वाक्यभेदवती तथा वाक्याभेदवती विधाओं की भी कल्पना की है।
पण्डितराज ने अपह्न ति के सावयव एवं निरवयव-भेद भी माने हैं।
इस भेद-विवेचन से स्पष्ट है कि अपह्नति के कुछ भेदों की कल्पना उसके मूल में निहित सादृश्य तथा सादृश्येतर-सम्बन्ध के आधार पर; कुछ की उसके विधायक-तत्त्व अपह्नव और आरोप के आधार पर; कुछ की निषेध-वाक्य एवं आरोप वाक्य की एकता-अनेकता के आधार पर तथा कुछ की अन्य अलङ्कारों के साथ अपह्नति के मेल के आधार पर की गयी है। औपम्यवती और अनौपम्यापह्न ति क्रमशः सादृश्य तथा सादृश्येत्तर-सम्बन्ध पर आधृत है। अपह्नवपूर्वक आरोप तथा आरोपपूर्वोऽपह्नव भेद आह्नव और आरोप के पैर्वीपर्य-क्रम पर अवलम्बित हैं। वाक्यभेदवती तथा अनेक वाक्यगा अपह्न ति की कल्पना निषेध तथा आरोप वाक्य की एकता-अनेकता पर आश्रित है। भ्रान्तापह्न, ति, श्लेषमूलापह्न ति आदि क्रमशः भ्रान्तिमान्, श्लेष आदि के साथ अपह्नति की अवस्थिति की कल्पना के फल हैं।
निषेध तथा आरोप के साक्षात् या वाच्य तथा असाक्षात् या गम्य होने के आधार पर भी वाच्या तथा प्रतीयमाना अपह्न तियों की कल्पना की गयी है। पर्यस्तापह्नति, छेकापह्न ति, हेत्वपह्नति, कैतवापह्नति आदि अपह्न ति-भेदों की कल्पना का आधार अपह्नव एवं आरोष की उक्तियों की विचित्रता है । परिणाम
परिणाम अलङ्कार की उद्भावना बहुत पीछे चल कर हुई है; पर उद्भूत होने के उपरान्त यह अलङ्कार प्रायः सर्वसम्मत रहा है। रुय्यक के 'अलङ्कार
१. जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ०४४२-४३ २. द्रष्टव्य, विश्वनाथ का साहित्यदर्पण पृ० ६४४-४६ ३. द्रष्टव्य, अप्पय्यदीक्षित, चित्रमीमांसा, पृ० ६६ ४. द्रष्टव्य, जगन्नाथ, रसगङ्गाधर पृ० ४३६