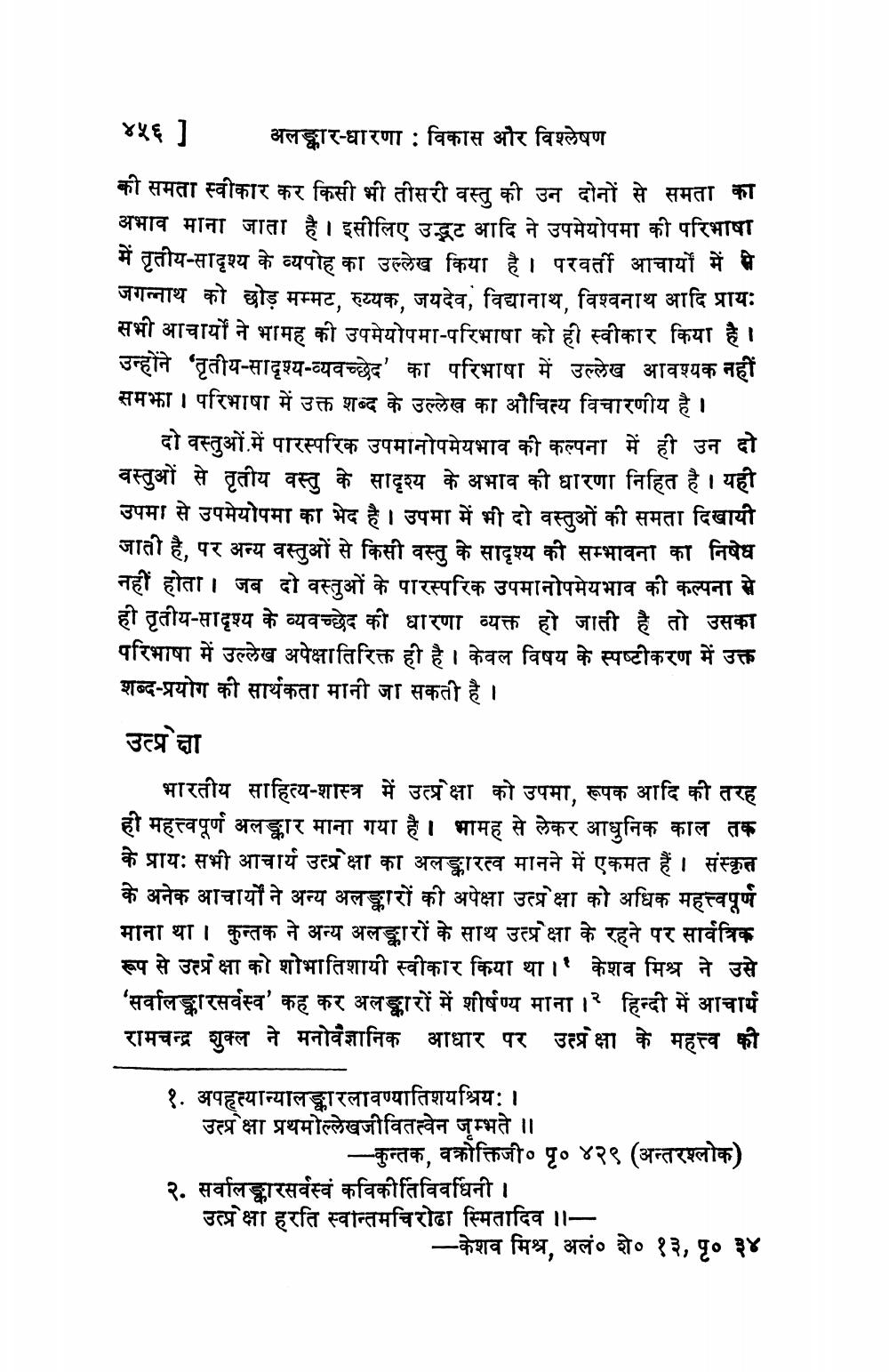________________
४५६ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
की समता स्वीकार कर किसी भी तीसरी वस्तु की उन दोनों से समता का अभाव माना जाता है । इसीलिए उद्भट आदि ने उपमेयोपमा की परिभाषा में तृतीय-सादृश्य के व्यपोह का उल्लेख किया है । परवर्ती आचार्यों में से जगन्नाथ को छोड़ मम्मट, रुय्यक, जयदेव, विद्यानाथ, विश्वनाथ आदि प्रायः सभी आचार्यों ने भामह की उपमेयोपमा - परिभाषा को ही स्वीकार किया है । उन्होंने 'तृतीय - सादृश्य-व्यवच्छेद' का परिभाषा में उल्लेख आवश्यक नहीं समझा । परिभाषा में उक्त शब्द के उल्लेख का औचित्य विचारणीय है ।
दो वस्तुओं में पारस्परिक उपमानोपमेयभाव की कल्पना में ही उन दो वस्तुओं से तृतीय वस्तु के सादृश्य के अभाव की धारणा निहित है । यही उपमा से उपमेयोपमा का भेद है । उपमा में भी दो वस्तुओं की समता दिखायी जाती है, पर अन्य वस्तुओं से किसी वस्तु के सादृश्य की सम्भावना का निषेध नहीं होता । जब दो वस्तुओं के पारस्परिक उपमानोपमेयभाव की कल्पना से ही तृतीय - सादृश्य के व्यवच्छेद की धारणा व्यक्त हो जाती है तो उसका परिभाषा में उल्लेख अपेक्षातिरिक्त ही है । केवल विषय के स्पष्टीकरण में उक्त शब्द-प्रयोग की सार्थकता मानी जा सकती है ।
उत्प्रेक्षा
भारतीय साहित्य - शास्त्र में उत्प्रेक्षा को उपमा, रूपक आदि की तरह ही महत्त्वपूर्ण अलङ्कार माना गया है । भामह से लेकर आधुनिक काल तक के प्रायः सभी आचार्य उत्प्र ेक्षा का अलङ्कारत्व मानने में एकमत हैं । संस्कृत के अनेक आचार्यों ने अन्य अलङ्कारों की अपेक्षा उत्प्र ेक्षा को अधिक महत्त्वपूर्ण माना था । कुन्तक ने अन्य अलङ्कारों के साथ उत्प्र ेक्षा के रहने पर सार्वत्रिक रूप से उत्प्रेक्षा को शोभातिशायी स्वीकार किया था । केशव मिश्र ने उसे 'सर्वालङ्कारसर्वस्व' कह कर अलङ्कारों में शीर्षण्य माना । २ हिन्दी में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक आधार पर उत्प्रेक्षा के महत्त्व की
१
१. अपहृत्यान्यालङ्कारलावण्यातिशयश्रियः । उत्प्र ेक्षा प्रथमोल्लेखजीवितत्वेन जृम्भते ॥
—कुन्तक, वक्रोक्तिजी० पृ० ४२९ ( अन्तरश्लोक ) २. सर्वालङ्कारसर्वस्वं कविकीर्तिविवर्धिनी ।
उत्प्रेक्षा हरति स्वान्तमचिरोढा स्मितादिव ॥
- केशव मिश्र, अलं० शे० १३, पृ० ३४