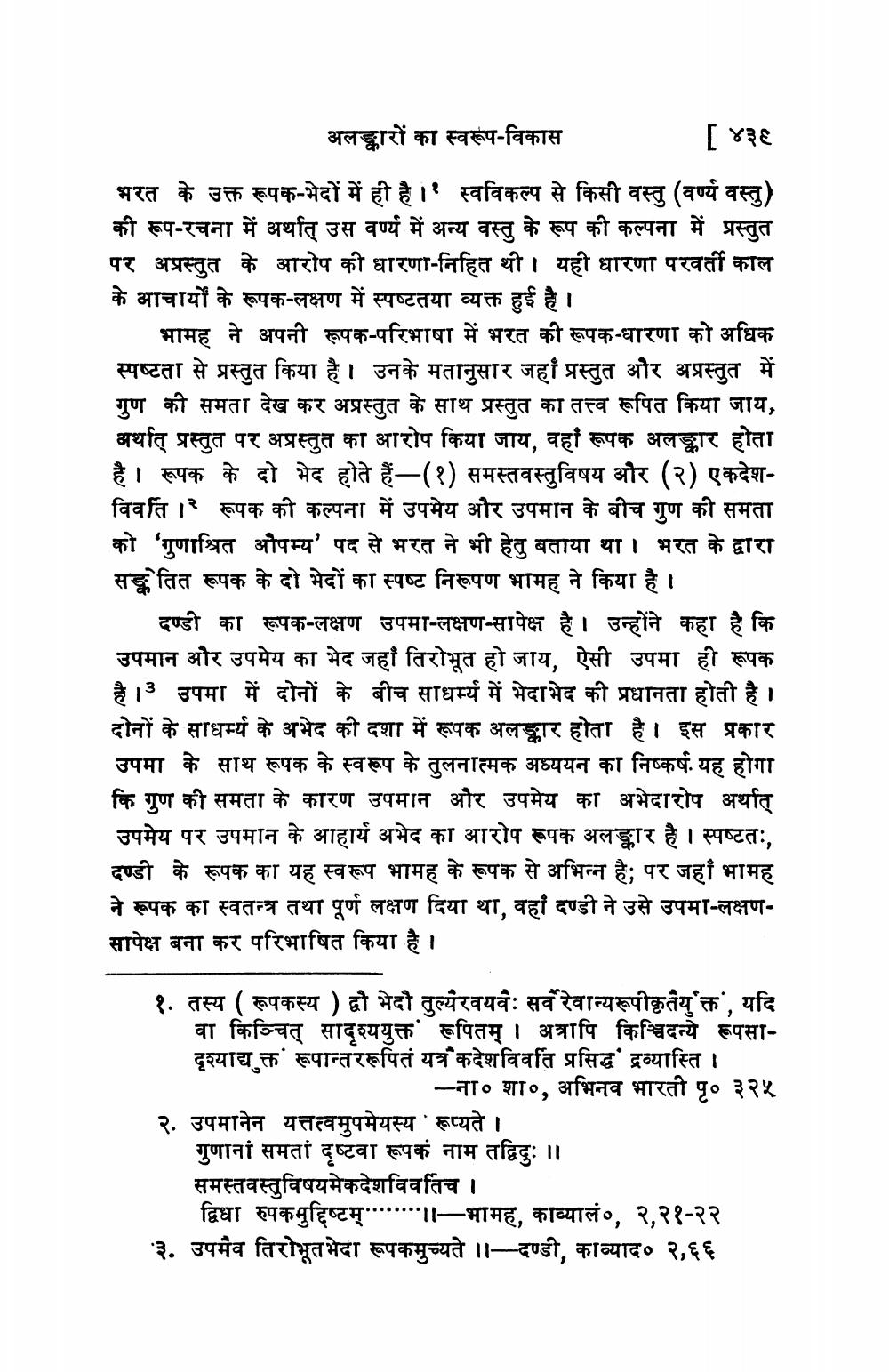________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ४३६ भरत के उक्त रूपक-भेदों में ही है। स्वविकल्प से किसी वस्तु (वर्ण्य वस्तु) की रूप-रचना में अर्थात् उस वर्ण्य में अन्य वस्तु के रूप की कल्पना में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के आरोप की धारणा-निहित थी। यही धारणा परवर्ती काल के आचार्यों के रूपक-लक्षण में स्पष्टतया व्यक्त हुई है।
भामह ने अपनी रूपक-परिभाषा में भरत की रूपक-धारणा को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया है। उनके मतानुसार जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में गुण की समता देख कर अप्रस्तुत के साथ प्रस्तुत का तत्त्व रूपित किया जाय, अर्थात् प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप किया जाय, वहाँ रूपक अलङ्कार होता है। रूपक के दो भेद होते हैं-(१) समस्तवस्तुविषय और (२) एकदेशविवति ।। रूपक की कल्पना में उपमेय और उपमान के बीच गुण की समता को 'गुणाश्रित औपम्य' पद से भरत ने भी हेतु बताया था। भरत के द्वारा सङ्कतित रूपक के दो भेदों का स्पष्ट निरूपण भामह ने किया है।
दण्डी का रूपक-लक्षण उपमा-लक्षण-सापेक्ष है। उन्होंने कहा है कि उपमान और उपमेय का भेद जहाँ तिरोभूत हो जाय, ऐसी उपमा ही रूपक है। उपमा में दोनों के बीच साधर्म्य में भेदाभेद की प्रधानता होती है। दोनों के साधर्म्य के अभेद की दशा में रूपक अलङ्कार होता है। इस प्रकार उपमा के साथ रूपक के स्वरूप के तुलनात्मक अध्ययन का निष्कर्ष यह होगा कि गुण की समता के कारण उपमान और उपमेय का अभेदारोप अर्थात् उपमेय पर उपमान के आहार्य अभेद का आरोप रूपक अलङ्कार है । स्पष्टतः, दण्डी के रूपक का यह स्वरूप भामह के रूपक से अभिन्न है; पर जहां भामह ने रूपक का स्वतन्त्र तथा पूर्ण लक्षण दिया था, वहाँ दण्डी ने उसे उपमा-लक्षणसापेक्ष बना कर परिभाषित किया है।
१. तस्य ( रूपकस्य ) द्वौ भेदौ तुल्यैरवयवैः सर्व रेवान्यरूपीकृतयुक्त, यदि
वा किञ्चित् सादृश्ययुक्त रूपितम् । अत्रापि किञ्चिदन्ये रूपसादृश्याद्य क्त रूपान्तररूपितं यत्र कदेश विवर्ति प्रसिद्ध द्रव्यास्ति ।
-ना० शा०, अभिनव भारती पृ० ३२५ २. उपमानेन यत्तत्वमुपमेयस्य रूप्यते।
गुणानां समतां दृष्टवा रूपकं नाम तद्विदुः । समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्तिच ।
द्विधा रुपकमुद्दिष्टम्..."||-भामह, काव्यालं०, २,२१-२२ ३. उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते ॥-दण्डी, काव्याद० २,६६