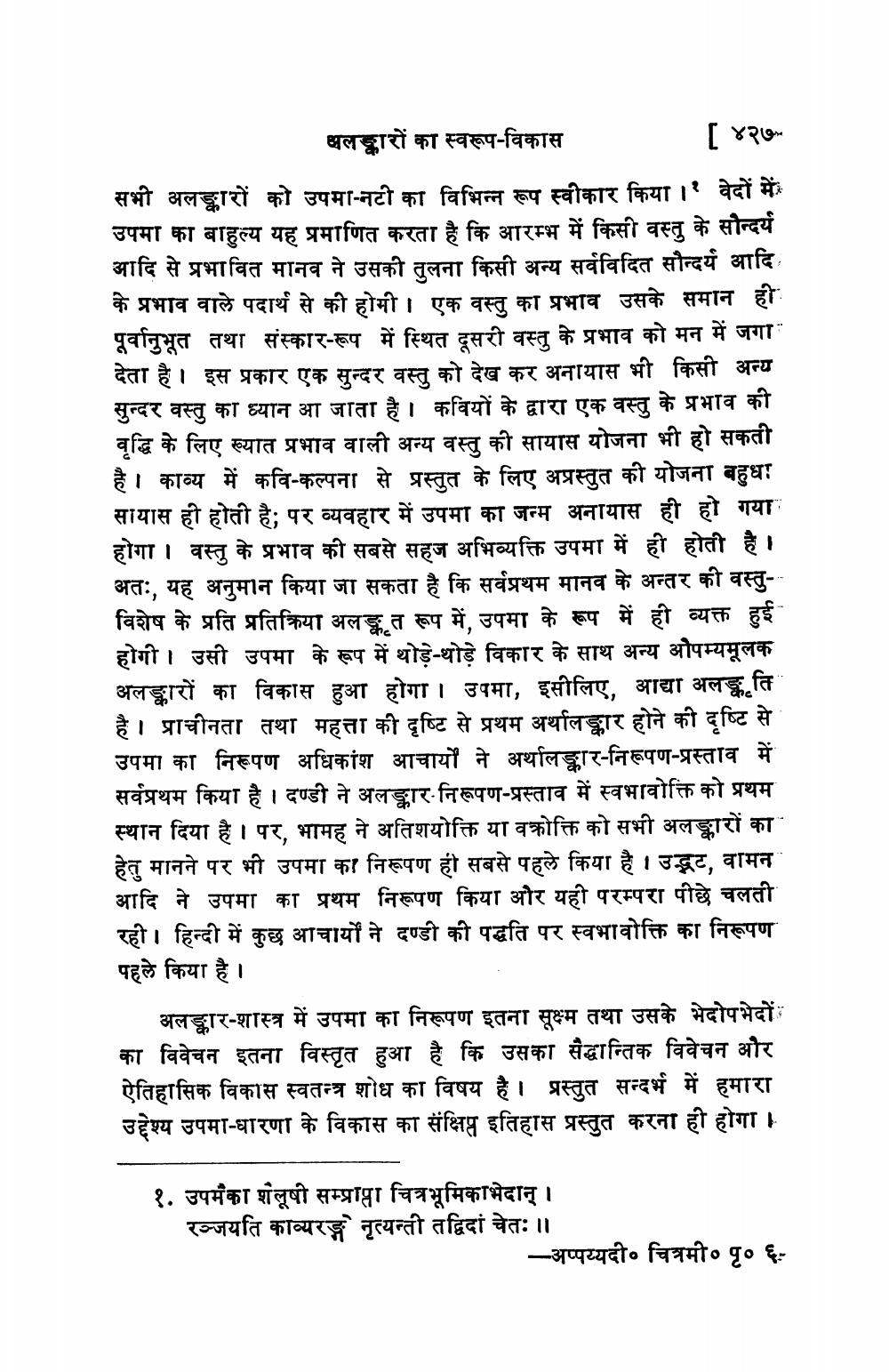________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ४२७ सभी अलङ्कारों को उपमा-नटी का विभिन्न रूप स्वीकार किया।' वेदों में उपमा का बाहुल्य यह प्रमाणित करता है कि आरम्भ में किसी वस्तु के सौन्दर्य आदि से प्रभावित मानव ने उसकी तुलना किसी अन्य सर्वविदित सौन्दर्य आदि के प्रभाव वाले पदार्थ से की होमी। एक वस्तु का प्रभाव उसके समान ही पूर्वानुभूत तथा संस्कार-रूप में स्थित दूसरी वस्तु के प्रभाव को मन में जगा देता है। इस प्रकार एक सुन्दर वस्तु को देख कर अनायास भी किसी अन्य सुन्दर वस्तु का ध्यान आ जाता है। कवियों के द्वारा एक वस्तु के प्रभाव की वृद्धि के लिए ख्यात प्रभाव वाली अन्य वस्तु की सायास योजना भी हो सकती है। काव्य में कवि-कल्पना से प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत की योजना बहुधा सायास ही होती है; पर व्यवहार में उपमा का जन्म अनायास ही हो गया होगा। वस्तु के प्रभाव की सबसे सहज अभिव्यक्ति उपमा में ही होती है। अतः, यह अनुमान किया जा सकता है कि सर्वप्रथम मानव के अन्तर की वस्तु-- विशेष के प्रति प्रतिक्रिया अलङ्कत रूप में, उपमा के रूप में ही व्यक्त हुई होगी। उसी उपमा के रूप में थोड़े-थोड़े विकार के साथ अन्य औपम्यमूलक अलङ्कारों का विकास हुआ होगा। उपमा, इसीलिए, आद्या अलङ्क ति है। प्राचीनता तथा महत्ता की दृष्टि से प्रथम अर्थालङ्कार होने की दृष्टि से उपमा का निरूपण अधिकांश आचार्यों ने अर्थालङ्कार-निरूपण-प्रस्ताव में सर्वप्रथम किया है । दण्डी ने अलङ्कार-निरूपण-प्रस्ताव में स्वभावोक्ति को प्रथम स्थान दिया है। पर, भामह ने अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति को सभी अलङ्कारों का हेतु मानने पर भी उपमा का निरूपण ही सबसे पहले किया है । उद्भट, वामन आदि ने उपमा का प्रथम निरूपण किया और यही परम्परा पीछे चलती रही। हिन्दी में कुछ आचार्यों ने दण्डी की पद्धति पर स्वभावोक्ति का निरूपण पहले किया है।
अलङ्कार-शास्त्र में उपमा का निरूपण इतना सूक्ष्म तथा उसके भेदोपभेदों का विवेचन इतना विस्तृत हुआ है कि उसका सैद्धान्तिक विवेचन और ऐतिहासिक विकास स्वतन्त्र शोध का विषय है। प्रस्तुत सन्दर्भ में हमारा उद्देश्य उपमा-धारणा के विकास का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना ही होगा।
१. उपमैका शैलूषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान् । रञ्जयति काव्यरङ्ग नृत्यन्ती तद्विदां चेतः॥
-अप्पय्यदी. चित्रमी० पृ० ६.