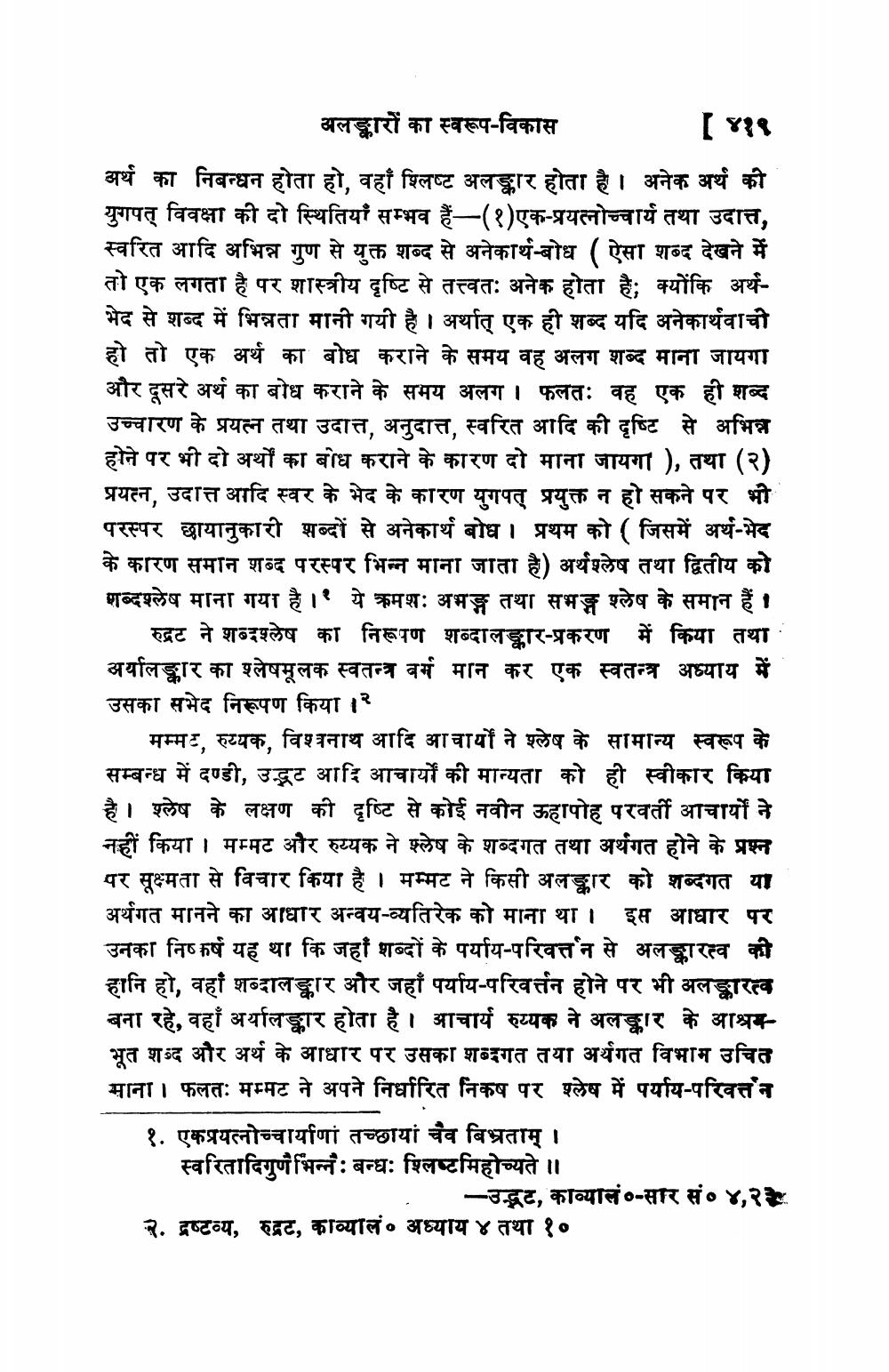________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[४१९ अर्थ का निबन्धन होता हो, वहाँ श्लिष्ट अलङ्कार होता है। अनेक अर्थ की युगपत् विवक्षा की दो स्थितियां सम्भव हैं-(१)एक-प्रयत्नोच्चार्य तथा उदात्त, स्वरित आदि अभिन्न गुण से युक्त शब्द से अनेकार्थ-बोध ( ऐसा शब्द देखने में तो एक लगता है पर शास्त्रीय दृष्टि से तत्त्वतः अनेक होता है; क्योंकि अर्थभेद से शब्द में भिन्नता मानी गयी है । अर्थात् एक ही शब्द यदि अनेकार्थवाची हो तो एक अर्थ का बोध कराने के समय वह अलग शब्द माना जायगा
और दूसरे अर्थ का बोध कराने के समय अलग । फलतः वह एक ही शब्द उच्चारण के प्रयत्न तथा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि की दृष्टि से अभिन्न होने पर भी दो अर्थों का बोध कराने के कारण दो माना जायगा ), तथा (२) प्रयत्न, उदात्त आदि स्वर के भेद के कारण युगपत् प्रयुक्त न हो सकने पर भी परस्पर छायानुकारी शब्दों से अनेकार्थ बोध । प्रथम को ( जिसमें अर्थ-भेद के कारण समान शब्द परस्पर भिन्न माना जाता है) अर्थश्लेष तथा द्वितीय को शब्दश्लेष माना गया है। ये क्रमशः अभङ्ग तथा सभङ्ग श्लेष के समान हैं।
रुद्रट ने शब्दश्लेष का निरूपण शब्दालङ्कार-प्रकरण में किया तथा अर्यालङ्कार का श्लेषमूलक स्वतन्त्र वर्म मान कर एक स्वतन्त्र अध्याय में उसका सभेद निरूपण किया। ___ मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने श्लेष के सामान्य स्वरूप के सम्बन्ध में दण्डी, उद्भट आदि आचार्यों की मान्यता को ही स्वीकार किया है। श्लेष के लक्षण की दृष्टि से कोई नवीन ऊहापोह परवर्ती आचार्यों ने नहीं किया। मम्मट और रुय्यक ने श्लेष के शब्दगत तथा अर्थगत होने के प्रश्न पर सूक्ष्मता से विचार किया है । मम्मट ने किसी अलङ्कार को शब्दगत या अर्थगत मानने का आधार अन्वय-व्यतिरेक को माना था। इस आधार पर उनका निष्कर्ष यह था कि जहां शब्दों के पर्याय-परिवर्तन से अलङ्कारत्व की हानि हो, वहां शब्दालङ्कार और जहाँ पर्याय-परिवर्तन होने पर भी अलङ्कारत्व बना रहे, वहाँ अर्यालङ्कार होता है। आचार्य रुय्यक ने अलङ्कार के आश्रमभूत शब्द और अर्थ के आधार पर उसका शब्दगत तया अर्थगत विभाम उचित माना। फलतः मम्मट ने अपने निर्धारित निकष पर श्लेष में पर्याय-परिवर्तन १. एकप्रयत्नोच्चार्याणां तच्छायां चैव बिभ्रताम् । स्वरितादिगुणैभिन्नः बन्धः श्लिष्टमिहोच्यते ॥
. -उद्भट, काव्यालं०-सार सं०४,२ २. द्रष्टव्य, रुद्रट, काव्यालं. अध्याय ४ तथा १०