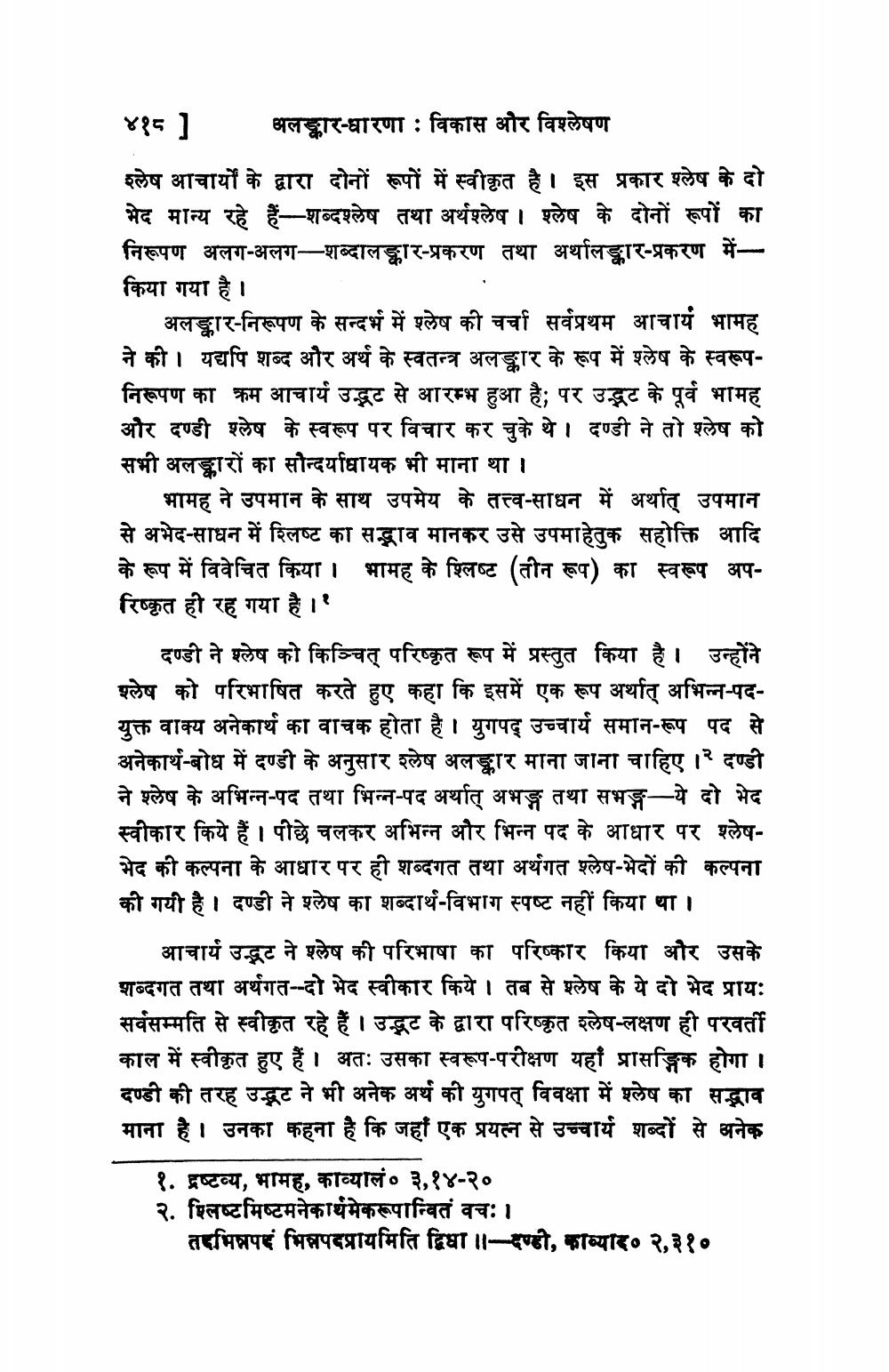________________
४१८ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
श्लेष आचार्यों के द्वारा दोनों रूपों में स्वीकृत है। इस प्रकार श्लेष के दो भेद मान्य रहे हैं-शब्दश्लेष तथा अर्थश्लेष । श्लेष के दोनों रूपों का निरूपण अलग-अलग–शब्दालङ्कार-प्रकरण तथा अर्थालङ्कार-प्रकरण मेंकिया गया है। ___ अलङ्कार-निरूपण के सन्दर्भ में श्लेष की चर्चा सर्वप्रथम आचार्य भामह ने की। यद्यपि शब्द और अर्थ के स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में श्लेष के स्वरूपनिरूपण का क्रम आचार्य उद्भट से आरम्भ हुआ है; पर उद्भट के पूर्व भामह
और दण्डी श्लेष के स्वरूप पर विचार कर चुके थे। दण्डी ने तो श्लेष को सभी अलङ्कारों का सौन्दर्याधायक भी माना था।
भामह ने उपमान के साथ उपमेय के तत्त्व-साधन में अर्थात् उपमान से अभेद-साधन में श्लिष्ट का सद्भाव मानकर उसे उपमाहेतुक सहोक्ति आदि के रूप में विवेचित किया। भामह के श्लिष्ट (तीन रूप) का स्वरूप अपरिष्कृत ही रह गया है।' ___ दण्डी ने श्लेष को किञ्चित् परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने श्लेष को परिभाषित करते हुए कहा कि इसमें एक रूप अर्थात् अभिन्न-पदयुक्त वाक्य अनेकार्थ का वाचक होता है। युगपद् उच्चार्य समान-रूप पद से अनेकार्थ-बोध में दण्डी के अनुसार श्लेष अलङ्कार माना जाना चाहिए। दण्डी ने श्लेष के अभिन्न-पद तथा भिन्न-पद अर्थात् अभङ्ग तथा सभङ्ग-ये दो भेद स्वीकार किये हैं। पीछे चलकर अभिन्न और भिन्न पद के आधार पर श्लेषभेद की कल्पना के आधार पर ही शब्दगत तथा अर्थगत श्लेष-भेदों की कल्पना की गयी है। दण्डी ने श्लेष का शब्दार्थ-विभाग स्पष्ट नहीं किया था।
आचार्य उद्भट ने श्लेष की परिभाषा का परिष्कार किया और उसके शब्दगत तथा अर्थगत-दो भेद स्वीकार किये। तब से श्लेष के ये दो भेद प्रायः सर्वसम्मति से स्वीकृत रहे हैं । उद्भट के द्वारा परिष्कृत श्लेष-लक्षण ही परवर्ती काल में स्वीकृत हुए हैं। अतः उसका स्वरूप-परीक्षण यहाँ प्रासङ्गिक होगा। दण्डी की तरह उद्भट ने भी अनेक अर्थ की युगपत् विवक्षा में श्लेष का सद्भाव माना है। उनका कहना है कि जहां एक प्रयत्न से उच्चार्य शब्दों से अनेक
१. द्रष्टव्य, भामह, काव्यालं० ३,१४-२० २. श्लिष्टमिष्टमनेकार्थमेकरूपान्वितं वचः।
तभिन्नपदं भिन्नपदप्रायमिति द्विधा ।।-दण्डी, काम्यार० २,३१०