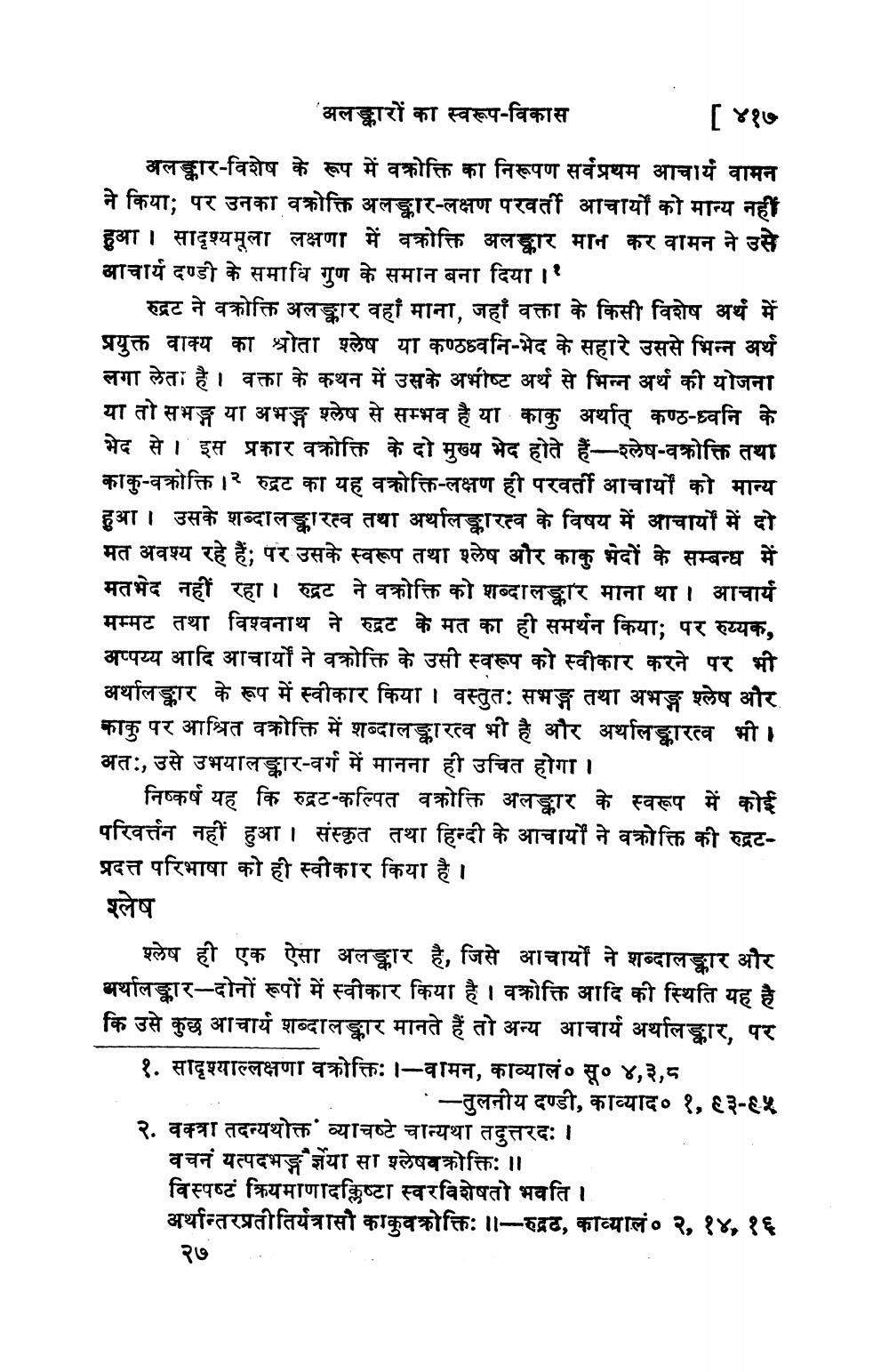________________
'अलङ्कारों का स्वरूप - विकास
[ ४१७
अलङ्कार - विशेष के रूप में वक्रोक्ति का निरूपण सर्वप्रथम आचार्य वामन ने किया; पर उनका वक्रोक्ति अलङ्कार - लक्षण परवर्ती आचार्यों को मान्य नहीं हुआ । सादृश्यमूला लक्षणा में वक्रोक्ति अलङ्कार मान कर वामन ने उसे आचार्य दण्डी के समाधि गुण के समान बना दिया । "
रुद्रट ने वक्रोक्ति अलङ्कार वहाँ माना, जहाँ वक्ता के किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त वाक्य का श्रोता श्लेष या कण्ठध्वनि-भेद के सहारे उससे भिन्न अर्थ लगा लेता है । वक्ता के कथन में उसके अभीष्ट अर्थ से भिन्न अर्थ की योजना या तो सभङ्ग या अभङ्ग श्लेष से सम्भव है या काकु अर्थात् कण्ठ-ध्वनि के भेद से । इस प्रकार वक्रोक्ति के दो मुख्य भेद होते हैं - श्लेष - वक्रोक्ति तथा काकु - वक्रोक्ति । २ रुद्रट का यह वक्रोक्ति-लक्षण ही परवर्ती आचार्यों को मान्य हुआ । उसके शब्दालङ्कारत्व तथा अर्थालङ्कारत्व के विषय में आचार्यों में दो मत अवश्य रहे हैं; पर उसके स्वरूप तथा श्लेष और काकु भेदों के सम्बन्ध में मतभेद नहीं रहा । रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार माना था । आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ ने रुद्रट के मत का ही समर्थन किया; पर रुय्यक, अप्पय्य आदि आचार्यों ने वक्रोक्ति के उसी स्वरूप को स्वीकार करने पर भी अर्थालङ्कार के रूप में स्वीकार किया । वस्तुत: सभङ्ग तथा अभङ्ग श्लेष और काकु पर आश्रित वक्रोक्ति में शब्दालङ्कारत्व भी है और अर्थालङ्कारत्व भी । अत:, उसे उभयालङ्कार वर्ग में मानना ही उचित होगा ।
निष्कर्ष यह कि रुद्रट - कल्पित वक्रोक्ति अलङ्कार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । संस्कृत तथा हिन्दी के आचार्यों ने वक्रोक्ति की रुद्रटप्रदत्त परिभाषा को ही स्वीकार किया है ।
श्लेष
श्लेष ही एक ऐसा अलङ्कार है, जिसे आचार्यों ने शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार - दोनों रूपों में स्वीकार किया है । वक्रोक्ति आदि की स्थिति यह है कि उसे कुछ आचार्य शब्दालङ्कार मानते हैं तो अन्य आचार्य अर्थालङ्कार, पर
१. सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः । - वामन, काव्यालं ० सू० ४,३,८ - तुलनीय दण्डी, काव्याद० १, ६३-६५
२. वक्त्रा तदन्यथोक्त व्याचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः ।
वचनं यत्पदभङ्ग ज्ञेया सा श्लेषवक्रोक्तिः ॥ विस्पष्टं क्रियमाणादक्लिष्टा स्वरविशेषतो भवति ।
अर्थान्तरप्रतीतिर्यत्रासौ काकुवक्रोक्तिः ॥ रुद्रट, काव्यालं ० २, १४, १६
२७