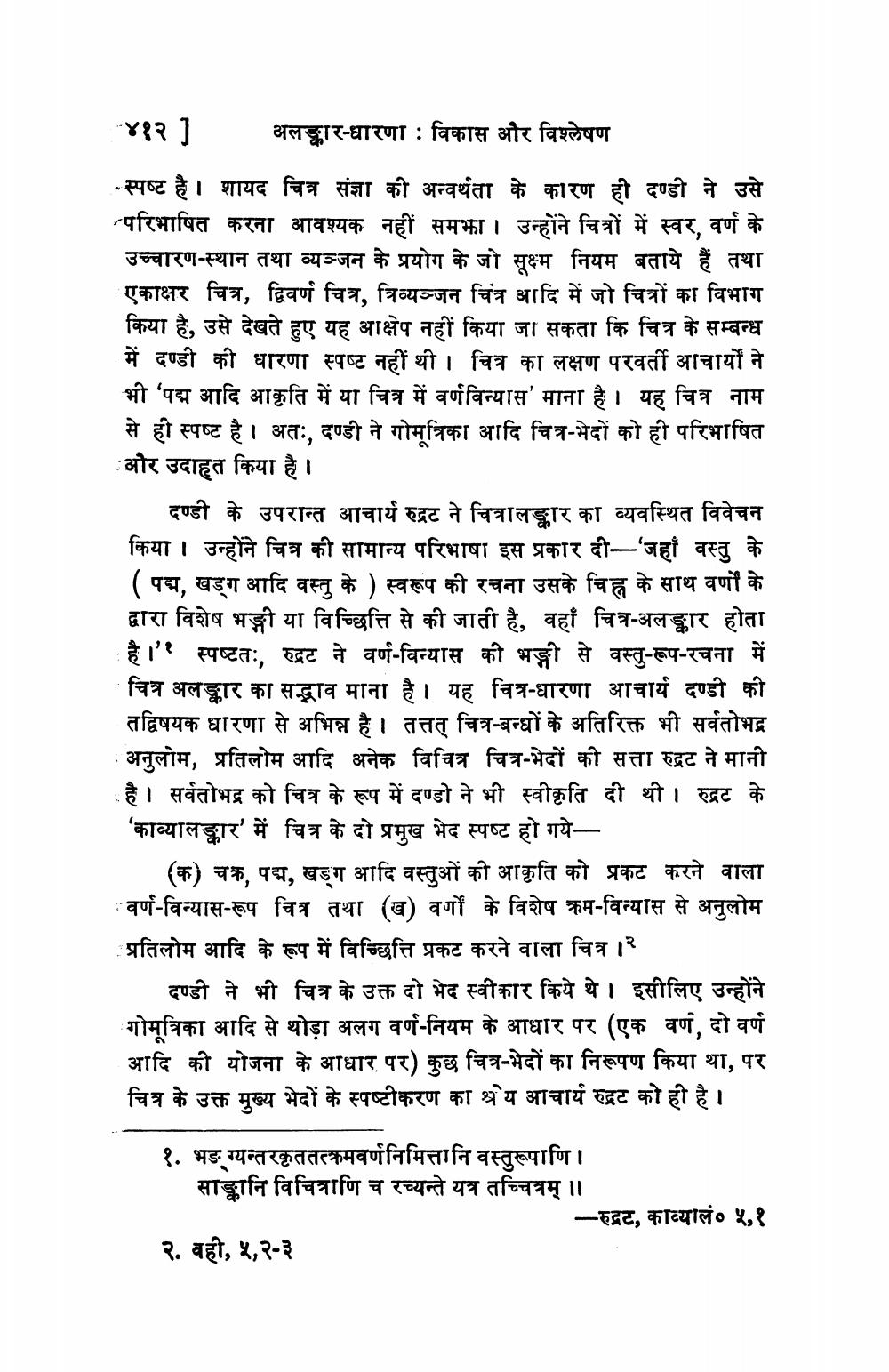________________
“४१२]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
• स्पष्ट है। शायद चित्र संज्ञा की अन्वर्थता के कारण ही दण्डी ने उसे “परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने चित्रों में स्वर, वर्ण के उच्चारण-स्थान तथा व्यञ्जन के प्रयोग के जो सूक्ष्म नियम बताये हैं तथा एकाक्षर चित्र, द्विवर्ण चित्र, त्रिव्यञ्जन चित्र आदि में जो चित्रों का विभाग किया है, उसे देखते हुए यह आक्षेप नहीं किया जा सकता कि चित्र के सम्बन्ध में दण्डी की धारणा स्पष्ट नहीं थी। चित्र का लक्षण परवर्ती आचार्यों ने भी 'पद्म आदि आकृति में या चित्र में वर्णविन्यास' माना है। यह चित्र नाम से ही स्पष्ट है। अतः, दण्डी ने गोमूत्रिका आदि चित्र-भेदों को ही परिभाषित और उदाहृत किया है।
दण्डी के उपरान्त आचार्य रुद्रट ने चित्रालङ्कार का व्यवस्थित विवेचन किया। उन्होंने चित्र की सामान्य परिभाषा इस प्रकार दी-'जहाँ वस्तु के ( पद्म, खड्ग आदि वस्तु के ) स्वरूप की रचना उसके चिह्न के साथ वर्णों के द्वारा विशेष भङ्गी या विच्छित्ति से की जाती है, वहाँ चित्र-अलङ्कार होता है।'' स्पष्टतः, रुद्रट ने वर्ण-विन्यास की भङ्गी से वस्तु-रूप-रचना में चित्र अलङ्कार का सद्भाव माना है। यह चित्र-धारणा आचार्य दण्डी की तद्विषयक धारणा से अभिन्न है। तत्तत् चित्र-बन्धों के अतिरिक्त भी सर्वतोभद्र . अनुलोम, प्रतिलोम आदि अनेक विचित्र चित्र-भेदों की सत्ता रुद्रट ने मानी है। सर्वतोभद्र को चित्र के रूप में दण्डो ने भी स्वीकृति दी थी। रुद्रट के 'काव्यालङ्कार' में चित्र के दो प्रमुख भेद स्पष्ट हो गये
(क) चक्र, पद्म, खड्ग आदि वस्तुओं की आकृति को प्रकट करने वाला वर्ण-विन्यास-रूप चित्र तथा (ख) वर्गों के विशेष क्रम-विन्यास से अनुलोम प्रतिलोम आदि के रूप में विच्छित्ति प्रकट करने वाला चित्र ।
दण्डी ने भी चित्र के उक्त दो भेद स्वीकार किये थे। इसीलिए उन्होंने गोमूत्रिका आदि से थोड़ा अलग वर्ण-नियम के आधार पर (एक वर्ण, दो वर्ण आदि की योजना के आधार पर) कुछ चित्र-भेदों का निरूपण किया था, पर चित्र के उक्त मुख्य भेदों के स्पष्टीकरण का श्रेय आचार्य रुद्रट को ही है।
१. भङ ग्यन्तरकृततत्क्रमवर्णनिमित्तानि वस्तुरूपाणि। साकानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम् ।।
-रुद्रट, काव्यालं० ५,१ २. वही, ५,२-३