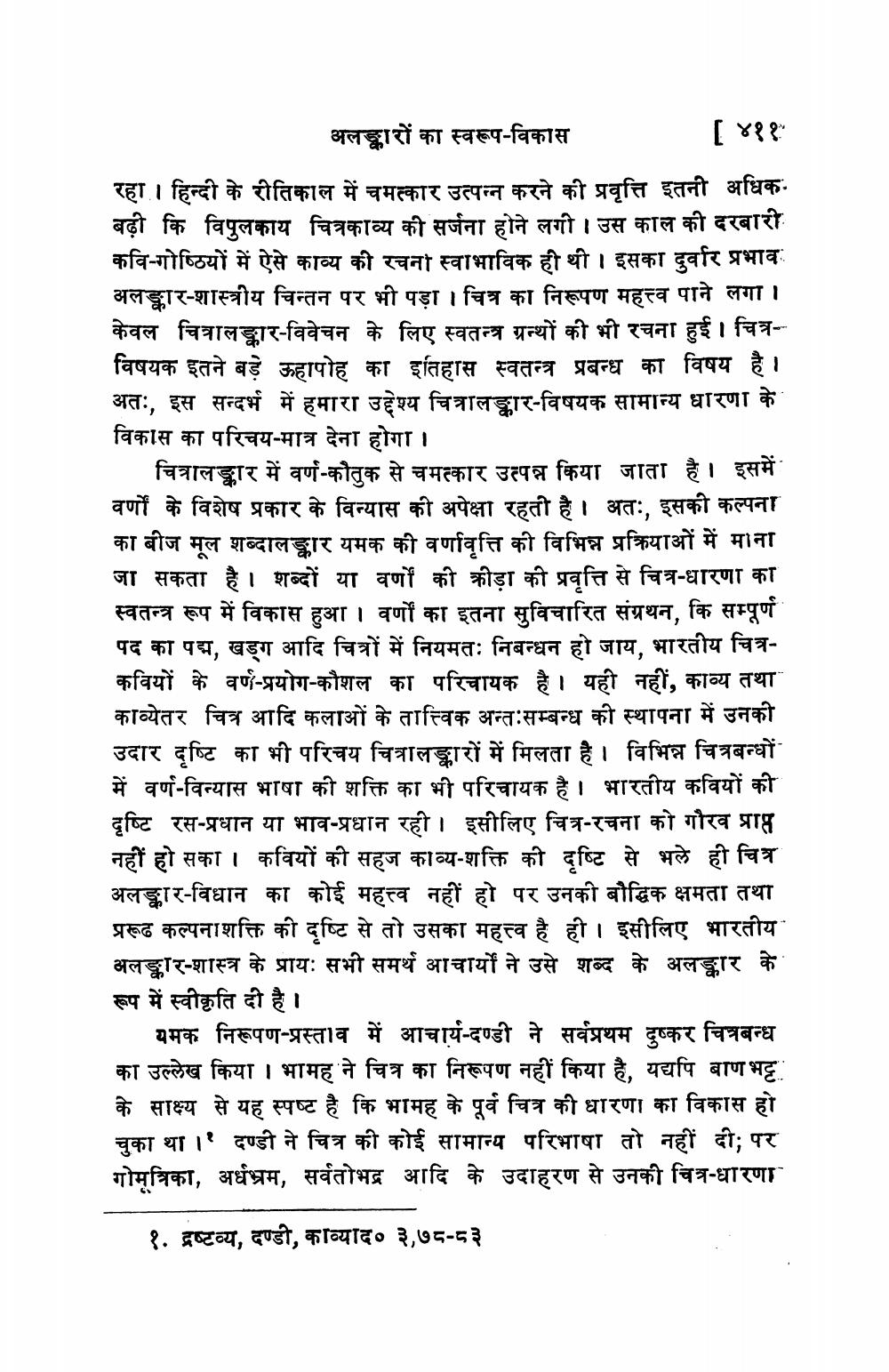________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास [४११ रहा । हिन्दी के रीतिकाल में चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक. बढ़ी कि विपुलकाय चित्रकाव्य की सर्जना होने लगी। उस काल की दरबारी कवि-गोष्ठियों में ऐसे काव्य की रचना स्वाभाविक ही थी। इसका दुर्वार प्रभाव अलङ्कार-शास्त्रीय चिन्तन पर भी पड़ा । चित्र का निरूपण महत्त्व पाने लगा। केवल चित्रालङ्कार-विवेचन के लिए स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी रचना हुई। चित्रविषयक इतने बड़े ऊहापोह का इतिहास स्वतन्त्र प्रबन्ध का विषय है। अतः, इस सन्दर्भ में हमारा उद्देश्य चित्रालङ्कार-विषयक सामान्य धारणा के विकास का परिचय-मात्र देना होगा।
चित्रालङ्कार में वर्ण-कौतुक से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इसमें वर्गों के विशेष प्रकार के विन्यास की अपेक्षा रहती है। अतः, इसकी कल्पना का बीज मूल शब्दालङ्कार यमक की वर्णावृत्ति की विभिन्न प्रक्रियाओं में माना जा सकता है। शब्दों या वर्णों की क्रीड़ा की प्रवृत्ति से चित्र-धारणा का स्वतन्त्र रूप में विकास हुआ। वर्षों का इतना सुविचारित संग्रथन, कि सम्पूर्ण पद का पद्म, खड्ग आदि चित्रों में नियमतः निबन्धन हो जाय, भारतीय चित्रकवियों के वर्ण-प्रयोग-कौशल का परिचायक है। यही नहीं, काव्य तथा काव्येतर चित्र आदि कलाओं के तात्त्विक अन्तःसम्बन्ध की स्थापना में उनकी उदार दृष्टि का भी परिचय चित्रालङ्कारों में मिलता है। विभिन्न चित्रबन्धों में वर्ण-विन्यास भाषा की शक्ति का भी परिचायक है। भारतीय कवियों की दृष्टि रस-प्रधान या भाव-प्रधान रही। इसीलिए चित्र-रचना को गौरव प्राप्त नहीं हो सका । कवियों की सहज काव्य-शक्ति की दृष्टि से भले ही चित्र अलङ्कार-विधान का कोई महत्त्व नहीं हो पर उनकी बौद्धिक क्षमता तथा प्ररूढ कल्पनाशक्ति की दृष्टि से तो उसका महत्त्व है ही। इसीलिए भारतीय अलङ्कार-शास्त्र के प्रायः सभी समर्थ आचार्यों ने उसे शब्द के अलङ्कार के रूप में स्वीकृति दी है।
यमक निरूपण-प्रस्ताव में आचार्य-दण्डी ने सर्वप्रथम दुष्कर चित्रबन्ध का उल्लेख किया । भामह ने चित्र का निरूपण नहीं किया है, यद्यपि बाण भट्ट के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि भामह के पूर्व चित्र की धारणा का विकास हो चुका था ।' दण्डी ने चित्र की कोई सामान्य परिभाषा तो नहीं दी; पर गोमत्रिका, अर्धभ्रम, सर्वतोभद्र आदि के उदाहरण से उनकी चित्र-धारणा
१. द्रष्टव्य, दण्डी, काव्याद० ३,७८-८३