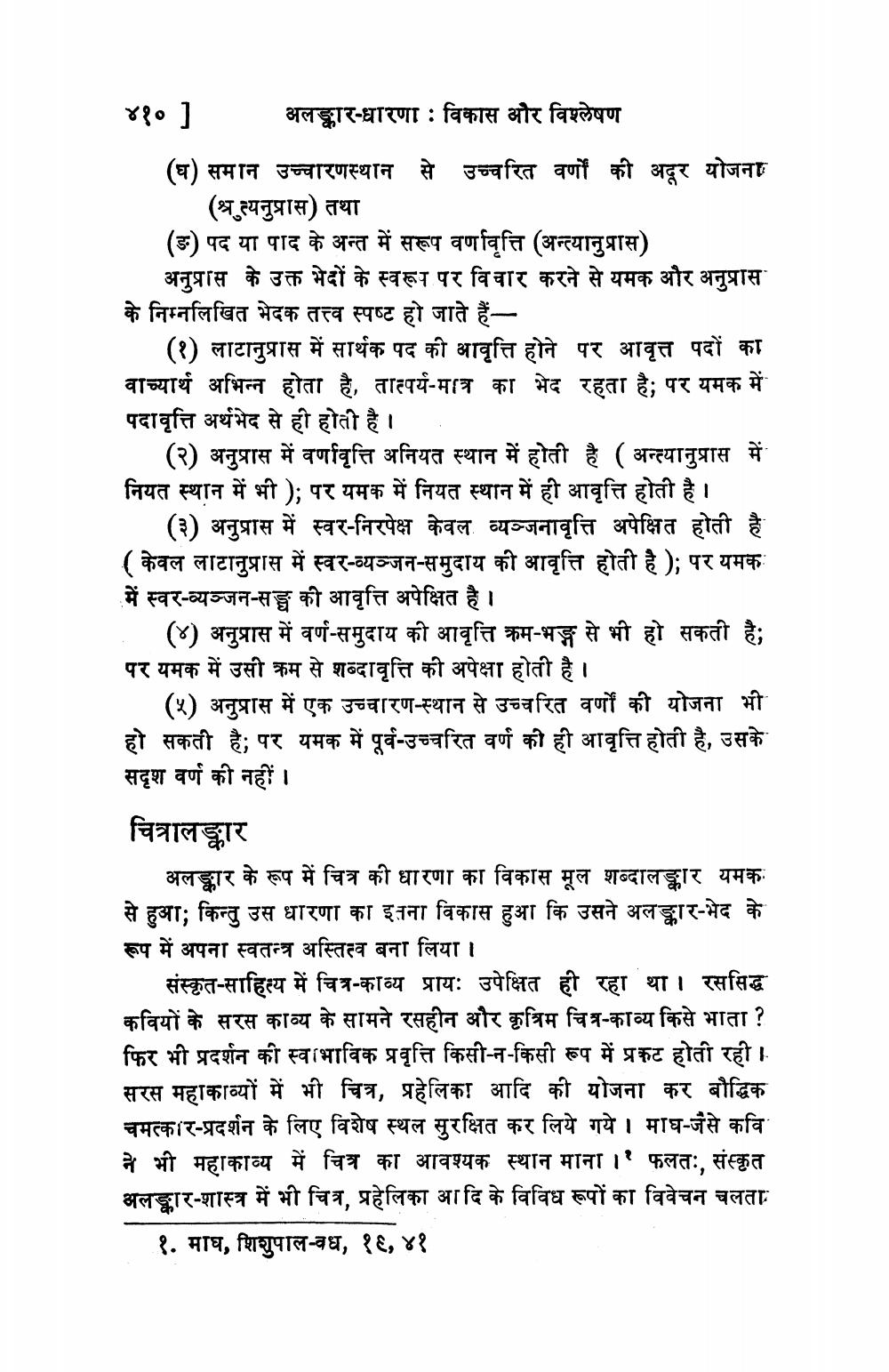________________
४१० ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण (घ) समान उच्चारणस्थान से उच्चरित वर्णों की अदूर योजना
(श्र त्यनुप्रास) तथा (ङ) पद या पाद के अन्त में सरूप वर्णावृत्ति (अन्त्यानुप्रास)
अनुप्रास के उक्त भेदों के स्वरूप पर विचार करने से यमक और अनुप्रास के निम्नलिखित भेदक तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं
(१) लाटानुप्रास में सार्थक पद की आवृत्ति होने पर आवृत्त पदों का वाच्यार्थ अभिन्न होता है, तात्पर्य-मात्र का भेद रहता है; पर यमक में पदावृत्ति अर्थभेद से ही होती है।
(२) अनुप्रास में वर्णावृत्ति अनियत स्थान में होती है ( अन्त्यानुप्रास में नियत स्थान में भी ); पर यमक में नियत स्थान में ही आवृत्ति होती है।
(३) अनुप्रास में स्वर-निरपेक्ष केवल व्यञ्जनावृत्ति अपेक्षित होती है ( केवल लाटानुप्रास में स्वर-व्यञ्जन-समुदाय की आवृत्ति होती है ); पर यमक में स्वर-व्यञ्जन-सङ्घ की आवृत्ति अपेक्षित है।
(४) अनुप्रास में वर्ण-समुदाय की आवृत्ति क्रम-भङ्ग से भी हो सकती है; पर यमक में उसी क्रम से शब्दावृत्ति की अपेक्षा होती है।
(५) अनुप्रास में एक उच्चारण-स्थान से उच्चरित वर्णों की योजना भी हो सकती है; पर यमक में पूर्व-उच्चरित वर्ण की ही आवृत्ति होती है, उसके सदृश वर्ण की नहीं। चित्रालङ्कार
अलङ्कार के रूप में चित्र की धारणा का विकास मूल शब्दालङ्कार यमक से हुआ; किन्तु उस धारणा का इतना विकास हुआ कि उसने अलङ्कार-भेद के रूप में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बना लिया। ____ संस्कृत-साहित्य में चित्र-काव्य प्रायः उपेक्षित ही रहा था। रससिद्ध कवियों के सरस काव्य के सामने रसहीन और कृत्रिम चित्र-काव्य किसे भाता? फिर भी प्रदर्शन की स्वाभाविक प्रवृत्ति किसी-न-किसी रूप में प्रकट होती रही। सरस महाकाव्यों में भी चित्र, प्रहेलिका आदि की योजना कर बौद्धिक चमत्कार-प्रदर्शन के लिए विशेष स्थल सुरक्षित कर लिये गये । माघ-जैसे कवि ने भी महाकाव्य में चित्र का आवश्यक स्थान माना। फलतः, संस्कृत अलङ्कार-शास्त्र में भी चित्र, प्रहेलिका आदि के विविध रूपों का विवेचन चलता
१. माघ, शिशुपाल-वध, १६, ४१