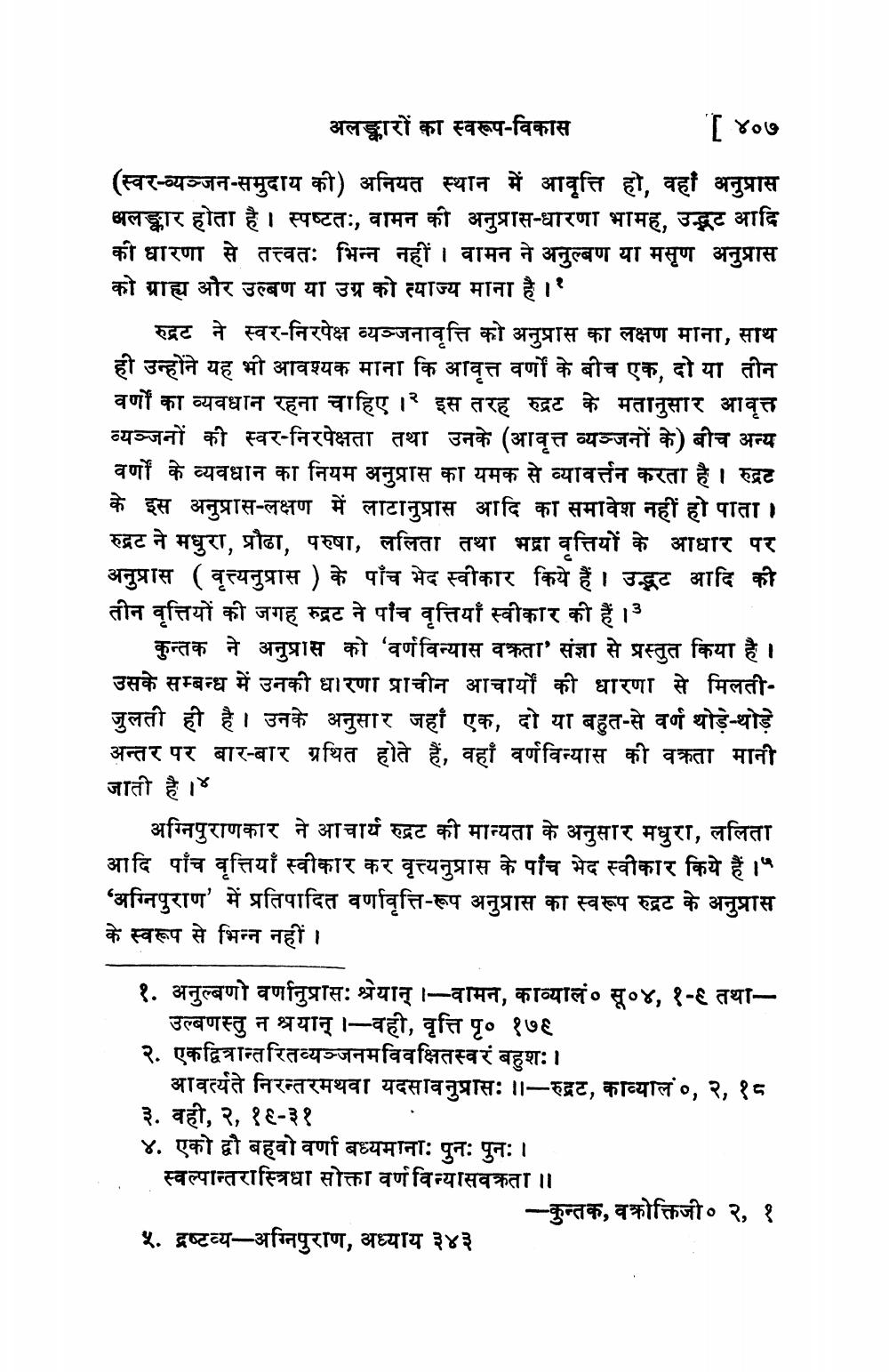________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास [ ४०७ (स्वर-व्यञ्जन-समुदाय की) अनियत स्थान में आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलङ्कार होता है। स्पष्टतः, वामन की अनुप्रास-धारणा भामह, उद्भट आदि की धारणा से तत्त्वतः भिन्न नहीं । वामन ने अनुल्बण या मसृण अनुप्रास को ग्राह्य और उल्बण या उग्र को त्याज्य माना है।'
रुद्रट ने स्वर-निरपेक्ष व्यञ्जनावृत्ति को अनुप्रास का लक्षण माना, साथ ही उन्होंने यह भी आवश्यक माना कि आवृत्त वर्गों के बीच एक, दो या तीन वर्णों का व्यवधान रहना चाहिए। इस तरह रुद्रट के मतानुसार आवृत्त व्यञ्जनों की स्वर-निरपेक्षता तथा उनके (आवृत्त व्यञ्जनों के) बीच अन्य वर्गों के व्यवधान का नियम अनुप्रास का यमक से व्यावर्तन करता है। रुद्रट के इस अनुप्रास-लक्षण में लाटानुप्रास आदि का समावेश नहीं हो पाता। रुद्रट ने मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता तथा भद्रा वृत्तियों के आधार पर अनुप्रास ( वृत्त्यनुप्रास ) के पाँच भेद स्वीकार किये हैं। उद्भट आदि की तीन वृत्तियों की जगह रुद्रट ने पांच वृत्तियाँ स्वीकार की हैं।।
कुन्तक ने अनुप्रास को 'वर्णविन्यास वक्रता' संज्ञा से प्रस्तुत किया है। उसके सम्बन्ध में उनकी धारणा प्राचीन आचार्यों की धारणा से मिलतीजुलती ही है। उनके अनुसार जहाँ एक, दो या बहुत-से वर्ण थोड़े-थोड़े अन्तर पर बार-बार ग्रथित होते हैं, वहाँ वर्णविन्यास की वक्रता मानी जाती है।४ ___ अग्निपुराणकार ने आचार्य रुद्रट की मान्यता के अनुसार मधुरा, ललिता आदि पाँच वृत्तियाँ स्वीकार कर वृत्त्यनुप्रास के पांच भेद स्वीकार किये हैं।" 'अग्निपुराण' में प्रतिपादित वर्णावृत्ति-रूप अनुप्रास का स्वरूप रुद्रट के अनुप्रास के स्वरूप से भिन्न नहीं।
१. अनुल्बणो वर्णानुप्रासः श्रेयान् । -वामन, काव्यालं० सू०४, १-६ तथा
उल्बणस्तु न श्रयान् ।-वही, वृत्ति पृ० १७६ २. एकद्वित्रान्तरितव्यञ्जनमविवक्षितस्वरं बहुशः।
आवय॑ते निरन्तरमथवा यदसावनुप्रासः ।।-रुद्रट, काव्याल०, २, १८ ३. वही, २, १६-३१ ४. एको द्वौ बहवो वर्णा बध्यमानाः पुनः पुनः । __ स्वल्पान्तरास्त्रिधा सोक्ता वर्ण विन्यासवक्रता ॥
-कुन्तक, वक्रोक्तिजी० २, १ ५. द्रष्टव्य-अग्निपुराण, अध्याय ३४३