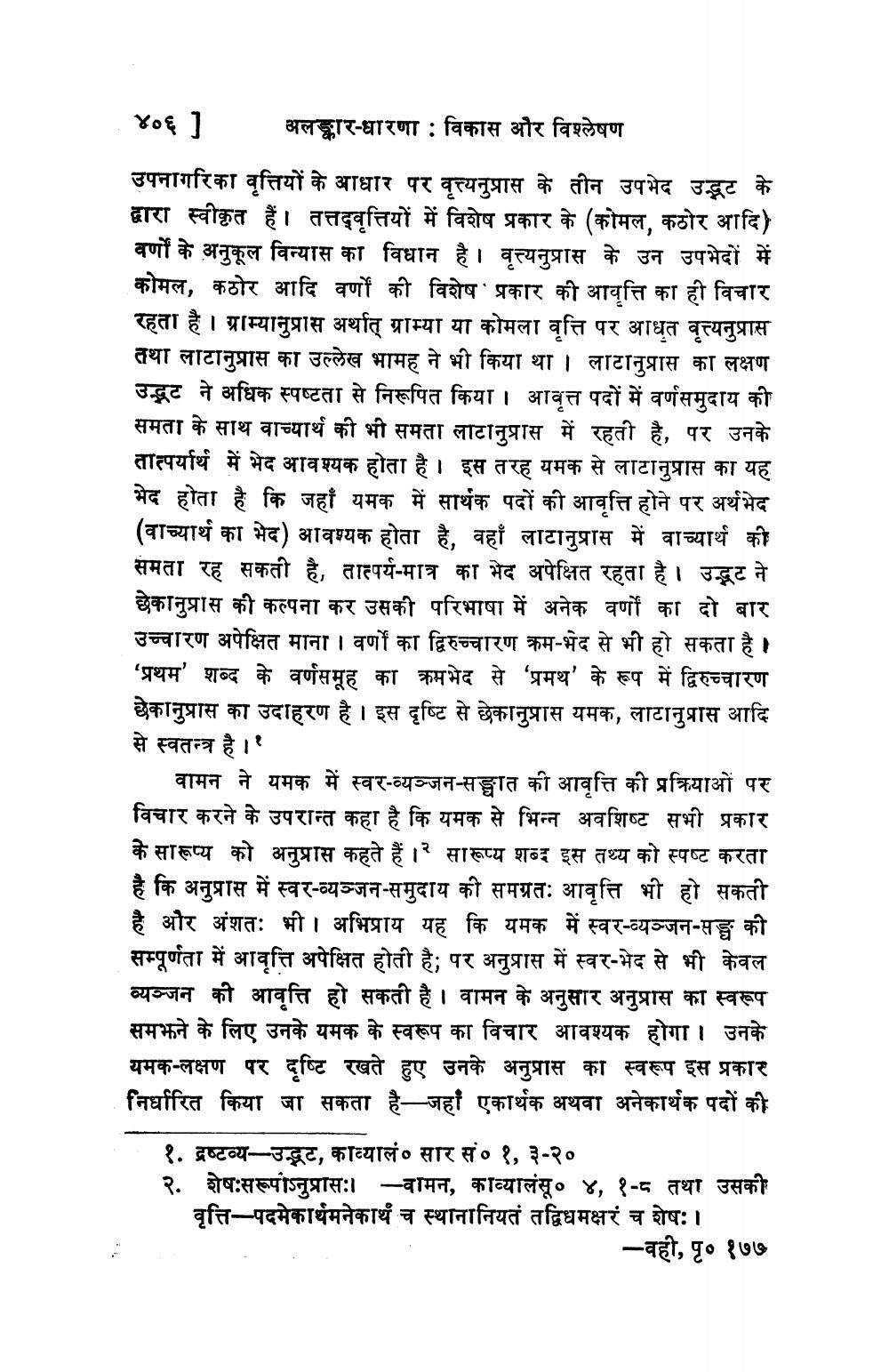________________
४०६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण उपनागरिका वृत्तियों के आधार पर वृत्त्यनुप्रास के तीन उपभेद उद्भट के द्वारा स्वीकृत हैं। तत्तवृत्तियों में विशेष प्रकार के (कोमल, कठोर आदि) वर्णों के अनुकूल विन्यास का विधान है। वृत्त्यनुप्रास के उन उपभेदों में कोमल, कठोर आदि वर्गों की विशेष प्रकार की आवृत्ति का ही विचार रहता है । ग्राम्यानुप्रास अर्थात् ग्राम्या या कोमला वृत्ति पर आधुत वृत्त्यनुप्रास तथा लाटानुप्रास का उल्लेख भामह ने भी किया था। लाटानुप्रास का लक्षण उद्भट ने अधिक स्पष्टता से निरूपित किया। आवृत्त पदों में वर्णसमुदाय की समता के साथ वाच्यार्थ की भी समता लाटानुप्रास में रहती है, पर उनके तात्पर्यार्थ में भेद आवश्यक होता है। इस तरह यमक से लाटानुप्रास का यह भेद होता है कि जहाँ यमक में सार्थक पदों की आवृत्ति होने पर अर्थभेद (वाच्यार्थ का भेद) आवश्यक होता है, वहाँ लाटानुप्रास में वाच्यार्थ की समता रह सकती है, तात्पर्य-मात्र का भेद अपेक्षित रहता है। उद्भट ने छेकानुप्रास की कल्पना कर उसकी परिभाषा में अनेक वर्णों का दो बार उच्चारण अपेक्षित माना । वर्गों का द्विरुच्चारण क्रम-भेद से भी हो सकता है। 'प्रथम' शब्द के वर्णसमूह का क्रमभेद से 'प्रमथ' के रूप में द्विरुच्चारण छेकानुप्रास का उदाहरण है । इस दृष्टि से छेकानुप्रास यमक, लाटानुप्रास आदि से स्वतन्त्र है।' __ वामन ने यमक में स्वर-व्यञ्जन-सङ्घात की आवृत्ति की प्रक्रियाओं पर विचार करने के उपरान्त कहा है कि यमक से भिन्न अवशिष्ट सभी प्रकार के सारूप्य को अनुप्रास कहते हैं । २ सारूप्य शब्द इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अनुप्रास में स्वर-व्यञ्जन-समुदाय की समग्रतः आवृत्ति भी हो सकती है और अंशतः भी। अभिप्राय यह कि यमक में स्वर-व्यञ्जन-सङ्घ की सम्पूर्णता में आवृत्ति अपेक्षित होती है; पर अनुप्रास में स्वर-भेद से भी केवल व्यञ्जन की आवृत्ति हो सकती है । वामन के अनुसार अनुप्रास का स्वरूप समझने के लिए उनके यमक के स्वरूप का विचार आवश्यक होगा। उनके यमक-लक्षण पर दृष्टि रखते हुए उनके अनुप्रास का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है जहां एकार्थक अथवा अनेकार्थक पदों की
१. द्रष्टव्य-उद्भट, काव्यालं० सार सं० १, ३-२० २. शेषःसरूपोऽनुप्रासः। -वामन, काव्यालंसू० ४, १-८ तथा उसकी वृत्ति-पदमेकार्थमनेकार्थं च स्थानानियतं तद्विधमक्षरं च शेषः।
-वही, पृ० १७७