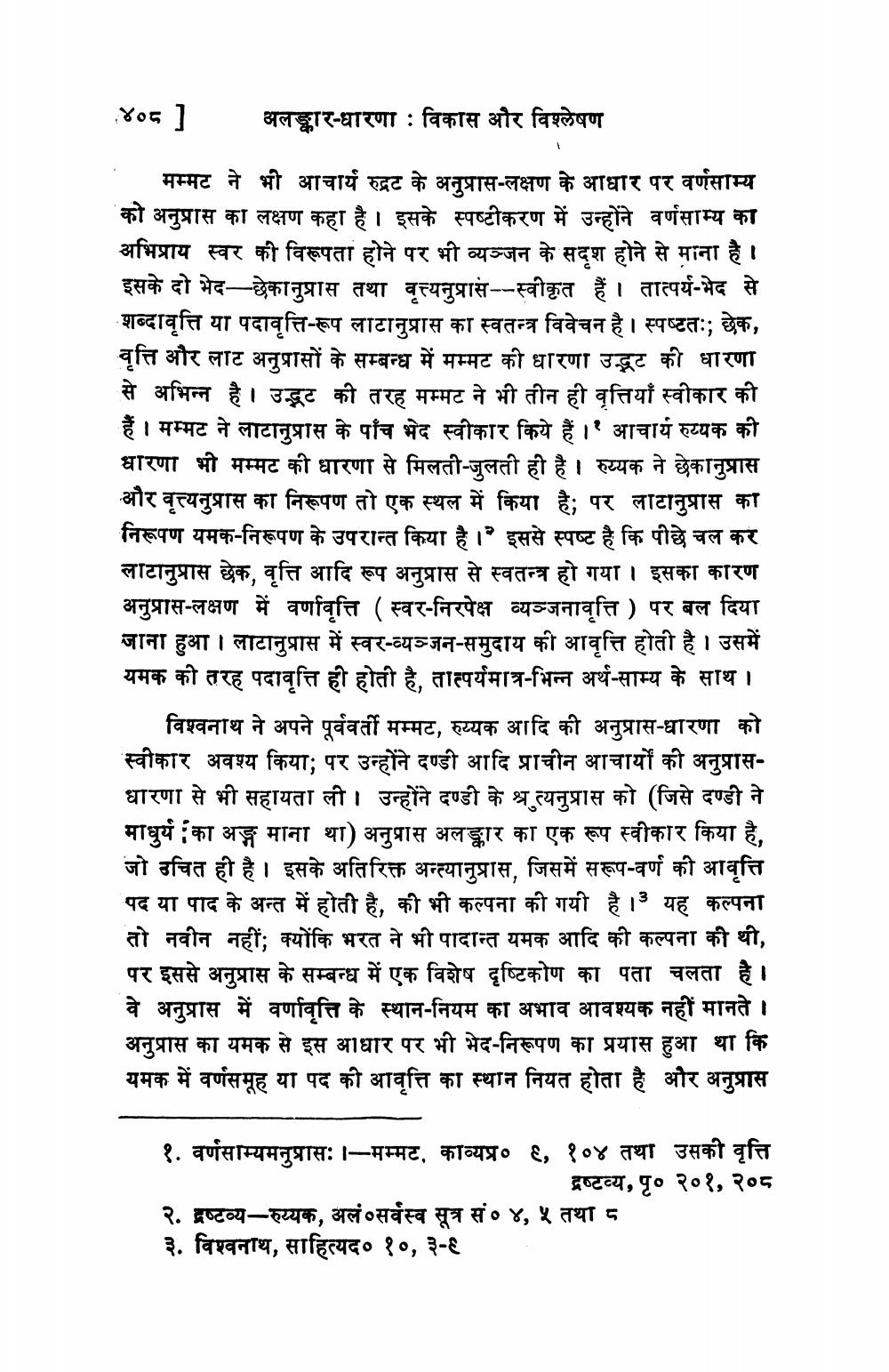________________
४०८ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
___मम्मट ने भी आचार्य रुद्रट के अनुप्रास-लक्षण के आधार पर वर्णसाम्य को अनुप्रास का लक्षण कहा है। इसके स्पष्टीकरण में उन्होंने वर्णसाम्य का अभिप्राय स्वर की विरूपता होने पर भी व्यञ्जन के सदृश होने से माना है। इसके दो भेद-छेकानुप्रास तथा वृत्त्यनुप्रास--स्वीकृत हैं। तात्पर्य-भेद से शब्दावृत्ति या पदावृत्ति-रूप लाटानुप्रास का स्वतन्त्र विवेचन है। स्पष्टतः; छेक, वृत्ति और लाट अनुप्रासों के सम्बन्ध में मम्मट की धारणा उद्भट की धारणा से अभिन्न है। उद्भट की तरह मम्मट ने भी तीन ही वृत्तियाँ स्वीकार की हैं । मम्मट ने लाटानुप्रास के पाँच भेद स्वीकार किये हैं।' आचार्य रुय्यक की धारणा भी मम्मट की धारणा से मिलती-जुलती ही है। रुय्यक ने छेकानुप्रास
और वृत्त्यनुप्रास का निरूपण तो एक स्थल में किया है; पर लाटानुप्रास का निरूपण यमक-निरूपण के उपरान्त किया है। इससे स्पष्ट है कि पीछे चल कर लाटानुप्रास छेक, वत्ति आदि रूप अनुप्रास से स्वतन्त्र हो गया। इसका कारण अनुप्रास-लक्षण में वर्णावृत्ति ( स्वर-निरपेक्ष व्यञ्जनावृत्ति ) पर बल दिया जाना हुआ। लाटानुप्रास में स्वर-व्यञ्जन-समुदाय की आवृत्ति होती है। उसमें यमक की तरह पदावृत्ति ही होती है, तात्पर्यमात्र-भिन्न अर्थ-साम्य के साथ।
विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती मम्मट, रुय्यक आदि की अनुप्रास-धारणा को स्वीकार अवश्य किया; पर उन्होंने दण्डी आदि प्राचीन आचार्यों की अनुप्रासधारणा से भी सहायता ली। उन्होंने दण्डी के श्र त्यनुप्रास को (जिसे दण्डी ने माधुर्य का अङ्ग माना था) अनुप्रास अलङ्कार का एक रूप स्वीकार किया है, जो उचित ही है। इसके अतिरिक्त अन्त्यानुप्रास, जिसमें सरूप-वर्ण की आवृत्ति पद या पाद के अन्त में होती है, की भी कल्पना की गयी है। यह कल्पना तो नवीन नहीं; क्योंकि भरत ने भी पादान्त यमक आदि की कल्पना की थी, पर इससे अनुप्रास के सम्बन्ध में एक विशेष दृष्टिकोण का पता चलता है। वे अनुप्रास में वर्णावृत्ति के स्थान-नियम का अभाव आवश्यक नहीं मानते । अनुप्रास का यमक से इस आधार पर भी भेद-निरूपण का प्रयास हुआ था कि यमक में वर्णसमूह या पद की आवृत्ति का स्थान नियत होता है और अनुप्रास
१. वर्णसाम्यमनुप्रासः।-मम्मट, काव्यप्र० ६, १०४ तथा उसकी वृत्ति
द्रष्टव्य, पृ० २०१, २०८ २. द्रष्टव्य-रुय्यक, अलं सर्वस्व सूत्र सं० ४, ५ तथा ८ ३. विश्वनाथ, साहित्यद० १०, ३-६