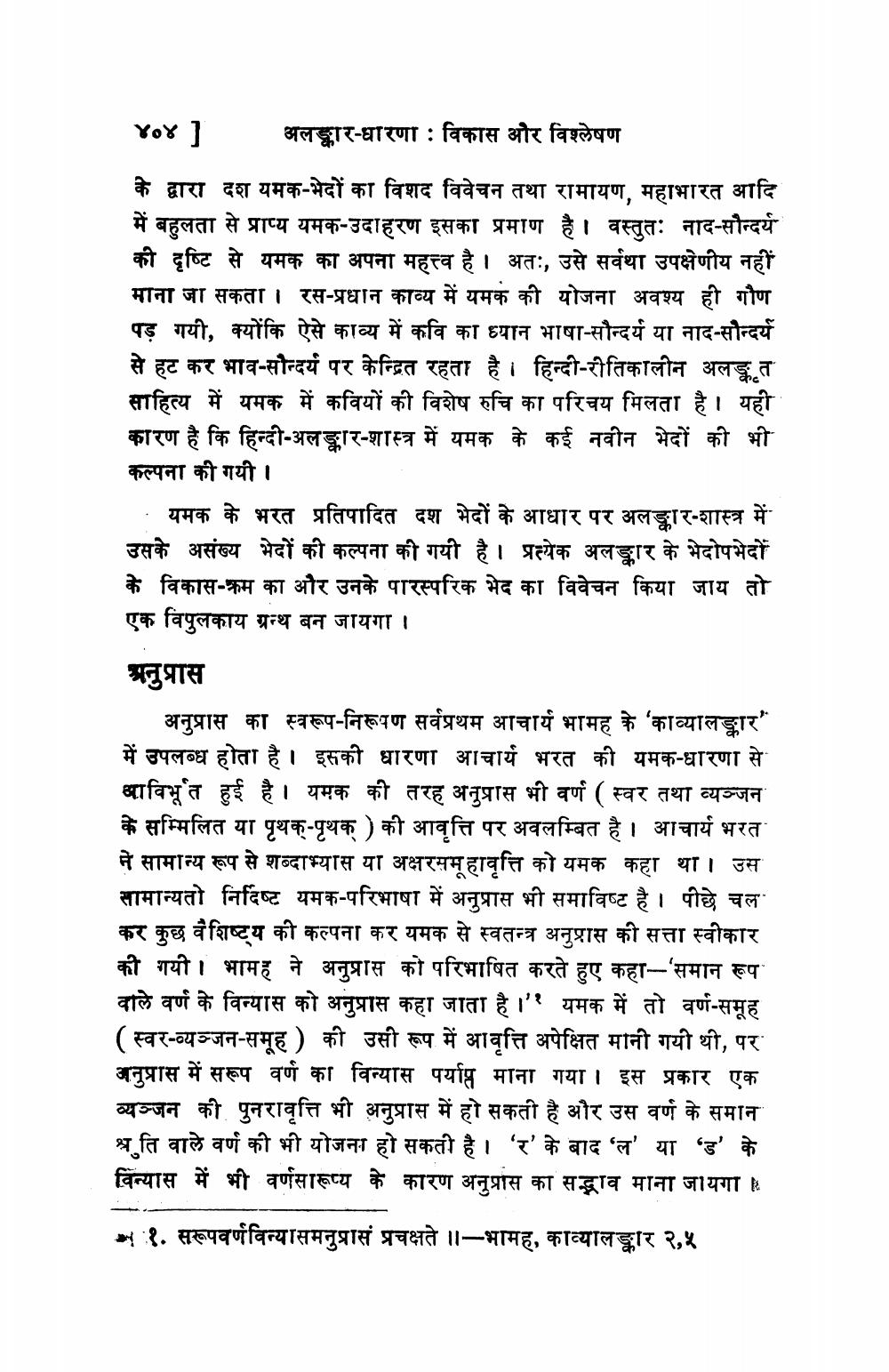________________
४०४ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
के द्वारा दश यमक-भेदों का विशद विवेचन तथा रामायण, महाभारत आदि में बहुलता से प्राप्य यमक-उदाहरण इसका प्रमाण है। वस्तुतः नाद-सौन्दर्य की दृष्टि से यमक का अपना महत्त्व है। अतः, उसे सर्वथा उपक्षेणीय नहीं माना जा सकता। रस-प्रधान काव्य में यमक की योजना अवश्य ही गौण पड़ गयी, क्योंकि ऐसे काव्य में कवि का ध्यान भाषा-सौन्दर्य या नाद-सौन्दर्य से हट कर भाव-सौन्दर्य पर केन्द्रित रहता है। हिन्दी-रीतिकालीन अलङ्कत साहित्य में यमक में कवियों की विशेष रुचि का परिचय मिलता है। यही कारण है कि हिन्दी-अलङ्कार-शास्त्र में यमक के कई नवीन भेदों की भी कल्पना की गयी।
- यमक के भरत प्रतिपादित दश भेदों के आधार पर अलङ्कार-शास्त्र में उसके असंख्य भेदों की कल्पना की गयी है। प्रत्येक अलङ्कार के भेदोपभेदों के विकास-क्रम का और उनके पारस्परिक भेद का विवेचन किया जाय तो एक विपुलकाय ग्रन्थ बन जायगा । अनुप्रास
अनुप्रास का स्वरूप-निरूपण सर्वप्रथम आचार्य भामह के 'काव्यालङ्कार' में उपलब्ध होता है। इसकी धारणा आचार्य भरत की यमक-धारणा से बाविर्भूत हुई है। यमक की तरह अनुप्रास भी वर्ण ( स्वर तथा व्यञ्जन के सम्मिलित या पृथक्-पृथक् ) की आवृत्ति पर अवलम्बित है। आचार्य भरत ने सामान्य रूप से शब्दाभ्यास या अक्षरसमूहावृत्ति को यमक कहा था। उस सामान्यतो निर्दिष्ट यमक-परिभाषा में अनुप्रास भी समाविष्ट है। पीछे चल कर कुछ वैशिष्ट्य की कल्पना कर यमक से स्वतन्त्र अनुप्रास की सत्ता स्वीकार की गयी। भामह ने अनुप्रास को परिभाषित करते हुए कहा-'समान रूप वाले वर्ण के विन्यास को अनुप्रास कहा जाता है।'' यमक में तो वर्ण-समूह (स्वर-व्यञ्जन-समूह) की उसी रूप में आवृत्ति अपेक्षित मानी गयी थी, पर अनुप्रास में सरूप वर्ण का विन्यास पर्याप्त माना गया। इस प्रकार एक व्यञ्जन की पुनरावृत्ति भी अनुप्रास में हो सकती है और उस वर्ण के समान श्रुति वाले वर्ण की भी योजना हो सकती है। 'र' के बाद 'ल' या 'ड' के विन्यास में भी वर्णसारूप्य के कारण अनुप्रास का सद्भाव माना जायगा ।
१. सरूपवर्णविन्यासमनुप्रासं प्रचक्षते ॥–भामह, काव्यालङ्कार २,५