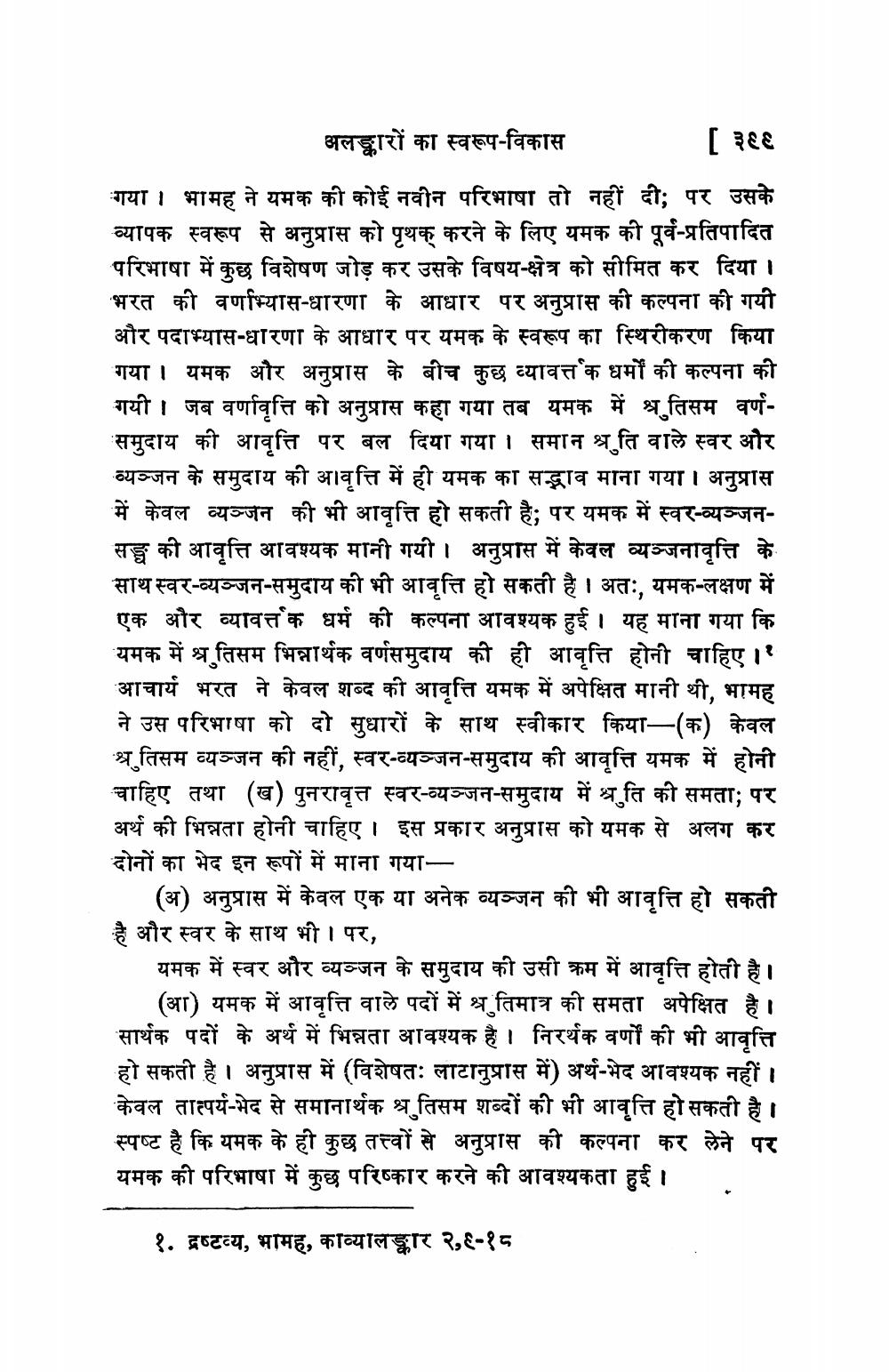________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ३६६ गया । भामह ने यमक की कोई नवीन परिभाषा तो नहीं दी; पर उसके व्यापक स्वरूप से अनुप्रास को पृथक् करने के लिए यमक की पूर्व प्रतिपादित परिभाषा में कुछ विशेषण जोड़ कर उसके विषय क्षेत्र को सीमित कर दिया । भरत की वर्णाभ्यास-धारणा के आधार पर अनुप्रास की कल्पना की गयी और पदाभ्यास-धारणा के आधार पर यमक के स्वरूप का स्थिरीकरण किया गया। यमक और अनुप्रास के बीच कुछ व्यावत के धर्मों की कल्पना की गयी। जब वर्णावृत्ति को अनुप्रास कहा गया तब यमक में श्र ुतिसम वर्णसमुदाय की आवृत्ति पर बल दिया गया । समान श्रुति वाले स्वर और व्यञ्जन के समुदाय की आवृत्ति में ही यमक का सद्भाव माना गया। अनुप्रास में केवल व्यञ्जन की भी आवृत्ति हो सकती है; पर यमक में स्वर- व्यञ्जनसङ्घ की आवृत्ति आवश्यक मानी गयी । अनुप्रास में केवल व्यञ्जनावृत्ति के साथ स्वर-व्यञ्जन-समुदाय की भी आवृत्ति हो सकती है । अतः, यमक - लक्षण में एक और व्यावर्त्तक धर्म की कल्पना आवश्यक हुई। यह माना गया कि यमक में श्रुतिसमभिन्नार्थक वर्णसमुदाय की ही आवृत्ति होनी चाहिए । आचार्य भरत ने केवल शब्द की आवृत्ति यमक में अपेक्षित मानी थी, भामह ने उस परिभाषा को दो सुधारों के साथ स्वीकार किया— (क) केवल श्र ुतिसम व्यञ्जन की नहीं, स्वर- व्यञ्जन-समुदाय की आवृत्ति यमक में होनी चाहिए तथा (ख) पुनरावृत्त स्वर - व्यञ्जन - समुदाय में श्र ुति की समता; पर अर्थ की भिन्नता होनी चाहिए । इस प्रकार अनुप्रास को यमक से अलग कर दोनों का भेद इन रूपों में माना गया -
(अ) अनुप्रास में केवल एक या अनेक व्यञ्जन की भी आवृत्ति हो सकती है और स्वर के साथ भी । पर,
यमक में स्वर और व्यञ्जन के समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति होती है ।
( आ ) यमक में आवृत्ति वाले पदों में श्रुतिमात्र की समता अपेक्षित है । सार्थक पदों के अर्थ में भिन्नता आवश्यक है । निरर्थक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है । अनुप्रास में (विशेषतः लाटानुप्रास में) अर्थ-भेद आवश्यक नहीं । केवल तात्पर्य-भेद से समानार्थक श्र ुतिसम शब्दों की भी आवृत्ति हो सकती है । स्पष्ट है कि यमक के ही कुछ तत्त्वों से अनुप्रास की कल्पना कर लेने पर यमक की परिभाषा में कुछ परिष्कार करने की आवश्यकता हुई ।
१. द्रष्टव्य, भामह, काव्यालङ्कार २,६-१८