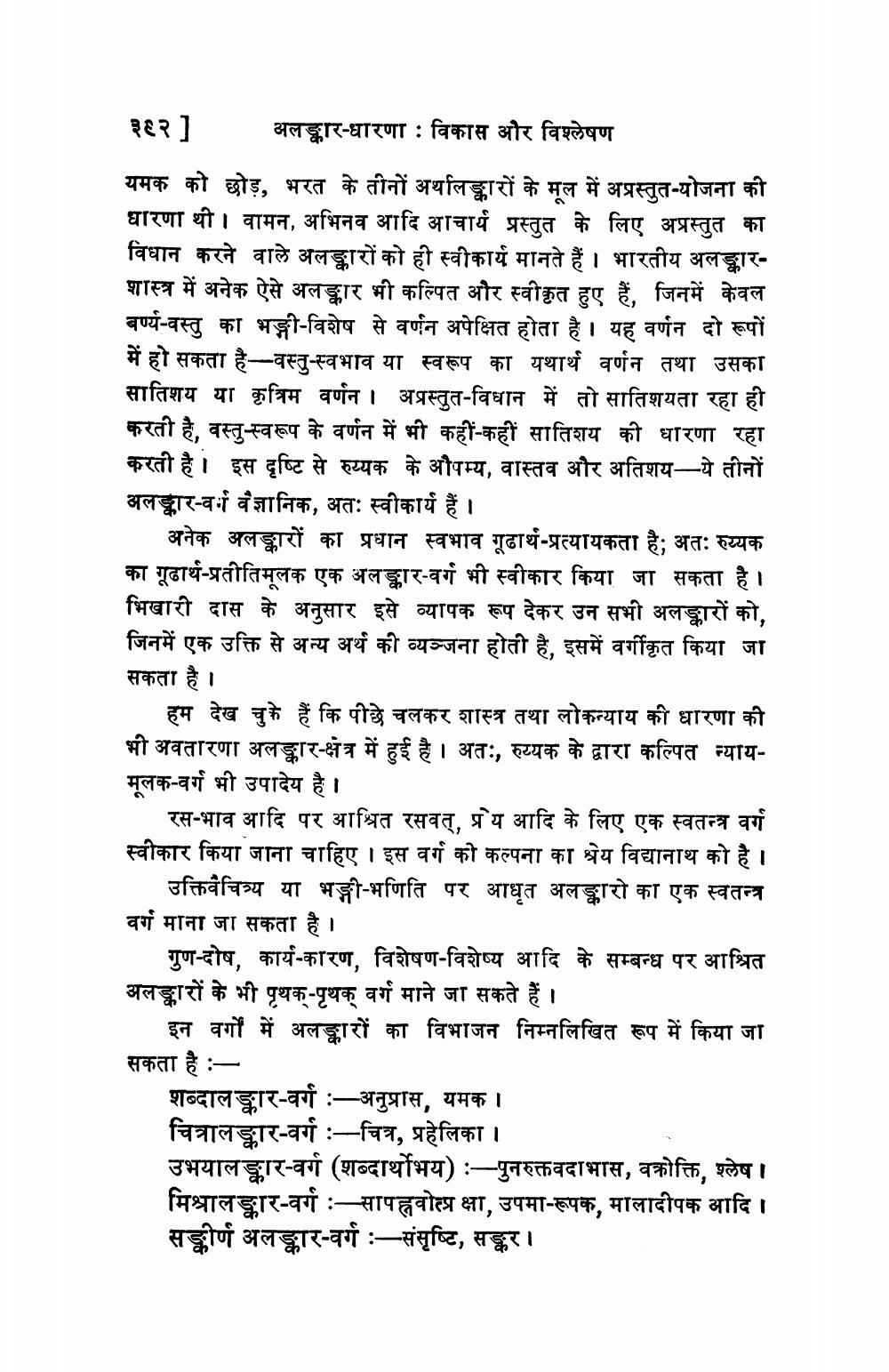________________
३९२] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण यमक को छोड़, भरत के तीनों अर्थालङ्कारों के मूल में अप्रस्तुत-योजना की धारणा थी। वामन, अभिनव आदि आचार्य प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का विधान करने वाले अलङ्कारों को ही स्वीकार्य मानते हैं। भारतीय अलङ्कारशास्त्र में अनेक ऐसे अलङ्कार भी कल्पित और स्वीकृत हुए हैं, जिनमें केवल वर्ण्य-वस्तु का भङ्गी-विशेष से वर्णन अपेक्षित होता है। यह वर्णन दो रूपों में हो सकता है-वस्तु-स्वभाव या स्वरूप का यथार्थ वर्णन तथा उसका सातिशय या कृत्रिम वर्णन । अप्रस्तुत-विधान में तो सातिशयता रहा ही करती है, वस्तु-स्वरूप के वर्णन में भी कहीं-कहीं सातिशय की धारणा रहा करती है। इस दृष्टि से रुय्यक के औपम्य, वास्तव और अतिशय-ये तीनों अलङ्कार-वर्ग वैज्ञानिक, अतः स्वीकार्य हैं। ___ अनेक अलङ्कारों का प्रधान स्वभाव गूढार्थ-प्रत्यायकता है; अतः रुय्यक का गूढार्थ-प्रतीतिमूलक एक अलङ्कार-वर्ग भी स्वीकार किया जा सकता है। भिखारी दास के अनुसार इसे व्यापक रूप देकर उन सभी अलङ्कारों को, जिनमें एक उक्ति से अन्य अर्थ की व्यञ्जना होती है, इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है।
हम देख चुके हैं कि पीछे चलकर शास्त्र तथा लोकन्याय की धारणा की भी अवतारणा अलङ्कार-क्षेत्र में हुई है । अतः, रुय्यक के द्वारा कल्पित न्यायमूलक-वर्ग भी उपादेय है। ____ रस-भाव आदि पर आश्रित रसवत्, प्रय आदि के लिए एक स्वतन्त्र वर्ग स्वीकार किया जाना चाहिए । इस वर्ग को कल्पना का श्रेय विद्यानाथ को है ।
उक्तिवैचित्र्य या भङ्गी-भणिति पर आधृत अलङ्कारो का एक स्वतन्त्र वर्ग माना जा सकता है।
गुण-दोष, कार्य-कारण, विशेषण-विशेष्य आदि के सम्बन्ध पर आश्रित अलङ्कारों के भी पृथक्-पृथक् वर्ग माने जा सकते हैं।
इन वर्गों में अलङ्कारों का विभाजन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :
शब्दालङ्कार-वर्ग :-अनुप्रास, यमक । चित्रालङ्कार-वर्ग :-चित्र, प्रहेलिका । उभयालङ्कार-वर्ग (शब्दार्थोभय):-पुनरुक्तवदाभास, वक्रोक्ति, श्लेष । मिश्रालङ्कार-वर्ग :-सापह्नवोत्प्र क्षा, उपमा-रूपक, मालादीपक आदि । सङ्कीर्ण अलङ्कार-वर्ग :-संसृष्टि, सङ्कर ।