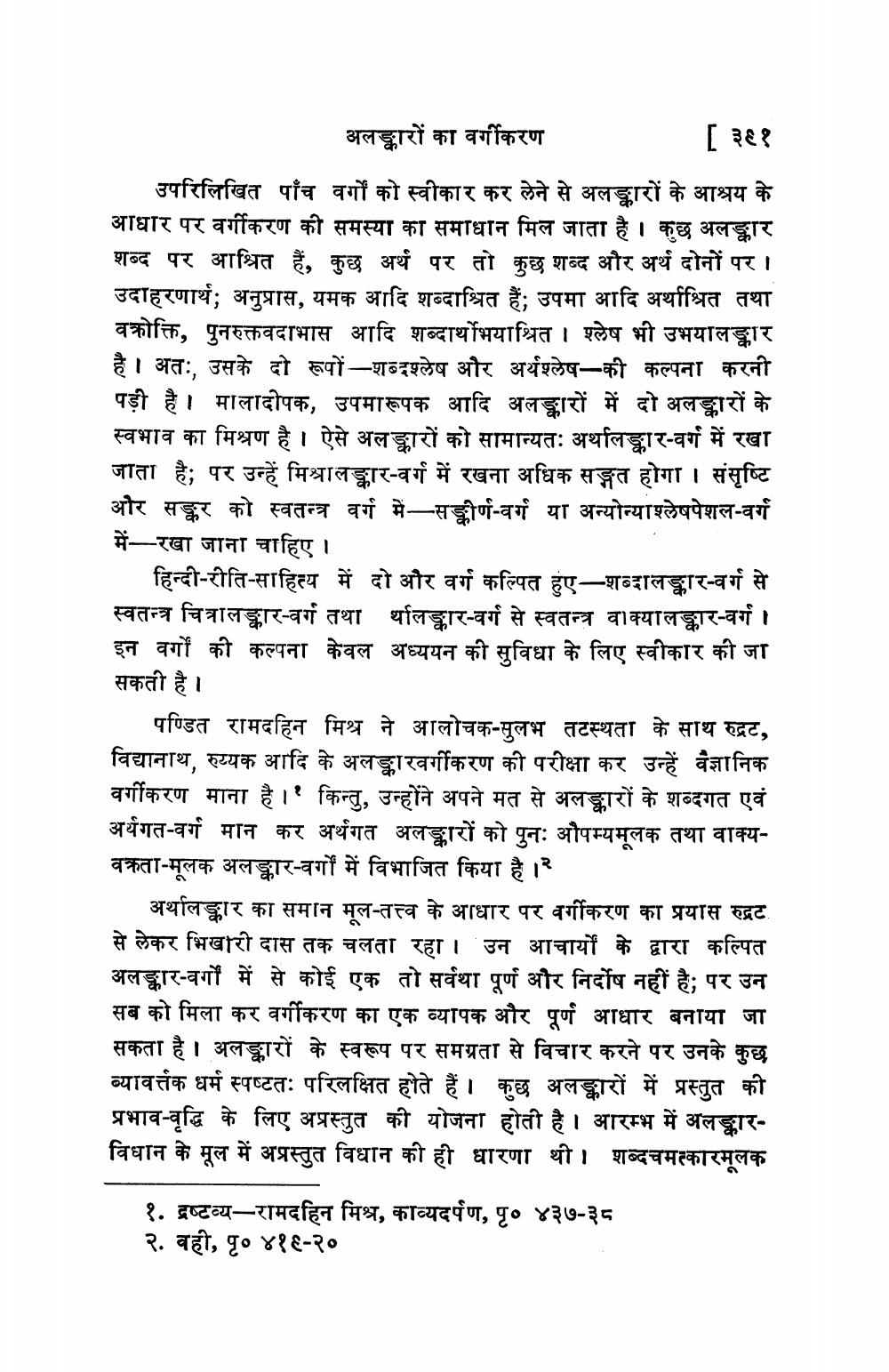________________
अलङ्कारों का वर्गीकरण
[ ३६१ उपरिलिखित पाँच वर्गों को स्वीकार कर लेने से अलङ्कारों के आश्रय के आधार पर वर्गीकरण की समस्या का समाधान मिल जाता है। कुछ अलङ्कार शब्द पर आश्रित हैं, कुछ अर्थ पर तो कुछ शब्द और अर्थ दोनों पर । उदाहरणार्थ; अनुप्रास, यमक आदि शब्दाश्रित हैं; उपमा आदि अर्थाश्रित तथा वक्रोक्ति, पुनरुक्तवदाभास आदि शब्दार्थोभयाश्रित । श्लेष भी उभयालङ्कार है। अतः, उसके दो रूपों-शब्दश्लेष और अर्थश्लेष-की कल्पना करनी पड़ी है। मालादोपक, उपमारूपक आदि अलङ्कारों में दो अलङ्कारों के स्वभाव का मिश्रण है । ऐसे अलङ्कारों को सामान्यतः अर्थालङ्कार-वर्ग में रखा जाता है; पर उन्हें मिश्रालङ्कार-वर्ग में रखना अधिक सङ्गत होगा। संसृष्टि और सङ्कर को स्वतन्त्र वर्ग में—सङ्कीर्ण-वर्ग या अन्योन्याश्लेषपेशल-वर्ग में रखा जाना चाहिए।
हिन्दी-रीति-साहित्य में दो और वर्ग कल्पित हए-शब्दालङ्कार-वर्ग से स्वतन्त्र चित्रालङ्कार-वर्ग तथा लिङ्कार-वर्ग से स्वतन्त्र वाक्यालङ्कार-वर्ग । इन वर्गों की कल्पना केवल अध्ययन की सुविधा के लिए स्वीकार की जा सकती है।
पण्डित रामदहिन मिश्र ने आलोचक-सुलभ तटस्थता के साथ रुद्रट, विद्यानाथ, रुय्यक आदि के अलङ्कारवर्गीकरण की परीक्षा कर उन्हें वैज्ञानिक वर्गीकरण माना है। किन्तु, उन्होंने अपने मत से अलङ्कारों के शब्दगत एवं अर्थगत-वर्ग मान कर अर्थगत अलङ्कारों को पुनः औपम्यमूलक तथा वाक्यवक्रता-मूलक अलङ्कार-वर्गों में विभाजित किया है।
अर्थालङ्कार का समान मूल-तत्त्व के आधार पर वर्गीकरण का प्रयास रुद्रट से लेकर भिखारी दास तक चलता रहा। उन आचार्यों के द्वारा कल्पित अलङ्कार-वर्गों में से कोई एक तो सर्वथा पूर्ण और निर्दोष नहीं है; पर उन सब को मिला कर वर्गीकरण का एक व्यापक और पूर्ण आधार बनाया जा सकता है। अलङ्कारों के स्वरूप पर समग्रता से विचार करने पर उनके कुछ ब्यावर्तक धर्म स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। कुछ अलङ्कारों में प्रस्तुत की प्रभाव-वृद्धि के लिए अप्रस्तुत की योजना होती है। आरम्भ में अलङ्कारविधान के मूल में अप्रस्तुत विधान की ही धारणा थी। शब्दचमत्कारमूलक
१. द्रष्टव्य-रामदहिन मिश्र, काव्यदर्पण, पृ० ४३७-३८ २. वही, पृ० ४१६-२०