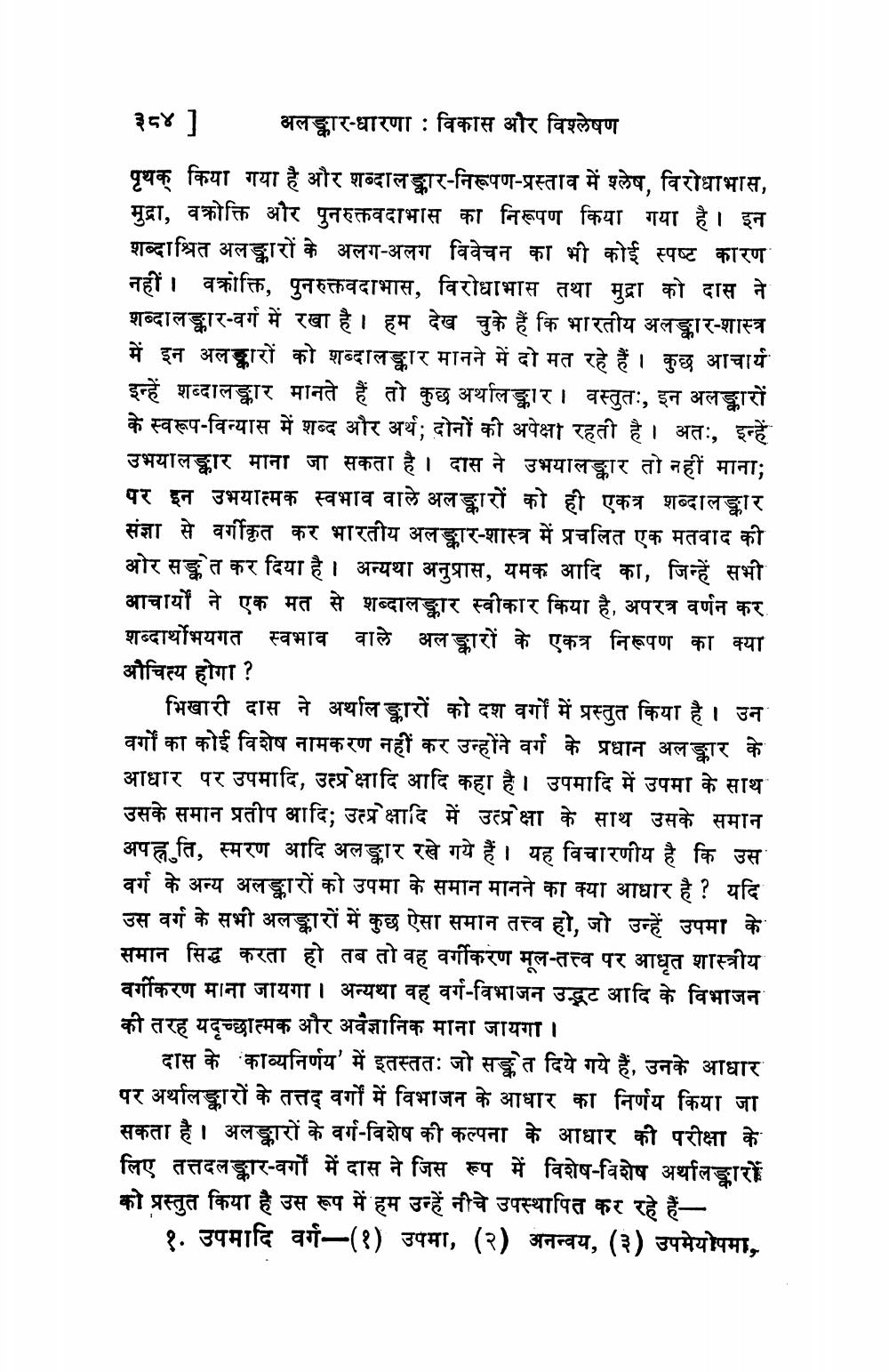________________
३८४ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
पृथक् किया गया है और शब्दालङ्कार - निरूपण - प्रस्ताव में श्लेष, विरोधाभास, मुद्रा, वक्रोक्ति और पुनरुक्तवदाभास का निरूपण किया गया है । इन शब्दाश्रित अलङ्कारों के अलग-अलग विवेचन का भी कोई स्पष्ट कारण नहीं । वक्रोक्ति, पुनरुक्तवदाभास, विरोधाभास तथा मुद्रा को दास ने शब्दालङ्कार-वर्ग में रखा है । हम देख चुके हैं कि भारतीय अलङ्कार-शास्त्र में इन अलङ्कारों को शब्दालङ्कार मानने में दो मत रहे हैं । कुछ आचार्य इन्हें शब्दालङ्कार मानते हैं तो कुछ अर्थालङ्कार । वस्तुतः, इन अलङ्कारों के स्वरूप - विन्यास में शब्द और अर्थ; दोनों की अपेक्षा रहती है । अतः, इन्हें उभयालङ्कार माना जा सकता है । दास ने उभयालङ्कार तो नहीं माना; पर इन उभयात्मक स्वभाव वाले अलङ्कारों को ही एकत्र शब्दालङ्कार संज्ञा से वर्गीकृत कर भारतीय अलङ्कार - शास्त्र में प्रचलित एक मतवाद की ओर सङ्क ेत कर दिया है । अन्यथा अनुप्रास, यमक आदि का, जिन्हें सभी आचार्यों ने एक मत से शब्दालङ्कार स्वीकार किया है, अपरत्र वर्णन कर शब्दार्थोभयगत स्वभाव वाले अलङ्कारों के एकत्र निरूपण का क्या औचित्य होगा ?
भिखारी दास ने अर्थालङ्कारों को दश वर्गों में प्रस्तुत किया है। उन वर्गों का कोई विशेष नामकरण नहीं कर उन्होंने वर्ग के प्रधान अलङ्कार के आधार पर उपमादि, उत्प्र ेक्षादि आदि कहा है । उपमादि में उपमा के साथ उसके समान प्रतीप आदि; उत्प्र ेक्षादि में उत्प्रेक्षा के साथ उसके समान अपह्न ुति, स्मरण आदि अलङ्कार रखे गये हैं । यह विचारणीय है कि उस वर्ग के अन्य अलङ्कारों को उपमा के समान मानने का क्या आधार है ? यदि उस वर्ग के सभी अलङ्कारों में कुछ ऐसा समान तत्त्व हो, जो उन्हें उपमा के समान सिद्ध करता हो तब तो वह वर्गीकरण मूल तत्त्व पर आधृत शास्त्रीय वर्गीकरण माना जायगा । अन्यथा वह वर्ग-विभाजन उद्भट आदि के विभाजन की तरह यदृच्छात्मक और अवैज्ञानिक माना जायगा ।
दास के 'काव्यनिर्णय' में इतस्ततः जो सङ्केत दिये गये हैं, उनके आधार पर अर्थालङ्कारों के तत्तद् वर्गों में विभाजन के आधार का निर्णय किया जा सकता है । अलङ्कारों के वर्ग विशेष की कल्पना के आधार की परीक्षा के लिए तत्तदलङ्कार-वर्गों में दास ने जिस रूप में विशेष - विशेष अर्थालङ्कारों को प्रस्तुत किया है उस रूप में हम उन्हें नीचे उपस्थापित कर रहे हैं
१. उपमादि वर्ग - ( १ ) उपमा, (२) अनन्वय, (३) उपमेयोपमा,