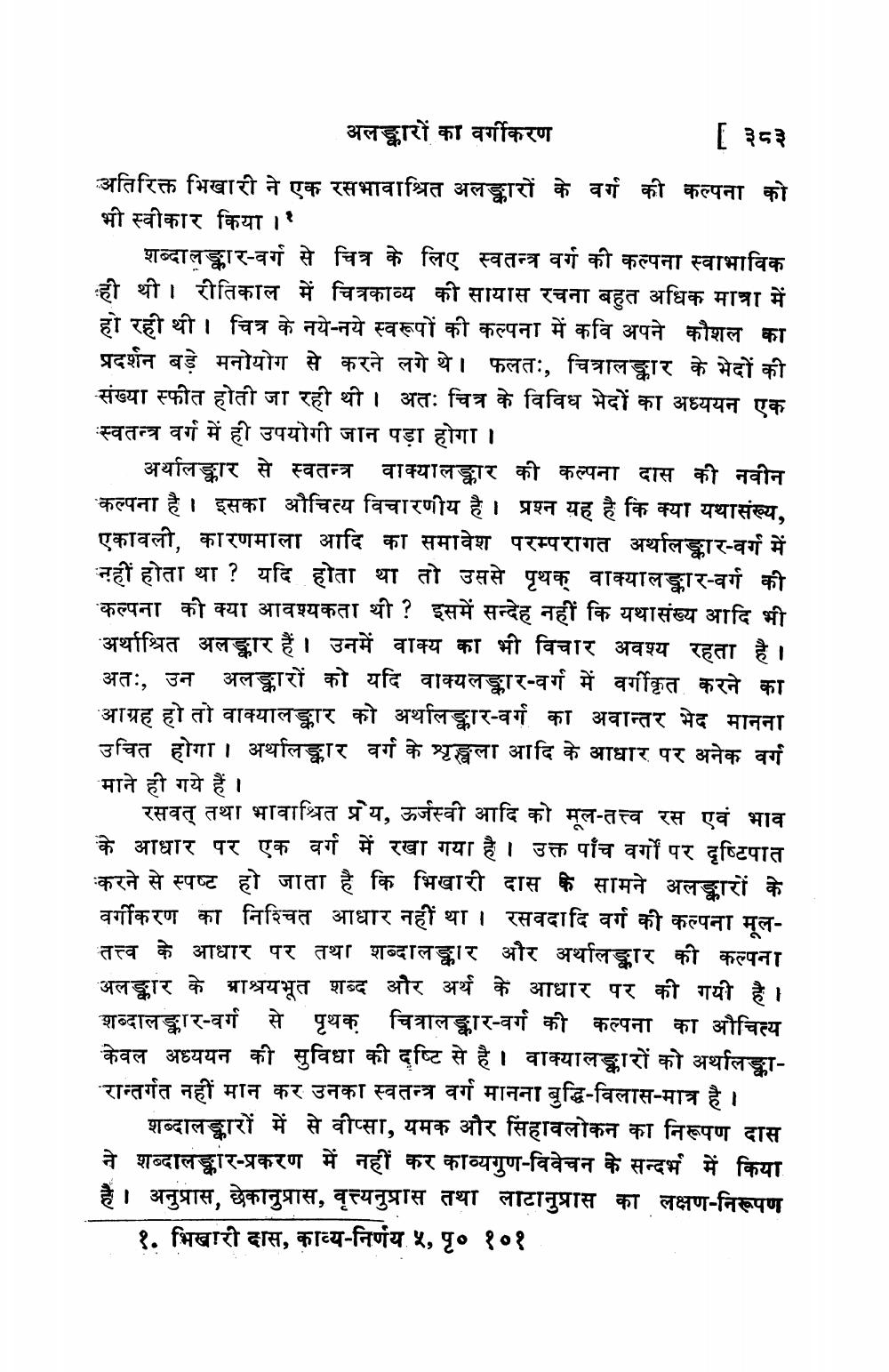________________
अलङ्कारों का वर्गीकरण
[ ३८३ अतिरिक्त भिखारी ने एक रसभावाश्रित अलङ्कारों के वर्ग की कल्पना को भी स्वीकार किया।' ___ शब्दालङ्कार-वर्ग से चित्र के लिए स्वतन्त्र वर्ग की कल्पना स्वाभाविक ही थी। रीतिकाल में चित्रकाव्य की सायास रचना बहुत अधिक मात्रा में हो रही थी। चित्र के नये-नये स्वरूपों की कल्पना में कवि अपने कौशल का प्रदर्शन बड़े मनोयोग से करने लगे थे। फलतः, चित्रालङ्कार के भेदों की संख्या स्फीत होती जा रही थी। अतः चित्र के विविध भेदों का अध्ययन एक स्वतन्त्र वर्ग में ही उपयोगी जान पड़ा होगा। ___ अर्थालङ्कार से स्वतन्त्र वाक्यालङ्कार की कल्पना दास की नवीन कल्पना है। इसका औचित्य विचारणीय है। प्रश्न यह है कि क्या यथासंख्य, एकावली, कारणमाला आदि का समावेश परम्परागत अर्थालङ्कार-वर्ग में नहीं होता था ? यदि होता था तो उससे पृथक् वाक्यालङ्कार-वर्ग की कल्पना की क्या आवश्यकता थी? इसमें सन्देह नहीं कि यथासंख्य आदि भी अर्थाश्रित अलङ्कार हैं। उनमें वाक्य का भी विचार अवश्य रहता है। अतः, उन अलङ्कारों को यदि वाक्यलङ्कार-वर्ग में वर्गीकृत करने का आग्रह हो तो वाक्यालङ्कार को अर्थालङ्कार-वर्ग का अवान्तर भेद मानना उचित होगा। अर्थालङ्कार वर्ग के शृङ्खला आदि के आधार पर अनेक वर्ग माने ही गये हैं। ___ रसवत् तथा भावाश्रित प्रेय, ऊर्जस्वी आदि को मूल-तत्त्व रस एवं भाव के आधार पर एक वर्ग में रखा गया है। उक्त पाँच वर्गों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि भिखारी दास के सामने अलङ्कारों के वर्गीकरण का निश्चित आधार नहीं था। रसवदादि वर्ग की कल्पना मूलतत्त्व के आधार पर तथा शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की कल्पना अलङ्कार के आश्रयभूत शब्द और अर्थ के आधार पर की गयी है। शब्दालङ्कार-वर्ग से पृथक चित्रालङ्कार-वर्ग की कल्पना का औचित्य केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से है। वाक्यालङ्कारों को अर्थालङ्कारान्तर्गत नहीं मान कर उनका स्वतन्त्र वर्ग मानना बुद्धि-विलास-मात्र है। ___शब्दालङ्कारों में से वीप्सा, यमक और सिंहावलोकन का निरूपण दास ने शब्दालङ्कार-प्रकरण में नहीं कर काव्यगुण-विवेचन के सन्दर्भ में किया है। अनुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास तथा लाटानुप्रास का लक्षण-निरूपण
१. भिखारी दास, काव्य-निर्णय ५, पृ० १०१