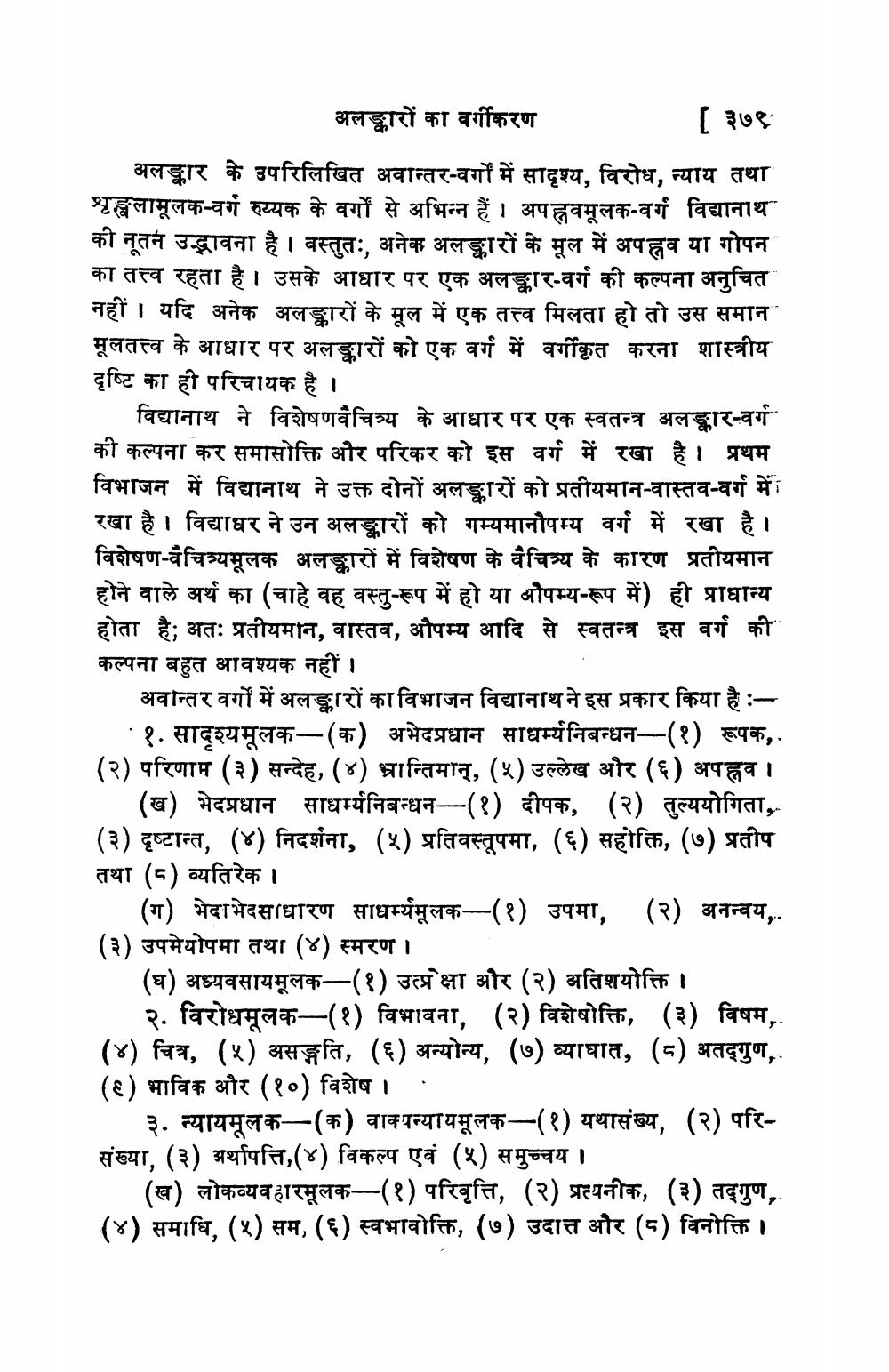________________
अलङ्कारों का वर्गीकरण
[ ३७९ अलङ्कार के उपरिलिखित अवान्तर-वर्गों में सादृश्य, विरोध, न्याय तथा शृङ्खलामूलक-वर्ग रुय्यक के वर्गों से अभिन्न हैं । अपह्नवमूलक-वर्ग विद्यानाथ की नूतन उद्भावना है । वस्तुतः, अनेक अलङ्कारों के मूल में अपह्नव या गोपन का तत्त्व रहता है। उसके आधार पर एक अलङ्कार-वर्ग की कल्पना अनुचित नहीं। यदि अनेक अलङ्कारों के मूल में एक तत्त्व मिलता हो तो उस समान मूलतत्त्व के आधार पर अलङ्कारों को एक वर्ग में वर्गीकृत करना शास्त्रीय दृष्टि का ही परिचायक है ।
विद्यानाथ ने विशेषणवैचित्र्य के आधार पर एक स्वतन्त्र अलङ्कार-वर्ग की कल्पना कर समासोक्ति और परिकर को इस वर्ग में रखा है। प्रथम विभाजन में विद्यानाथ ने उक्त दोनों अलङ्कारों को प्रतीयमान-वास्तव-वर्ग में रखा है। विद्याधर ने उन अलङ्कारों को गम्यमानौपम्य वर्ग में रखा है। विशेषण-वैचित्र्यमूलक अलङ्कारों में विशेषण के वैचित्र्य के कारण प्रतीयमान होने वाले अर्थ का (चाहे वह वस्तु-रूप में हो या औपम्य-रूप में) ही प्राधान्य होता है; अतः प्रतीयमान, वास्तव, औपम्य आदि से स्वतन्त्र इस वर्ग की कल्पना बहुत आवश्यक नहीं।
अवान्तर वर्गों में अलङ्कारों का विभाजन विद्यानाथ ने इस प्रकार किया है :
१. सादृश्यमूलक-(क) अभेदप्रधान साधर्म्यनिबन्धन-(१) रूपक,. (२) परिणाम (३) सन्देह, (४) भ्रान्तिमान्, (५) उल्लेख और (६) अपह्नव ।
(ख) भेदप्रधान साधर्म्यनिबन्धन-(१) दीपक, (२) तुल्ययोगिता, (३) दृष्टान्त, (४) निदर्शना, (५) प्रतिवस्तूपमा, (६) सहोक्ति, (७) प्रतीप तथा (८) व्यतिरेक ।
(ग) भेदाभेदसाधारण साधर्म्यमूलक-(१) उपमा, (२) अनन्वय,. (३) उपमेयोपमा तथा (४) स्मरण।
(घ) अध्यवसायमूलक-(१) उत्प्रेक्षा और (२) अतिशयोक्ति ।
२. विरोधमूलक-(१) विभावना, (२) विशेषोक्ति, (३) विषम, (४) चित्र, (५) असङ्गति, (६) अन्योन्य, (७) व्याघात, (८) अतद्गुण, (६) भाविक और (१०) विशेष । '
३. न्यायमूलक-(क) वाक्यन्यायमूलक-(१) यथासंख्य, (२) परिसंख्या, (३) अर्थापत्ति,(४) विकल्प एवं (५) समुच्चय । __ (ख) लोकव्यवहारमूलक-(१) परिवृत्ति, (२) प्रत्यनीक, (३) तद्गुण, (४) समाधि, (५) सम, (६) स्वभावोक्ति, (७) उदात्त और (८) विनोक्ति।