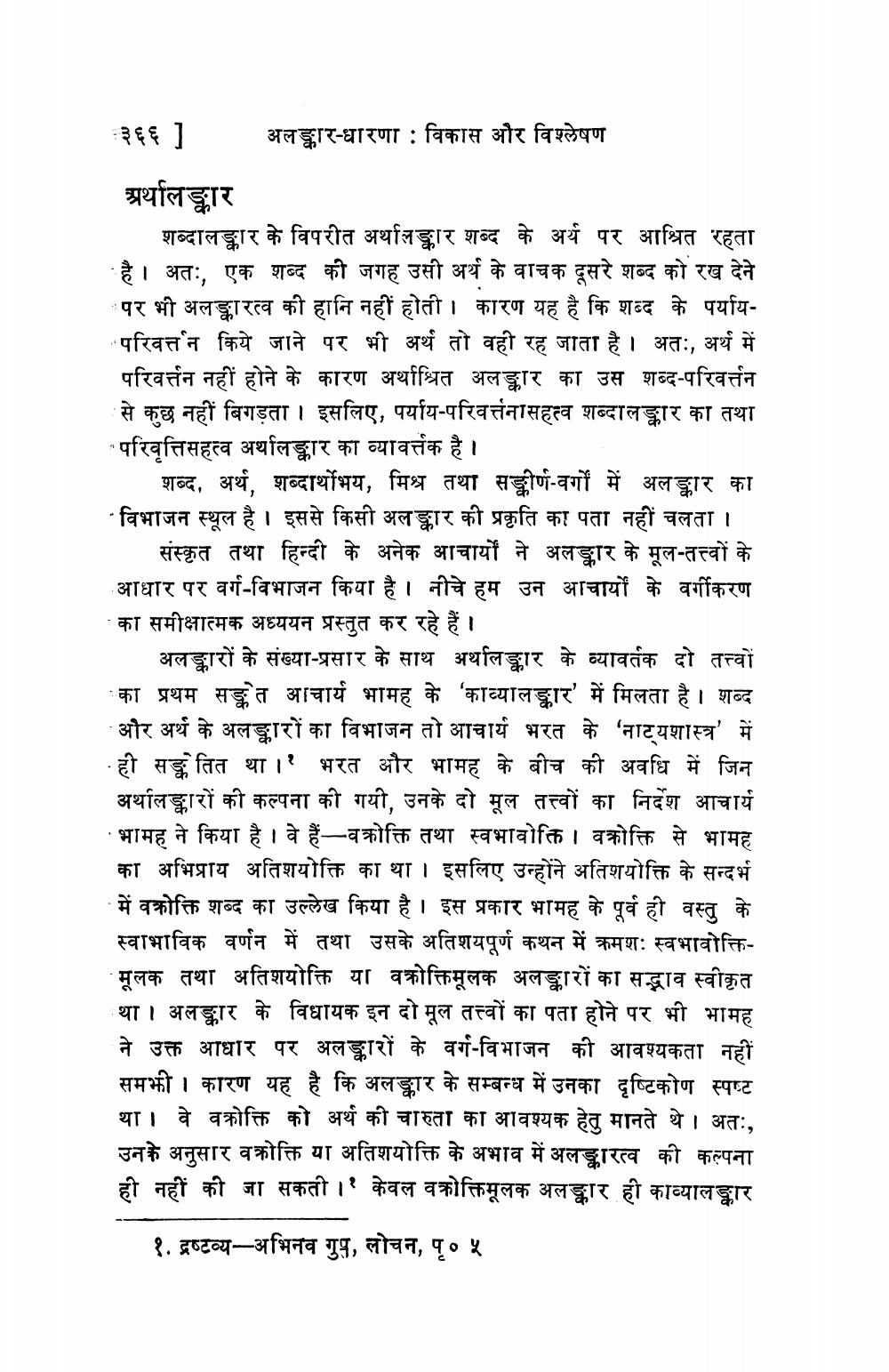________________
-३६६ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
अर्थालङ्कार
शब्दालङ्कार के विपरीत अर्थालङ्कार शब्द के अर्थ पर आश्रित रहता है । अतः, एक शब्द की जगह उसी अर्थ के वाचक दूसरे शब्द को रख देने पर भी अलङ्कारत्व की हानि नहीं होती । कारण यह है कि शब्द के पर्यायपरिवर्तन किये जाने पर भी अर्थ तो वही रह जाता है । अतः, अर्थ में परिवर्तन नहीं होने के कारण अर्थाश्रित अलङ्कार का उस शब्द - परिवर्तन से कुछ नहीं बिगड़ता । इसलिए, पर्याय - परिवर्तनासहत्व शब्दालङ्कार का तथा " परिवृत्तिसहत्व अर्थालङ्कार का व्यावर्त्तक है ।
शब्द, अर्थ, शब्दार्थोभय, मिश्र तथा सङ्कीर्ण-वर्गों में अलङ्कार का - विभाजन स्थूल है । इससे किसी अलङ्कार की प्रकृति का पता नहीं चलता । संस्कृत तथा हिन्दी के अनेक आचार्यों ने अलङ्कार के मूल तत्त्वों के • आधार पर वर्ग - विभाजन किया है । नीचे हम उन आचार्यों के वर्गीकरण - का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं ।
अलङ्कारों के संख्या-प्रसार के साथ अर्थालङ्कार के व्यावर्तक दो तत्त्वों का प्रथम सङ्केत आचार्य भामह के 'काव्यालङ्कार' में मिलता है । शब्द - और अर्थ के अलङ्कारों का विभाजन तो आचार्य भरत के 'नाट्यशास्त्र' में - ही सङ्केतित था । ' भरत और भामह के बीच की अवधि में जिन अर्थालङ्कारों की कल्पना की गयी, उनके दो मूल तत्त्वों का निर्देश आचार्य • भामह ने किया है । वे हैं - वक्रोक्ति तथा स्वभावोति । वक्रोक्ति से भामह का अभिप्राय अतिशयोक्ति का था । इसलिए उन्होंने अतिशयोक्ति के सन्दर्भ में वक्रोक्ति शब्द का उल्लेख किया है । इस प्रकार भामह के पूर्व ही वस्तु के स्वाभाविक वर्णन में तथा उसके अतिशयपूर्ण कथन में क्रमशः स्वभावोक्तिमूलक तथा अतिशयोक्ति या वक्रोक्तिमूलक अलङ्कारों का सद्भाव स्वीकृत था । अलङ्कार के विधायक इन दो मूल तत्त्वों का पता होने पर भी भामह ने उक्त आधार पर अलङ्कारों के वर्ग-विभाजन की आवश्यकता नहीं समझी। कारण यह है कि अलङ्कार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था । वे वक्रोक्ति को अर्थ की चारुता का आवश्यक हेतु मानते थे । अतः, उनके अनुसार वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति के अभाव में अलङ्कारत्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती । केवल वक्रोक्तिमूलक अलङ्कार ही काव्यालङ्कार
१. द्रष्टव्य - अभिनव गुप, लोचन, पृ० ५