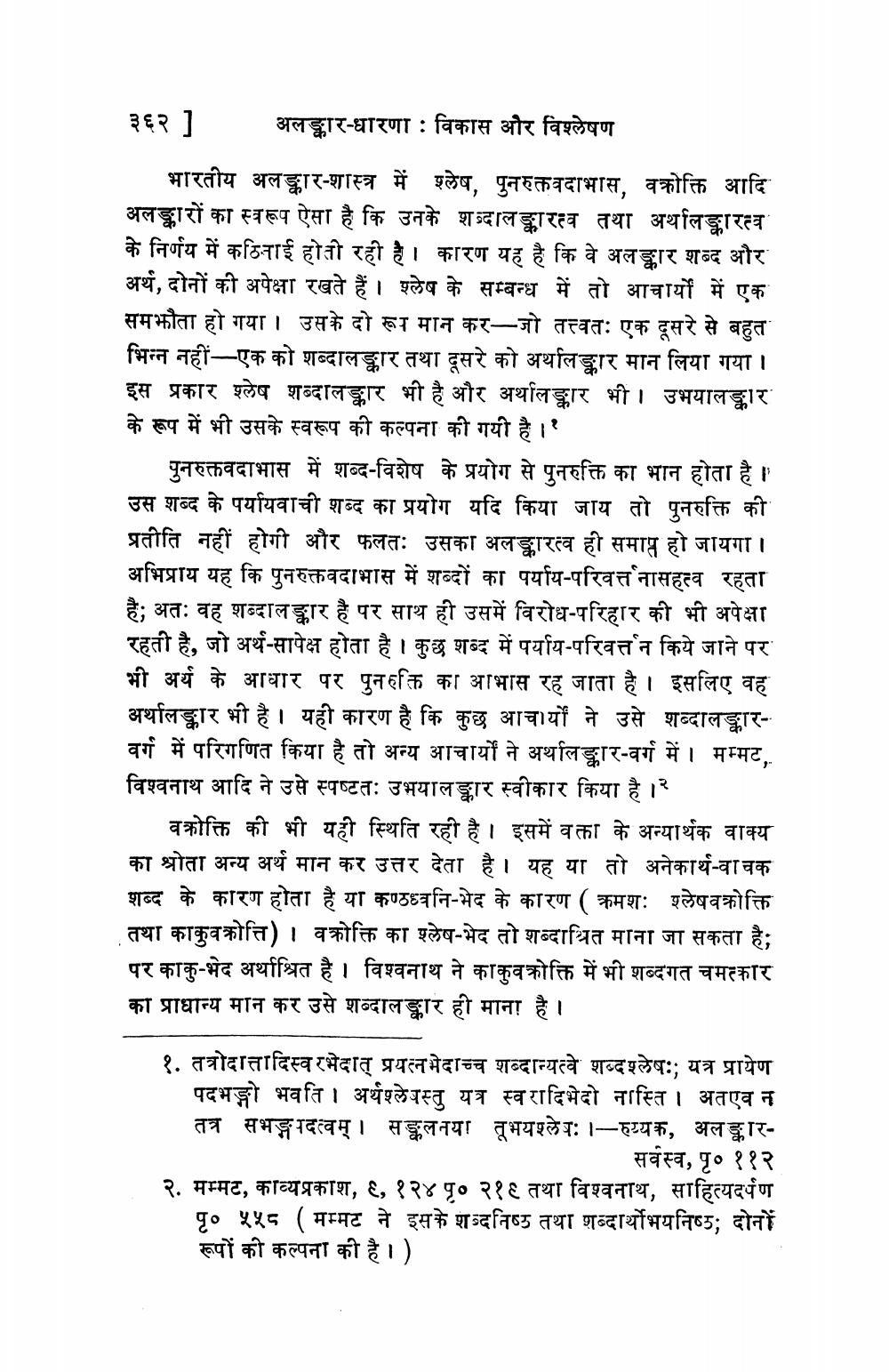________________
३६२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
भारतीय अलङ्कार-शास्त्र में श्लेष, पुनरुक्तवदाभास, वक्रोक्ति आदि अलङ्कारों का स्वरूप ऐसा है कि उनके शब्दालङ्कारत्व तथा अर्थालङ्कारत्व के निर्णय में कठिनाई होती रही है। कारण यह है कि वे अलङ्कार शब्द और अर्थ, दोनों की अपेक्षा रखते हैं। श्लेष के सम्बन्ध में तो आचार्यों में एक समझौता हो गया। उसके दो रूप मान कर-जो तत्त्वतः एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं-एक को शब्दालङ्कार तथा दूसरे को अर्थालङ्कार मान लिया गया। इस प्रकार श्लेष शब्दालङ्कार भी है और अर्थालङ्कार भी। उभयालङ्कार के रूप में भी उसके स्वरूप की कल्पना की गयी है।'
पुनरुक्तवदाभास में शब्द-विशेष के प्रयोग से पुनरुक्ति का भान होता है । उस शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग यदि किया जाय तो पुनरुक्ति की प्रतीति नहीं होगी और फलतः उसका अलङ्कारत्व ही समाप्त हो जायगा। अभिप्राय यह कि पुनरुक्तवदाभास में शब्दों का पर्याय-परिवर्तनासहत्व रहता है; अतः वह शब्दालङ्कार है पर साथ ही उसमें विरोध-परिहार की भी अपेक्षा रहती है, जो अर्थ-सापेक्ष होता है । कुछ शब्द में पर्याय-परिवर्तन किये जाने पर भी अर्य के आधार पर पुनरुक्ति का आभास रह जाता है। इसलिए वह अर्थालङ्कार भी है। यही कारण है कि कुछ आचार्यों ने उसे शब्दालङ्कारवर्ग में परिगणित किया है तो अन्य आचार्यों ने अर्थालङ्कार-वर्ग में। मम्मट, विश्वनाथ आदि ने उसे स्पष्टतः उभयालङ्कार स्वीकार किया है।
वक्रोक्ति की भी यही स्थिति रही है। इसमें वक्ता के अन्यार्थक वाक्य का श्रोता अन्य अर्थ मान कर उत्तर देता है। यह या तो अनेकार्थ-वाचक शब्द के कारण होता है या कण्ठध्वनि-भेद के कारण ( क्रमशः श्लेषवक्रोक्ति तथा काकुवक्रोत्ति)। वक्रोक्ति का श्लेष-भेद तो शब्दाश्रित माना जा सकता है; पर काकु-भेद अर्थाश्रित है। विश्वनाथ ने काकुवक्रोक्ति में भी शब्दगत चमत्कार का प्राधान्य मान कर उसे शब्दालङ्कार ही माना है।
१. तत्रोदात्तादिस्वरभेदात् प्रयत्नभेदाच्च शब्दान्यत्वे शब्दश्लेषः; यत्र प्रायेण
पदभङ्गो भवति । अर्थश्लेषस्तु यत्र स्वरादिभेदो नास्ति । अतएव न तत्र सभङ्गादत्वम् । सङ्कलनया तूभयश्लेषः । -हय्यक, अलङ्कार
सर्वस्व, पृ० ११२ २. मम्मट, काव्यप्रकाश, ६, १२४ पृ० २१६ तथा विश्वनाथ, साहित्यदर्पण पृ० ५५८ ( मम्मट ने इसके शब्दनिष्ठ तथा शब्दार्थोभयनिष्ठ; दोनों रूपों की कल्पना की है।)