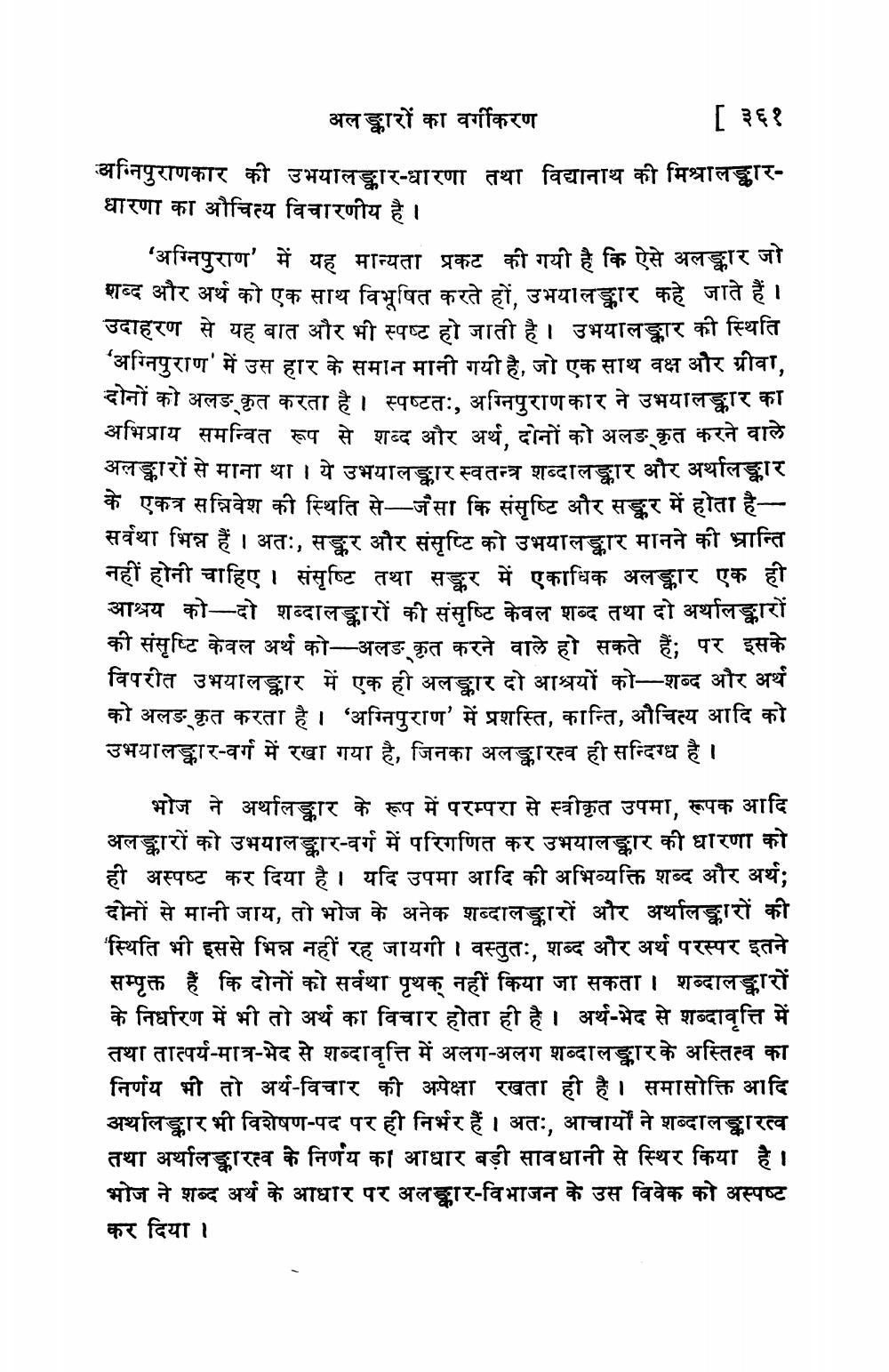________________
अलङ्कारों का वर्गीकरण
[ ३६१ अग्निपुराणकार की उभयालङ्कार-धारणा तथा विद्यानाथ की मिश्रालङ्कारधारणा का औचित्य विचारणीय है ।
'अग्निपुराण' में यह मान्यता प्रकट की गयी है कि ऐसे अलङ्कार जो शब्द और अर्थ को एक साथ विभूषित करते हों, उभयालङ्कार कहे जाते हैं । उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है । उभयालङ्कार की स्थिति 'अग्निपुराण' में उस हार के समान मानी गयी है, जो एक साथ वक्ष और ग्रीवा, दोनों को अलङकृत करता है । स्पष्टतः, अग्निपुराणकार ने उभयालङ्कार का अभिप्राय समन्वित रूप से शब्द और अर्थ, दोनों को अलङ्कृत करने वाले अलङ्कारों से माना था । ये उभयालङ्कार स्वतन्त्र शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार के एकत्र सन्निवेश की स्थिति से - जैसा कि संसृष्टि और सङ्कर में होता हैसर्वथा भिन्न हैं । अतः, सङ्कर और संसृष्टि को उभयालङ्कार मानने की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए । संसृष्टि तथा सङ्कर में एकाधिक अलङ्कार एक ही आश्रय को—दो शब्दालङ्कारों की संसृष्टि केवल शब्द तथा दो अर्थालङ्कारों की संसृष्टि केवल अर्थ को — अलङ कृत करने वाले हो सकते हैं; पर इसके विपरीत उभयालङ्कार में एक ही अलङ्कार दो आश्रयों को — शब्द और अर्थ को अलङ्कृत करता है । 'अग्निपुराण' में प्रशस्ति, कान्ति, औचित्य आदि को उभयालङ्कार-वर्ग में रखा गया है, जिनका अलङ्कारत्व ही सन्दिग्ध है ।
-
भोज ने अर्थालङ्कार के रूप में परम्परा से स्वीकृत उपमा, रूपक आदि अलङ्कारों को उभयालङ्कार वर्ग में परिगणित कर उभयालङ्कार की धारणा को ही अस्पष्ट कर दिया है । यदि उपमा आदि की अभिव्यक्ति शब्द और अर्थ ; दोनों से मानी जाय, तो भोज के अनेक शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों की "स्थिति भी इससे भिन्न नहीं रह जायगी । वस्तुतः, शब्द और अर्थ परस्पर इतने सम्पृक्त हैं कि दोनों को सर्वथा पृथक् नहीं किया जा सकता । शब्दालङ्कारों के निर्धारण में भी तो अर्थ का विचार होता ही है । अर्थ-भेद से शब्दावृत्ति में तथा तात्पर्य- मात्र भेद से शब्दावृत्ति में अलग-अलग शब्दालङ्कार के अस्तित्व का निर्णय भी तो अर्थ- विचार की अपेक्षा रखता ही है । समासोक्ति आदि अर्थालङ्कार भी विशेषण - पद पर ही निर्भर हैं । अतः, आचार्यों ने शब्दालङ्कारत्व तथा अर्थालङ्कारत्व के निर्णय का आधार बड़ी सावधानी से स्थिर किया है । भोज ने शब्द अर्थ के आधार पर अलङ्कार- विभाजन के उस विवेक को अस्पष्ट कर दिया ।