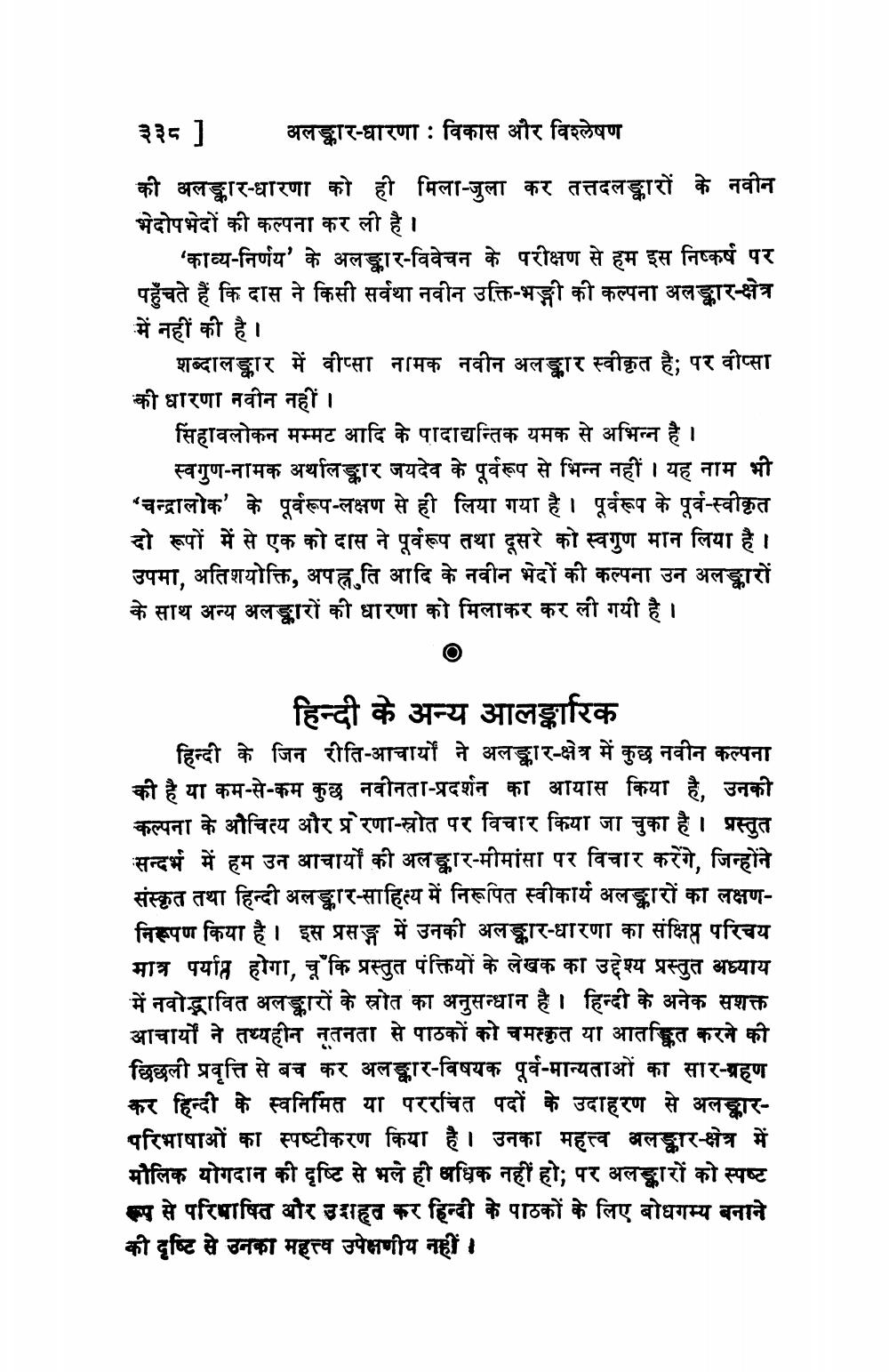________________
३३८ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण की अलङ्कार-धारणा को ही मिला-जुला कर तत्तदलङ्कारों के नवीन भेदोपभेदों की कल्पना कर ली है। ___ 'काव्य-निर्णय' के अलङ्कार-विवेचन के परीक्षण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दास ने किसी सर्वथा नवीन उक्ति-भङ्गी की कल्पना अलङ्कार-क्षेत्र में नहीं की है।
शब्दालङ्कार में वीप्सा नामक नवीन अलङ्कार स्वीकृत है; पर वीप्सा की धारणा नवीन नहीं।
सिंहावलोकन मम्मट आदि के पादाद्यन्तिक यमक से अभिन्न है।
स्वगुण-नामक अर्थालङ्कार जयदेव के पूर्वरूप से भिन्न नहीं । यह नाम भी 'चन्द्रालोक' के पूर्वरूप-लक्षण से ही लिया गया है। पूर्वरूप के पूर्व-स्वीकृत दो रूपों में से एक को दास ने पूर्वरूप तथा दूसरे को स्वगुण मान लिया है। उपमा, अतिशयोक्ति, अपह्न ति आदि के नवीन भेदों की कल्पना उन अलङ्कारों के साथ अन्य अलङ्कारों की धारणा को मिलाकर कर ली गयी है।
हिन्दी के अन्य आलङ्कारिक हिन्दी के जिन रीति-आचार्यों ने अलङ्कार-क्षेत्र में कुछ नवीन कल्पना की है या कम-से-कम कुछ नवीनता-प्रदर्शन का आयास किया है, उनकी कल्पना के औचित्य और प्रेरणा-स्रोत पर विचार किया जा चुका है। प्रस्तुत सन्दर्भ में हम उन आचार्यों की अलङ्कार-मीमांसा पर विचार करेंगे, जिन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी अलङ्कार-साहित्य में निरूपित स्वीकार्य अलङ्कारों का लक्षणनिरूपण किया है। इस प्रसङ्ग में उनकी अलङ्कार-धारणा का संक्षिप्त परिचय मात्र पर्याप्त होगा, चूकि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का उद्देश्य प्रस्तुत अध्याय में नवोद्भावित अलङ्कारों के स्रोत का अनुसन्धान है। हिन्दी के अनेक सशक्त आचार्यों ने तथ्यहीन नतनता से पाठकों को चमस्कृत या आतङ्कित करने की छिछली प्रवृत्ति से बच कर अलङ्कार-विषयक पूर्व-मान्यताओं का सार-ग्रहण कर हिन्दी के स्वनिर्मित या पररचित पदों के उदाहरण से अलङ्कारपरिभाषाओं का स्पष्टीकरण किया है। उनका महत्त्व अलङ्कार-क्षेत्र में मौलिक योगदान की दृष्टि से भले ही अधिक नहीं हो; पर अलङ्कारों को स्पष्ट कम से परिभाषित और उदाहृत कर हिन्दी के पाठकों के लिए बोधगम्य बनाने की दृष्टि से उनका महत्त्व उपेक्षणीय नहीं।