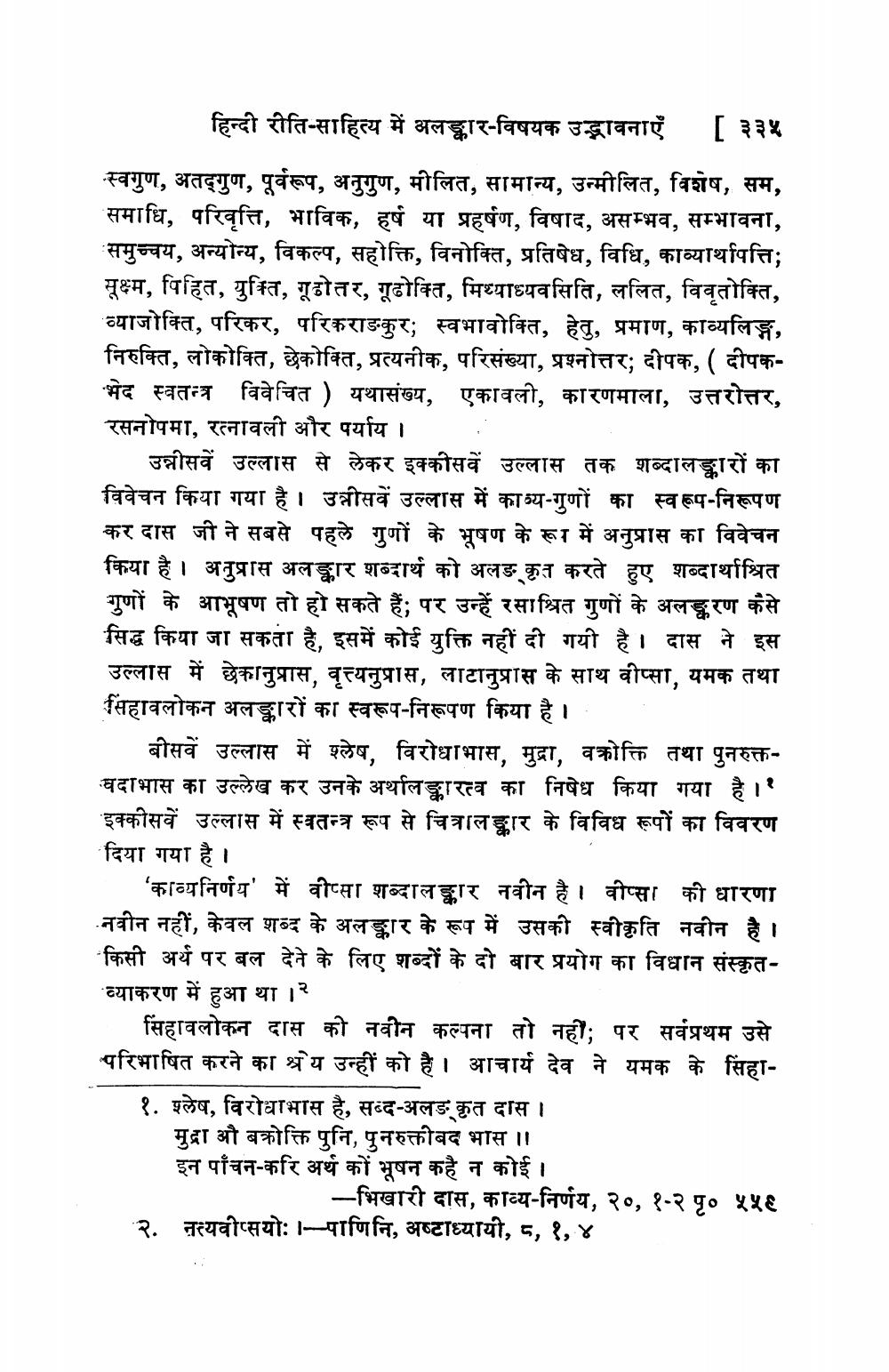________________
हिन्दी रीति-साहित्य में अलङ्कार-विषयक उद्भावनाएँ [ ३३५ स्वगुण, अतद्गुण, पूर्वरूप, अनुगुण, मीलित, सामान्य, उन्मीलित, विशेष, सम, समाधि, परिवृत्ति, भाविक, हर्ष या प्रहर्षण, विषाद, असम्भव, सम्भावना, समुच्चय, अन्योन्य, विकल्प, सहोक्ति, विनोक्ति, प्रतिषेध, विधि, काव्यार्थापत्ति; सूक्ष्म, पिहित, युक्ति, गूढोतर, गूढोक्ति, मिथ्याध्यवसिति, ललित, विवृतोक्ति, व्याजोक्ति, परिकर, परिकराङकुर; स्वभावोक्ति, हेतु, प्रमाण, काव्यलिङ्ग, निरुक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, प्रत्यनीक, परिसंख्या, प्रश्नोत्तर; दीपक, ( दीपकभेद स्वतन्त्र विवेचित ) यथासंख्य, एकावली, कारणमाला, उत्तरोत्तर, रसनोपमा, रत्नावली और पर्याय ।
उन्नीसवें उल्लास से लेकर इक्कीसवें उल्लास तक शब्दालङ्कारों का विवेचन किया गया है। उन्नीसवें उल्लास में काव्य-गुणों का स्वरूप-निरूपण कर दास जी ने सबसे पहले गुणों के भूषण के रूप में अनुप्रास का विवेचन किया है। अनुप्रास अलङ्कार शब्दार्थ को अलङ कृत करते हुए शब्दार्थाश्रित गुणों के आभूषण तो हो सकते हैं; पर उन्हें रसाश्रित गुणों के अलङ्करण कैसे सिद्ध किया जा सकता है, इसमें कोई युक्ति नहीं दी गयी है। दास ने इस उल्लास में छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास के साथ वीप्सा, यमक तथा सिंहावलोकन अलङ्कारों का स्वरूप-निरूपण किया है।
बीसवें उल्लास में श्लेष, विरोधाभास, मुद्रा, वक्रोक्ति तथा पुनरुक्तबदाभास का उल्लेख कर उनके अर्थालङ्कारत्व का निषेध किया गया है।' इक्कीसवें उल्लास में स्वतन्त्र रूप से चित्रालङ्कार के विविध रूपों का विवरण दिया गया है।
'काव्यनिर्णय' में वीप्सा शब्दालङ्कार नवीन है। वीप्सा की धारणा नवीन नहीं, केवल शब्द के अलङ्कार के रूप में उसकी स्वीकृति नवीन है। किसी अर्थ पर बल देने के लिए शब्दों के दो बार प्रयोग का विधान संस्कृतव्याकरण में हुआ था ।२ _ सिंहावलोकन दास को नवीन कल्पना तो नहीं; पर सर्वप्रथम उसे परिभाषित करने का श्रेय उन्हीं को है। आचार्य देव ने यमक के सिंहा१. श्लेष, विरोधाभास है, सब्द-अलङ कृत दास ।
मुद्रा औ बक्रोक्ति पुनि, पुनरुक्तीबद भास ।। इन पाँचन-करि अर्थ कों भूषन कहै न कोई।
-भिखारी दास, काव्य-निर्णय, २०, १-२ पृ० ५५६ २. नत्यवीप्सयोः।-पाणिनि, अष्टाध्यायी, ८, १, ४