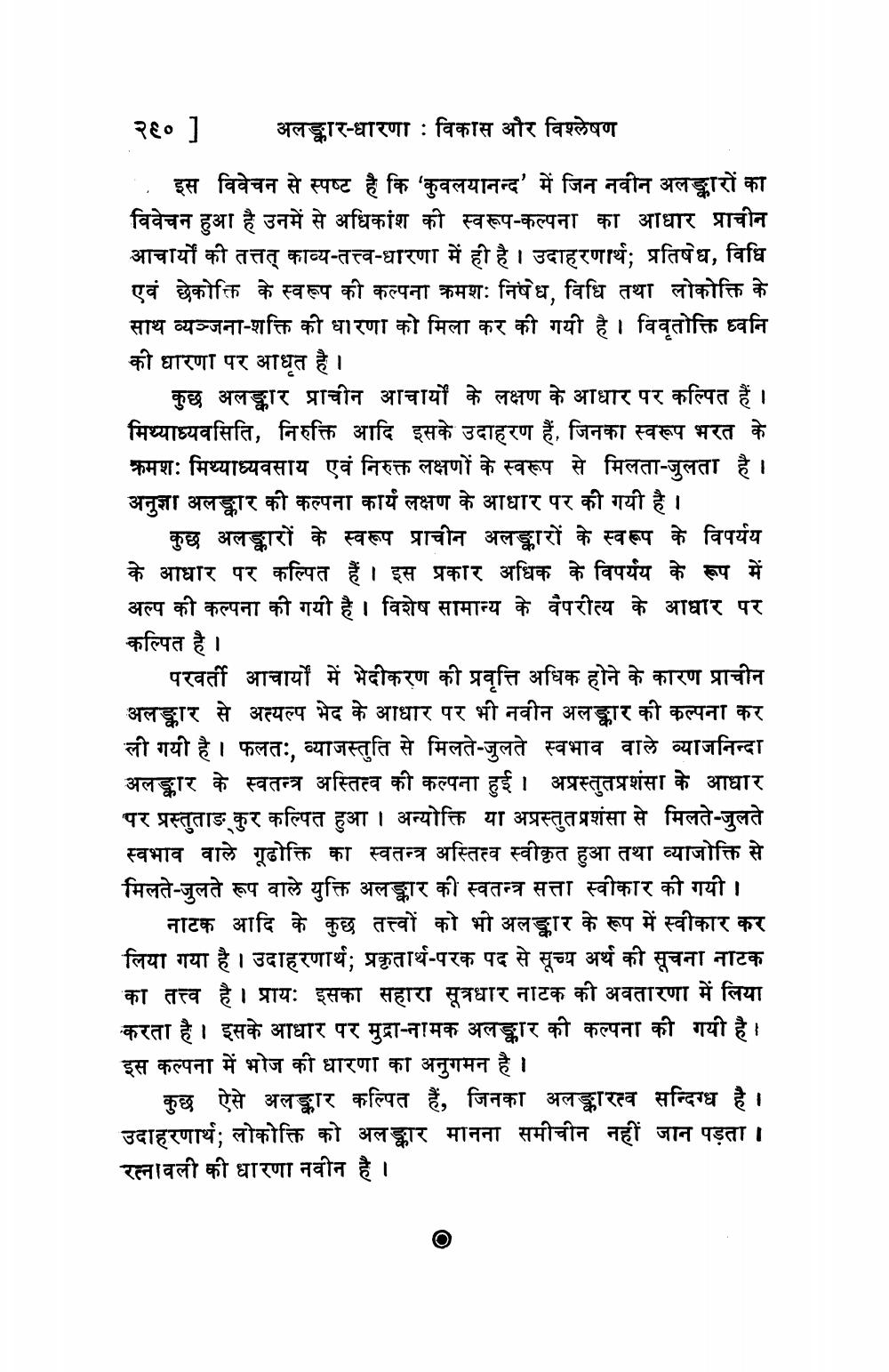________________
२९० ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण . इस विवेचन से स्पष्ट है कि 'कुवलयानन्द' में जिन नवीन अलङ्कारों का विवेचन हुआ है उनमें से अधिकांश की स्वरूप-कल्पना का आधार प्राचीन आचार्यों की तत्तत् काव्य-तत्त्व-धारणा में ही है। उदाहरणार्थ; प्रतिषेध, विधि एवं छेकोक्ति के स्वरूप की कल्पना क्रमशः निषेध, विधि तथा लोकोक्ति के साथ व्यञ्जना-शक्ति की धारणा को मिला कर की गयी है। विवृतोक्ति ध्वनि की धारणा पर आधृत है।
कुछ अलङ्कार प्राचीन आचार्यों के लक्षण के आधार पर कल्पित हैं। मिथ्याध्यवसिति, निरुक्ति आदि इसके उदाहरण हैं, जिनका स्वरूप भरत के क्रमश: मिथ्याध्यवसाय एवं निरुक्त लक्षणों के स्वरूप से मिलता-जुलता है। अनुज्ञा अलङ्कार की कल्पना कार्य लक्षण के आधार पर की गयी है। ___कुछ अलङ्कारों के स्वरूप प्राचीन अलङ्कारों के स्वरूप के विपर्यय के आधार पर कल्पित हैं। इस प्रकार अधिक के विपर्यय के रूप में अल्प की कल्पना की गयी है। विशेष सामान्य के वैपरीत्य के आधार पर कल्पित है।
परवर्ती आचार्यों में भेदीकरण की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण प्राचीन अलङ्कार से अत्यल्प भेद के आधार पर भी नवीन अलङ्कार की कल्पना कर ली गयी है। फलतः, व्याजस्तुति से मिलते-जुलते स्वभाव वाले व्याजनिन्दा अलङ्कार के स्वतन्त्र अस्तित्व की कल्पना हुई। अप्रस्तुतप्रशंसा के आधार पर प्रस्तुताङ कुर कल्पित हुआ । अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा से मिलते-जुलते स्वभाव वाले गूढोक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकृत हुआ तथा व्याजोक्ति से मिलते-जुलते रूप वाले युक्ति अलङ्कार की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गयी।
नाटक आदि के कुछ तत्त्वों को भी अलङ्कार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उदाहरणार्थ; प्रकृतार्थ-परक पद से सूच्य अर्थ की सूचना नाटक का तत्त्व है। प्रायः इसका सहारा सूत्रधार नाटक की अवतारणा में लिया करता है। इसके आधार पर मुद्रा-नामक अलङ्कार की कल्पना की गयी है। इस कल्पना में भोज की धारणा का अनुगमन है। ____ कुछ ऐसे अलङ्कार कल्पित हैं, जिनका अलङ्कारत्व सन्दिग्ध है। उदाहरणार्थ; लोकोक्ति को अलङ्कार मानना समीचीन नहीं जान पड़ता। रत्नावली की धारणा नवीन है।