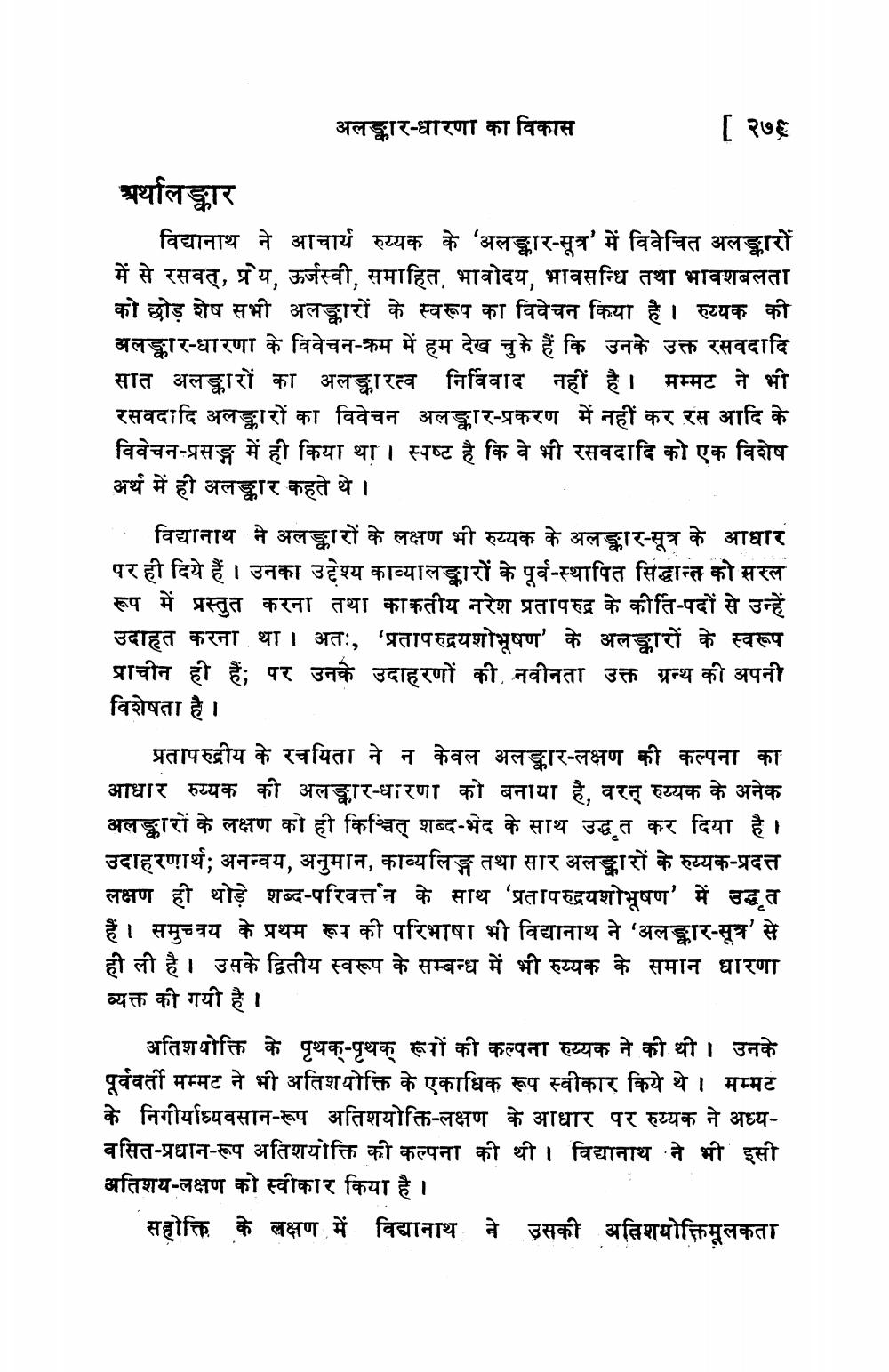________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ २७६
अर्थालङ्कार
विद्यानाथ ने आचार्य रुय्यक के 'अलङ्कार-सूत्र' में विवेचित अलङ्कारों में से रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वी, समाहित, भावोदय, भावसन्धि तथा भावशबलता को छोड़ शेष सभी अलङ्कारों के स्वरूप का विवेचन किया है। रुय्यक की अलङ्कार-धारणा के विवेचन-क्रम में हम देख चुके हैं कि उनके उक्त रसवदादि सात अलङ्कारों का अलङ्कारत्व निर्विवाद नहीं है। मम्मट ने भी रसवदादि अलङ्कारों का विवेचन अलङ्कार-प्रकरण में नहीं कर रस आदि के विवेचन-प्रसङ्ग में ही किया था। स्पष्ट है कि वे भी रसवदादि को एक विशेष अर्थ में ही अलङ्कार कहते थे। - विद्यानाथ ने अलङ्कारों के लक्षण भी रुय्यक के अलङ्कार-सूत्र के आधार पर ही दिये हैं । उनका उद्देश्य काव्यालङ्कारों के पूर्व-स्थापित सिद्धान्त को सरल रूप में प्रस्तुत करना तथा काकतीय नरेश प्रतापरुद्र के कीर्ति-पदों से उन्हें उदाहृत करना था। अतः, 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' के अलङ्कारों के स्वरूप प्राचीन ही हैं; पर उनके उदाहरणों की, नवीनता उक्त ग्रन्थ की अपनी विशेषता है।
प्रतापरुद्रीय के रचयिता ने न केवल अलङ्कार-लक्षण की कल्पना का आधार रुय्यक की अलङ्कार-धारणा को बनाया है, वरन् रुय्यक के अनेक अलङ्कारों के लक्षण को ही किञ्चित् शब्द-भेद के साथ उद्धत कर दिया है। उदाहरणार्थ; अनन्वय, अनुमान, काव्यलिङ्ग तथा सार अलङ्कारों के रुय्यक-प्रदत्त लक्षण ही थोड़े शब्द-परिवर्तन के साथ 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' में उद्ध त हैं। समुच्चय के प्रथम रूप की परिभाषा भी विद्यानाथ ने 'अलङ्कार-सूत्र' से ही ली है। उसके द्वितीय स्वरूप के सम्बन्ध में भी रुय्यक के समान धारणा व्यक्त की गयी है।
अतिशयोक्ति के पृथक्-पृथक् रूपों की कल्पना रुय्यक ने की थी। उनके पूर्ववर्ती मम्मट ने भी अतिशयोक्ति के एकाधिक रूप स्वीकार किये थे। मम्मट के निगीर्याध्यवसान-रूप अतिशयोक्ति-लक्षण के आधार पर रुय्यक ने अध्यवसित-प्रधान-रूप अतिशयोक्ति की कल्पना की थी। विद्यानाथ ने भी इसी अतिशय-लक्षण को स्वीकार किया है।
सहोक्ति के लक्षण में विद्यानाथ ने उसकी अतिशयोक्तिमूलकता